 हेमंत कुमार झा
हेमंत कुमार झा
नई सरकार श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव करने जा रही है। जिन्हें इन बदलावों का संज्ञान लेना चाहिये था, इनकी धाराओं की गहराई में जाना चाहिये था उनमें से अधिकतर चेतनाशून्य से हैं।
यह चेतना शून्यता अचानक की त्रासदी नहीं है। यद्यपि, हाल के वर्षों में इसकी गति में तीव्रता आई है...जब से सस्ते और तकनीकी रूप से उन्नत स्मार्टफोन लोगों के हाथों में आए हैं।
फ्री डाटा की उपलब्धता ने स्मार्टफोन को व्यवस्था का प्रभावी औजार बना दिया और नई पीढ़ी को राजनीतिक रूप से दिग्भ्रमित करना इतना आसान हो गया जितना इतिहास में कभी नहीं था।
हालांकि, युवा पीढ़ी की सामूहिक चेतना को कुंद करने के व्यवस्था के प्रयास एकायामी नहीं हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली का जैसा विकास हुआ है, मीडिया की प्रकृति और उसके चरित्र में जो बदलाव आए हैं...इन सबने सुनिश्चित किया है कि नई पीढ़ी अपने हित-अहित को लेकर इतनी संवेदनशील न बन पाए कि वह व्यवस्था को चुनौती दे सके।
सामूहिक चेतना के विकास के रास्ते में मनोवैज्ञानिक अवरोध खड़े करना अब अधिक आसान है।
नतीजा...दर्जनों की संख्या में छात्र संघों की सक्रियता के बावजूद उनके देखते-देखते शिक्षा तंत्र छात्र विरोधी, वंचित विरोधी बनता गया और तमाम संघ लकीरें पीटते रहे।
सबसे बड़ी जरूरत थी कि युवाओं को वास्तविकताओं का आकलन हो पाता। लेकिन...सूचना क्रांति जब कृत्रिम और प्रदूषित सूचनाओं के दौर में पहुंच गई तो वास्तविकता का आभास कर पाना बेहद कठिन हो गया।
अपनी शिक्षा के क्रम में नई पीढ़ी नेहरू, गांधी, अंबेडकर से लेकर बुद्ध, महावीर तक के बारे में जो जानती है उसमें सूचना का तत्व अधिक रहता है, ज्ञान का कम। सूचनाओं को विश्लेषित करने के लिये ज्ञान की संस्कृति का विकास आवश्यक है। लेकिन, व्यवस्था ने इसे अधिकाधिक हतोत्साहित किया है। नतीजा...नई पीढ़ी की विश्लेषण क्षमता का विकास प्रभावित होता है। उन्हें नहीं पता कि बुद्ध और महावीर से लेकर गांधी और अंबेडकर ने मनुष्य की गरिमा के लिये ही संघर्ष किया था...जिसे अब सुनियोजित तरीके से छीना जा रहा है।
सूचनाओं के विश्लेषण में रुचि नहीं लेने वाली पीढ़ी भ्रामक सूचनाओं के प्रभाव में जल्दी आती है। निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि गांधी और नेहरू को लेकर हाल के वर्षों में इतने सुनियोजित दुष्प्रचार हुए हैं कि बच्चे समझ नहीं पा रहे कि सच क्या है।
जिस पीढ़ी के दिमाग में यह भर दिया जाए कि विकास दर ही देश वासियों के सामूहिक विकास का पैमाना है, निजीकरण ही सारी समस्याओं का समाधान है वह विकास प्रक्रिया पर सवाल कैसे उठा सकता है?
जिस पीढ़ी को यह पढ़ाया ही नहीं गया कि श्रमिकों को मनुष्य का दर्जा देने के लिये कई पीढ़ियों ने दो शताब्दियों से भी अधिक का लंबा संघर्ष किया है, जिसे पता ही नहीं है कि काम के घंटों के उचित निर्धारण के लिये कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है वह इन्हें खोने के मानवीय दुष्प्रभावों का आकलन कैसे कर सकती है?
जिसे पाने के लिये शताब्दियों से संघर्ष चलता रहा हो और खोने में दो-ढाई दशक भी न लगें तो यह उस पीढ़ी की वैचारिक शून्यता को ही दर्शाता है।
अगर किसी सिक्युरिटी गार्ड का बच्चा बीमार है और एक दिन की छुट्टी मांगने पर प्रबंधन उसके तीन दिनों का वेतन काटने की धमकी देता है, नतीजा बच्चा बिना इलाज के मर जाता है तो...इस मुद्दे पर देशव्यापी विमर्श होना चाहिये था कि कम्पनियों को ऐसी मनमानी करने का कानूनी आधार कैसे मिलता है।
यह सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे देश के 80 प्रतिशत युवा, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर पाते हैं, सिक्युरिटी गार्ड, जोमैटो या स्विगी टाइप की कंपनियों के डिलीवरी ब्वाय, दिहाड़ी कर्मी या ऐसा ही कुछ बनने लायक कुशलता ही विकसित कर पाते हैं। इस तरह के कर्मियों की संख्या करोड़ों में है। सेवा शर्त्त, काम के घंटों और पारिश्रमिक को लेकर कंपनियां उनके साथ जो मनमानी करती हैं वह मनुष्यता के सिद्धांतों का सीधा अतिक्रमण करता है।
बाजार और उसकी मुनाफा आधारित संस्कृति को तो मनुष्यता विरोधी होना ही है। यह उसका सहज स्वभाव है। यहीं पर सरकारों की भूमिका शुरू होती है कि वह ऐसे कानूनों का निर्माण करें और इन कानूनों के अनुपालन के लिये ऐसे नियामक तंत्र विकसित करें ताकि बाजार मनुष्यता का अतिक्रमण न कर सके।
कोई तो संधि रेखा होनी चाहिये जिसकी हदों में श्रमिकों के मानवीय अधिकार बरकरार रह सकें। असंगठित क्षेत्र में तो पहले से ही श्रमिक विरोधी व्यवस्था हावी थी, अब संगठित क्षेत्र में भी ऐसी अराजकता फैल रही है।
निजी स्कूलों के शिक्षकों, निजी अस्पतालों के पारा मेडिकल कर्मियों आदि के शोषण की दास्तानें दिल दहलाने वाली हैं। लेकिन, इनकी कहीं सुनवाई नहीं क्योंकि कानून दिन ब दिन श्रमिक विरोधी होते जा रहे हैं और प्रबंधनों पर नियामक एजेंसियों की लगाम ढीली होती जा रही है।
आर्थिक मंदी की आहट और रोजगार के अवसरों में संकुचन ने बहुत सारे मध्यवर्गीय पढ़े लिखे युवाओं को भी विवश किया है कि वे अपनी बाइक लेकर अपने ही शहर में जोमेटों, स्विगी के डिलीवरी ब्वाय बन जाएं, किसी निजी बीमा कंपनी के एजेंट बन जाएं, किसी स्टाकिस्ट के एकाउंटेंट बन जाएं। निम्न मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय युवाओं के लिए जो रोजगार थे अब उनमें मध्यवर्गियों का भी प्रवेश हो चुका है और रोजगार में टिके रहने की जद्दोजहद में वे भी मनुष्य होने का अधिकार खोते जा रहे हैं।
जब कार्यसंस्कृति ही ऐसी विकसित हो रही हो जिसमें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पदों का अवमूल्यन कर दिया जाए, सरकारी बैंकों के कर्मियों को काम के अनुचित बोझ तले दबा दिया जाए, तो निजी स्कूलों और निजी बैंकों/वित्तीय संस्थानों के कर्मियों के अधिकारों की बात कौन करे।
व्यवस्था अपने षड्यंत्रों में सफल है। हर क्षेत्र में शोषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मुनाफा बढाने के लिये कंपनियां श्रमिकों से मनुष्य होने का अधिकार छीनती जा रही हैं।
जिन्हें भविष्य में इस श्रम व्यवस्था में शामिल होना है, ऐसी नई पीढ़ी में इन मुद्दों पर जागरूकता का अभाव कतई आश्चर्य में नहीं डालता। हमारी पीढ़ी ने यही संस्कार उनमें डाला है।
हम वह अभिशप्त पीढ़ी हैं जिसने अपने पूर्ववर्त्तियों के संघर्षों को मिट्टी में मिलाया है और अपनी आने वाली पीढ़ी से मनुष्य होने का अधिकार छीनने वालों का जयघोष किया है।



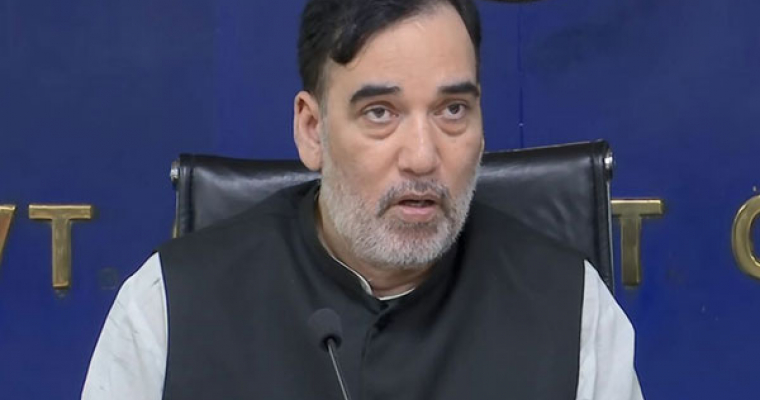



Comments