 राजेश बादल।
राजेश बादल।
चैनल इंडस्ट्री विराट हो रही है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय चैनलों की बाढ़। साल भर चुनाव का माहौल। हर चैनल को चर्चा के लिए चाहिए अनेक मेहमान पत्रकार। सारे सारे दिन बैठकर हर मुद्दे पर बाल की खाल निकालने वाले मेहमान।
शो का मानक ढांचा बन गया है-एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक पत्रकार। जिस मसले में तीसरी या चौथी पार्टी शामिल होती है तो उसका प्रवक्ता भी ज़रूरी है। अगर कोर्ट-कचहरी का मामला है तो वकील भी चाहिए।
इस तरह स्क्रीन पर पांच- छह खिड़कियां खुल जाती हैं। एक ऐसा ऑर्केस्ट्रा, जिसका हर वाद्य अपनी अलग धुन निकालता है। कई बार यह ऑर्केस्ट्रा बेसुरा हो जाता है। परदे पर गाली-गलौज जैसे हालाात बन जाते हैं।
सवाल ऑर्केस्ट्रा के बेसुरे होने पर नहीं है। इस पर है कि मेहमान के रूप में हम पत्रकार अपनी भूमिका के साथ कितना न्याय करते हैं? लंबी चर्चाओं से पत्रकार-मेहमानों के बारे में राय बनने लगती है।
चैनलों में राजनीतिक विषयों पर बहस के लिए यह छवि या राय बड़ा काम करती है। जब किसी राजनीतिक दल का कोई प्रवक्ता शो के समय तक नहीं मिलता तो गेस्ट-कोऑर्डिनेशन विभाग में बात होती है-अमुक पत्रकार प्रो बीजेपी है, उसे बुलाओ।
अमुक पत्रकार प्रो कांग्रेस है, उसे बुलाओ। अमुक पत्रकार प्रो या एंटी लेफ्ट है, उसे बुलाओ। अर्थात उस पत्रकार को चर्चा में शामिल करने का आधार उसकी काबिलियत नहीं, दलों के समर्थन या विरोध में बोलने के कारण बन जाता है।
उसके बाद उससे सवाल भी कुछ इस तरह किए जाते हैं मानो वह उस पार्टी का प्रवक्ता हो। इससे उसकी छवि पत्रकार सह राजनेता की बन जाती है। कुछ पत्रकार इस छवि के चलते बाद में बाक़ायदा उस पार्टी से जुड़ ही गए।
मुश्किल यह है कि निष्पक्ष पत्रकार की छवि इस पेशे की अनिवार्य शर्त है और वही बनाए रखना कठिन है। अगर आप बीजेपी की आलोचना करते हैं तो उसके विरोधी अथवा कांग्रेस समर्थक मान लिए जाते हैं। यदि कांग्रेस की आलोचना करते हैं तो उसके विरोधी मान लिए जाते हैं। कभी-कभी कई पत्रकार कोशिश करते हैं कि जिस चैनल में जा रहे हैं। अगर उसकी विचारधारा है, उसके अनुसार बोलने की कोशिश करते हैं।
संसदीय या सरकारी चैनलों में भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया देने के स्थान पर उस चैनल की चौखट का ख़्याल रखना पड़ता है। वैसे इसमें कोई आलोचना का कारण नहीं है। चिंता यह है कि पत्रकार अपने मौलिक विश्लेषण का अवसर तनिक कमज़ोर बना देते हैं।
इन दिनों मीडिया की अंदरूनी स्थितियां चुनौती भरी हैं। विश्लेषक पत्रकारों के सामने चैनल से मिलने वाला धन भी आड़े आता है। पार्टी से जोड़कर छवि बन जाती है। फिर भी जाते रहते हैं। अब तो सालाना अनुबंध भी होने लगे हैं। इसमें अनेक अवसरों पर पत्रकारिता के ज्ञान और अनुभव से अधिक उसका चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है।
भले ही पूरे शो में उसे दो-चार मिनट ही बोलने का अवसर मिले। उसकी स्थिति घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हो जाती है। इसके विपरीत कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो पत्रकारों को चर्चा में निशुल्क शामिल करते हैं। थेंक्यू सर्विस में प्राप्त होने वाले विचार भी अपने हित की चाशनी में डूबे होते हैं। यह बहुत पेशेवर रवैया नहीं है।
चैनलों को मुफ़्त सेवा प्राप्त करने की मंशा अब छोड़नी चाहिए। कोई भी चैनल मालिक कारोबार करने के लिए ही चैनल चलाता है। मशीनरी पर वह करोड़ों ख़र्च कर देता है, मानसिक श्रम की क़ीमत गौण हो जाती है। फिर हम लोग अपनी गोष्ठियों में डींग हांकते हैं कि-कंटेंट इज़ द किंग।
इन सारी स्थितियों में पत्रकार की निष्पक्षता पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता है। अगर यह इमेज खंडित होती है तो ज़ाहिर है पत्रकारिता के लिए नुकसान ही है। इसे तो गंभीरता से लेना ही पड़ेगा मिस्टर मीडिया!
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।




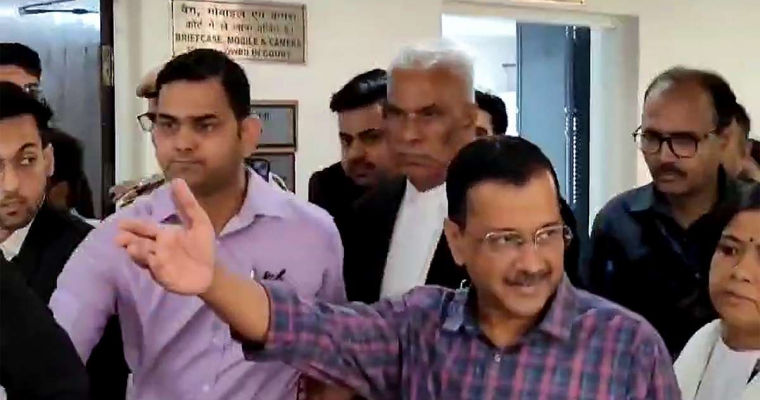


Comments