गोडसे ने गांधी को एक बार मारा, लेकिन...
खरी-खरी
Jan 30, 2015
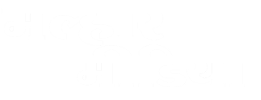
ममता यादव
पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रत्येक राजनीतिक दल ने अपने-अपने हिसाब और अपनी सुविधानुसार अपनाया और उसका उपयोग किया। देखा जाये तो सभी बड़ी पार्टियां ये दिखाने के प्रयास में लगी रहती हैं कि वह सबसे ज्यादा गांधी जी के सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप चल रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है ये वे भी जानते हैं और पूरा देश भी।
प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती और पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी की प्रासांगिकता पर सवाल उठाये जाते हैं।, लेकिन अतीत के पन्नों को यदि पलटा जाये तो हकीकत ये है कि गांधीजी तो अपने जीते जी ही आजादी के दिनों में ही आप्रसांगिक और अकेले हो गये थे। उनके सहयागियों ने उनके मूल्यों और कार्यक्रमों को तिलांजली दे दी थी।
वास्तव में गांधीजी 1946 में ये महसूस करने लगे थे कि अब उनका प्रभाव कम होने लगा है और उनकी बात नहीं सुनी जाती, जिसका जीता-जागता उदाहरण था सन् 1946 में उनकी इच्छा के विपरीत पंजाब का बंटवारा। इस बंटवारे से गांधीजी कितने दुखी हुये, उसका बयान शब्दों में करना मुश्किल है। उनका यह दुख एक प्रार्थना सभा में कहे गये इन शब्दों में साफ महसूस किया जा सकता है, कांग्रेस जो फैसला करेगी वही होगा, मेरे कहने के अनुसार कुछ नहीं होगा। मेरा आदेश अब नहीं चलता मैं वीराने में रो रहा हूं।
जो कांग्रेस पार्टी आज अपने को गांधीवादी कहते नहीं थकती वास्तव में गांधीजी ने उसी काग्रेस को खत्म करने की बात कही थी, क्योंकि तब कांग्रेस समाजसेवी पार्टी नहीं रह गई थी, बल्कि सत्तालोलुपों का अखाड़ा बनती जा रही थी। वे चाहते थे कि कांग्रेस सत्ता की भूखी पार्टी न बने बल्कि सत्ता जनता के सेवकों की संस्था बने और मुख्य रूप से गांवों में काम करे। गांधीजी का मानना था कि कांग्रेस की उपयोगिता खत्म हो चुकी है और उसे भंग कर देना जरूरी है। गांधी ने नेहरू को अपना उत्तारधिकारी कहा था, लेकिन खुद गांधीजी का नेहरू से मोहभंग होता जा रहा था। गांधीजी का मानना था कि रक्षा खर्च में कटौति की जाये,सरकारी तनख्वाहों पर भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के बजाय अधिक से अधिक स्वयं सेवकों को काम दिये जायें।
गांधीजी के कश्मीर मसले को सुलाझाने के अपने विचार थे, लेकिन उनके कश्मीर मसले पर शांतिपूर्ण प्रस्ताव को नेहरू ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगर नेहरू उनके उस प्रस्ताव को मान लेते तो संभवत: एक खर्चीले युद्ध से भारत अपने आप को बचा सकता था। महात्मा गांधी की जीवनी में वोल्पर्ट ने लिखा हथियारों के प्रसार में और अपनी विदेश नीति के मामले में नई दिल्ली बापू के आदर्श रास्ते और उनके जीवन भर के उपदेशों से बहुत दूर हो गई थी। 1947 तक गांधीजी ने अपने को वर्धा से काट लिया था।
महात्मा गांधी की जीवनी में जूडिश ब्राउने ने लिखा है, उनकी निर्लज्जता से उपेक्षा की गई, गांधीजी को इसका तीव्र अहसास था कि अब उनकी कोइ्र जरूरत नहीं रह गई है। वह अकेली आवाज रह जाने की बात करते थे। वह व्याकुल होकर कहते थे कि नये भारत में उनकी क्या जगह रह जायेगी? लंबी जिंदगी की कामना उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि वह बहुत लाचार महसूस करने लगे थे। गोडसे ने गांधी को एक बार मारा,लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने गांधीजी के सीने में इतने घाव किये थे कि वे पूरी तरह से छितरा गये थे। शायद इसलिये वह देश सेवा नहीं कर पा रहे थे। देश के विभाजन और बंगाल सहित दूसरे हिस्सों में भड़के दंगों के दौरान गांधी के अलग-थलग पड़ जाने की तस्वीर अब और साफ हो गई थी। यहां तक कि सरकार और संसद की भूमिका पर एतराज के कारण पंडित नेहरू ने उन्हें सेंटीमेंटलतक कहा था।
आज सरकारी कामकाजों में गांधीवादी मूल्यों, कार्यक्रमों और लक्ष्यों की तलाश हमें गांधीवादी मूल्यों, कार्यक्रमों और लक्ष्यों की तलाश में हमें निराश कर सकती है। यदि वह मूल्यांकन किसी कारण जरूरी भी लगे तो हासिल खाते में सिवाय खामियाजा सूची के कुछ नहीं होगा।
स्वराज आंदोलन के दिनों में भी अपने रचनात्मक अभिक्रमों को साथ लेकर चलने वाले गांधी ने भारतीय समाज और उसकी परंपराओं, आस्थाओं में श्रम की महत्ता पहचान ली थी। इसलिये उनका जोर पूंजी आधारित आर्थिक विकास के बजाय श्रम आधारित स्वाबलंबन पर था। गांधीजी मशीनीकरण के विरोधी नहीं थे,उनका विचार था कि यंत्रीकरण उस स्थिति में अच्छा है, जब काम की मात्रा की अपेक्षा काम करने वालों की संख्या कम हो। भारत में जनाधिक्य को देखते हुये वे मशीनीकरण के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इससे बेकार श्रमिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होती है। उनका विचार था मशीनों के प्रयोग से इनेगिने लोग लाखों का शोषण करने लगेंगे।
इसी प्रकार सर्वधर्म समभाव की जो विचारधारा गांधीजी ने रखी वह बाद में साम्प्रदायिक भेदभाव और दंगा भड़काव में बदल गई। आज हिदू-मुस्लिमों के नाम पर राजनीतिज्ञ क्या कर रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। गांधीजी की भावना सभी धर्मों की अच्छाईयों को अपनाने की थी, इसलिये उन्होंने इस बात को मानने से इन्कार कर दिया था कि भारत के सामने केवल प्राचीन आर्य परंपरा की ओर लौटने का विकल्प है। उनकी स्पष्ट राय थी कि बदलती परिस्थितियों में हिंदू धर्म और समाज को भी बदलना होगा। हर धर्म की कुछ विशेषता है, जैसे हिंदुओं की चिंतन की व्यापकता और उदारता, मुसलामानों का बिरादराना भाईचारा, बौद्धों की वैज्ञानिक व मध्यम मार्गीय विचारधारा, जैनियों का अनेकांत और ईसाइयों का प्रेम व सद्भाव। गांधीजी के अनुसार ये सब मानव जाति की अनुकरणीय निधियां हैं।
बहरहाल गांधीजी के उक्त विचारों के संक्षेप उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि वास्तव में यदि आजादी के बाद भारत उनके पदचिन्हों पर चलता तो इसकी तस्वीर कुछ और ही होती, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गांधी के नाम और उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का महज ढिंढोरा पीटा गया। गांधीजी की हालत आज लूट सके तो लूट वाली है। वे आज अमूर्त, अनैतिहासिक, उत्तर-आधुनिक हो चुके हैं। अपने समय में स्थित अपने समय के आदमी वे अब नहीं रह गये हैं। गांधी आज एक ऐसी अवधारणा बन गये हैं, जिसके साथ कोई कुछ भी कर सकता है। सांस्कृतिक प्रतीकों के उपलब्ध भंडार का एक अंश, एक ऐसा विंब, जिसे आधार लेकर इस्तेमाल किया जा सकता है, तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। विभिन्न उद्देश्यों की सेवा के लिये जिसे नयी-नयी शक्लों में ढाला जा सकता है और यह सब करते हुये ऐतिहासिकता और सत्य को कहीं दूर घूरे पर फेंक दिया जा सकता है। बेहतर हो कि अब गलतियों से सबक लिया जाये और पिछले दशकों की गलतियों को दोहराया न जाये बल्कि, गांधी के आदर्शों, सिद्धांतों को आत्मसात कर उन पर चलकर एक नये राष्ट्र निर्माण की नींव रखी जाये।
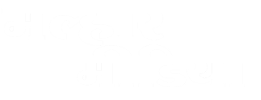
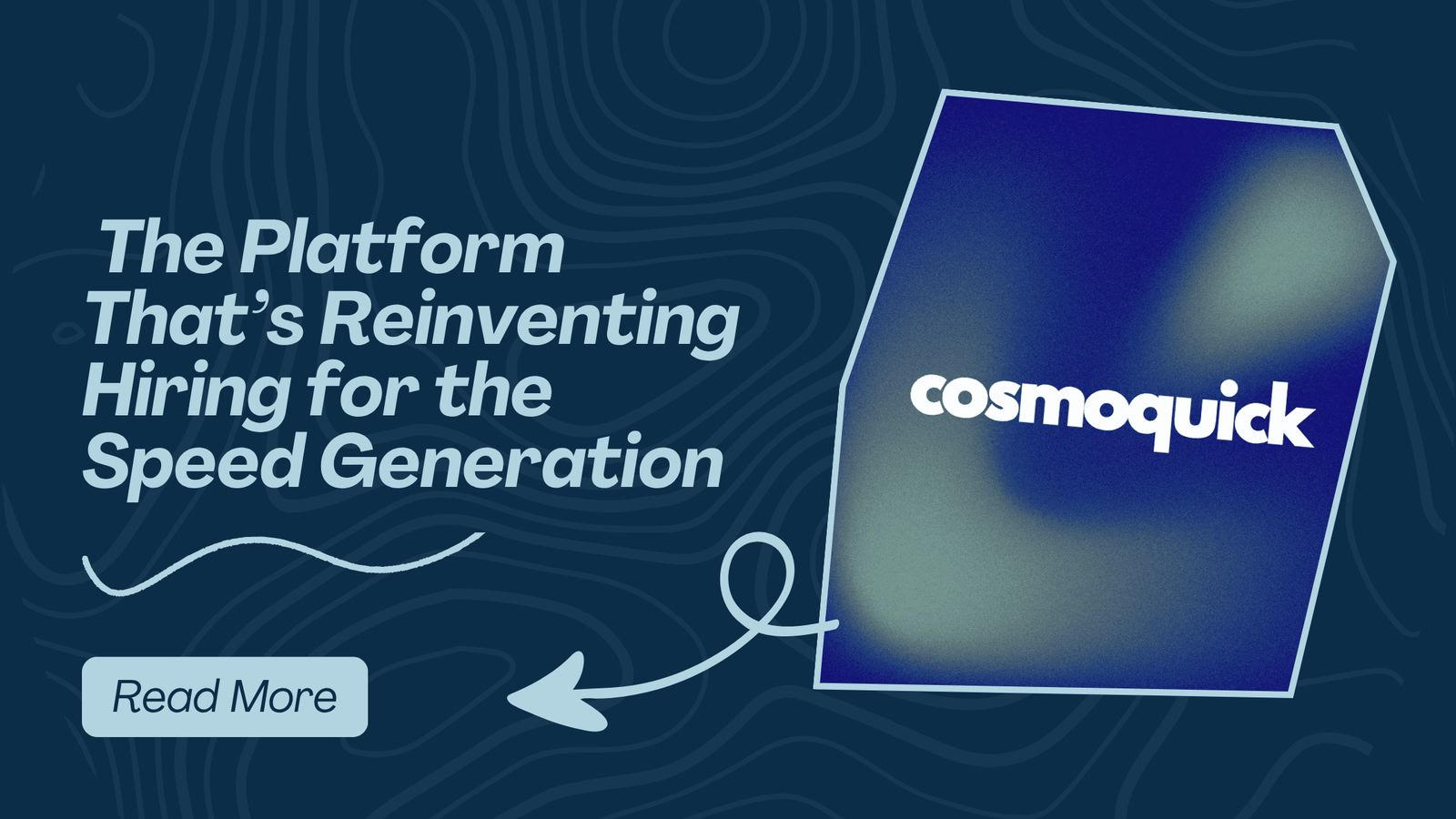





Comments