 श्रीश पांडे
श्रीश पांडे
हर पर्व की अपनी एक संस्कृति है, परम्परा है, उसका दर्शन है और इसीलिए इनका हर वर्ष हमारे जीवन में आगमन होता है, ताकि उसका न सिर्फ स्मरण बना रहे, बल्कि जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, का अहसास देश, समाज और वहां के नागरिक करते रहें।
भारत को सांस्कृतिक भिन्नता का अजायबघर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में और कोई मुल्क नहीं जहां भारत जैसी बहुरंगी संस्कृति, धर्म, भाषा-बोली, खान-पान और ऋतुओं की विविधता विद्यमान हो।
इस देश की विकास यात्रा को वर्तमान तक लाने में अनेक बलिदान, त्याग और संघर्ष की अनेक स्वर्णिम शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इसी स्वर्णिम इतिहास को स्मरण रखने के बरक्स आजादी के बाद से भारत में दो राष्ट्रीय पर्वों की परम्परा बरकरार रखी गई है। इन दोनों पर्वों से देश का हर कोना परिचित है। पहला है आजादी का पर्व जिसकी नाभिनाल 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि से जुड़ी है,जब ब्रितानी हुकूमत के यूनानी जैक को उतारकर देश में तिरंगे को फहराया गया था। आजादी अपने आप में वृहद अर्थ लिए हुए है।
एक आजाद देश का नागरिक होने का अनुभव उस पीढ़ी ने बारीकी से किया होगा जिसने होशोहवास में गुलाम भारत से आजाद भारत में न सिर्फ सांसें ली हो, बल्कि इसके लिए एक लम्बा संघर्ष देखा हो, झेला हो। लेकिन आजादी मिलना एक अवस्था है, मगर उसको बनाए रखना दूसरी और कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्य के साथ देश की कानून व्यवस्था की रूपरेखा व इसका संचालन कैसे हो इसके लिए देश का समग्र एवं स्पष्ट संविधान आवश्यक है।
इसी संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 195० है। यहीं भारत के दूसरे राष्ट्रीय पर्व का आरंभ हुआ, जिसे हम आज एक बार फिर 'गणतंत्र दिवस’ के तौर पर इसकी 67 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संविधान यानि ऐसा निश्चित और अनिवार्य विधान या कानून जिसमें सभी को समानता देने की भावना निहित है।
दरअसल, गणतंत्र यानि ऐसा तंत्र जिसमें राज्य का प्रमुख अनुवांशिक न होकर जनता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित शख्स होगा। कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां शासन पद्धति लोकतांत्रिक होती है, पर राष्ट्राध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जाता। जैसे ब्रिटेन, जापान जहां राष्ट्राध्यक्ष सम्राट होता है, जिसके परिवार के सदस्य ही राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। इस मायने में ब्रिटेन और जापान रिपब्लिक नहीं है।
भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार है मगर राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) का चुनाव होता है, इसलिए यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार तो हो गया था, मगर इसे दो महीने बाद 26 जनवरी 195० को ही लागू क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कि 26 जनवरी 193० के लाहौर कांग्रेस-अधिवेशन में पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था और अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में इसकी मांग की थी।
हालांकि संविधान से नागरिकता, चुनाव और संसद जैसी व्यवस्थाएं तत्काल लागू हो गईं थीं। इसी प्रकार राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन वह 15 अगस्त 1947 से औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज बना था। इसी कार्यक्रम में श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्रध्वज डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भेंट किया।
आज भी गणतंत्र से मिली ताकत और कमजोरियों के सवाल हमारा ध्यान बरबस खींचते हैं। हालांकि 67 वर्षों का सफर कोई अधिक नहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हम गणतंत्र के अर्थ को समझ-बूझ न सकें हों। मगर विकास और नागरिक अधिकारों के संरक्षण में हमारा तंत्र धीमा रहा है। तो इसके पीछे दोहरे कारण हैं। पहला केन्द्र और राज्यों में स्थापित सरकारें रही हैं, तो दूसरा अधिकांश नागरिकों का देश के प्रति उदासीन रवैय्या। मोटे तौर पद देखें तो भारत में अवाम हर मुश्किल में सरकारों से आपेक्षा करती है कि वह उन्हें दामादों की तरह केयर करे। यह सही है कि सरकार का दायित्व है कि जनकल्याण उसके जिम्मे है, लेकिन नागरिक स्तर पर भी सजगता और देश के प्रति निष्ठा की प्रगाढ़ता दिखनी चाहिए। मगर सरकारी संसाधन हो या काम काज सबके प्रति हमारा लापरवाहीपूर्ण रुख नजर आता है।
मसलन, शिक्षा हो या व्यापार, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जहां निजी क्षेत्र काम कर रहा है और जहां सरकारी दोनों की व्यवस्थाओं और मानसिकता में साफ फर्क मौजूद है। एक निजी स्कूल या फैक्ट्री का प्रबंधन और एक सरकारी स्कूल या निगम का प्रबंधन। दोनों जगहों पर भारत के नागरिक ही कार्यरत हैं, मगर दोनों के दायित्वबोध का फर्क दर्शाता है कि हम देश के प्रति कितने संजीदा हैं। यह मात्र इसलिए है कि राष्ट्र हमारे लिए चारागाह है, जहां जो जी में आये करें, अधिकारों के लिए बात-बात पर बाहें मोड़ें, सरकार को आंखें तरेरें और कर्त्तव्यों से जी चुराएं और यह केवल इसलिए कि संविधान में दर्ज कर्त्तव्यों का पालन करना हम जरूरी नहीं मानते, क्योंकि इनके न मानने पर दंडात्मक व्यवस्था प्रभावी नहीं है।
गर गणतंत्र समारोहों में मौजूद किसी नेता, प्रशासक या नागरिक से पूछ लिया कि अनुच्छेद-51(क) में जिन कर्त्तव्यों की राष्ट्र आप से अपेक्षा करता है, वे क्या हैं तो कईयों को सांप सूंघ जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन की हंसी उड़ाते लोग नहीं अघाते, लेकिन इतना चिंतन कर सकें कि यह सफाई किसके लिए है? एक प्रधानमंत्री की चिंता को हमने नागरिक कर्त्तव्य के तौर क्यों नहीं देखा? गिरेबां मे झांकने का वक्त है।
अपने ही लोगों से भेदभाव और वैमनस्य न रखना भी मूल कर्त्तव्य का हिस्सा है। आतंकी दूसरे मुल्कों से हवा में उड़कर वार नहीं करते। वे गर देश में छुप कर किसी के सहयोग से हमला करते हैं तो ऐसे गद्दारों को अपने चरित्र के दोगलेपन को टटोलना होगा। इस देश की मिट्टी में हवा, पानी भोजन और जीवन जीने वाले ये समझें कि गद्दारों को न जीते जी, न मरने के बाद सम्मान नहीं मिला, न कभी मिल सकता है।यदि भारत के संविधान रूपी शास्त्र में हमें गलत कर्म करने पर सजा का प्रावधान है और अच्छे कर्म करने पर पुरस्कृत करने का विचार है।
सच्चाई यह है कि संविधान को समझना, जानना और अपनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी धार्मिक शास्त्र को समझना, जानना और मानना। आज एक और गणतंत्र दिवस ने हमारी चौखट पर दस्तक दी है। यह दिन है धन्यवाद का, यह दिन है देश के संविधान को समझने का। हमारे देश का संविधान ही हमारा वह सूत्र है जिसने पूरे देश को बांधा हुआ है। इस संविधान को एक शास्त्र की तरह ही समझना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब भी हम दुविधा में होते हैं तब शास्त्र ही हमें सही दिशा देते हैं और संविधान देश को।
 श्रीश पांडे
हर पर्व की अपनी एक संस्कृति है, परम्परा है, उसका दर्शन है और इसीलिए इनका हर वर्ष हमारे जीवन में आगमन होता है, ताकि उसका न सिर्फ स्मरण बना रहे, बल्कि जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, का अहसास देश, समाज और वहां के नागरिक करते रहें।
भारत को सांस्कृतिक भिन्नता का अजायबघर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में और कोई मुल्क नहीं जहां भारत जैसी बहुरंगी संस्कृति, धर्म, भाषा-बोली, खान-पान और ऋतुओं की विविधता विद्यमान हो।
इस देश की विकास यात्रा को वर्तमान तक लाने में अनेक बलिदान, त्याग और संघर्ष की अनेक स्वर्णिम शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इसी स्वर्णिम इतिहास को स्मरण रखने के बरक्स आजादी के बाद से भारत में दो राष्ट्रीय पर्वों की परम्परा बरकरार रखी गई है। इन दोनों पर्वों से देश का हर कोना परिचित है। पहला है आजादी का पर्व जिसकी नाभिनाल 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि से जुड़ी है,जब ब्रितानी हुकूमत के यूनानी जैक को उतारकर देश में तिरंगे को फहराया गया था। आजादी अपने आप में वृहद अर्थ लिए हुए है।
एक आजाद देश का नागरिक होने का अनुभव उस पीढ़ी ने बारीकी से किया होगा जिसने होशोहवास में गुलाम भारत से आजाद भारत में न सिर्फ सांसें ली हो, बल्कि इसके लिए एक लम्बा संघर्ष देखा हो, झेला हो। लेकिन आजादी मिलना एक अवस्था है, मगर उसको बनाए रखना दूसरी और कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्य के साथ देश की कानून व्यवस्था की रूपरेखा व इसका संचालन कैसे हो इसके लिए देश का समग्र एवं स्पष्ट संविधान आवश्यक है।
इसी संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 195० है। यहीं भारत के दूसरे राष्ट्रीय पर्व का आरंभ हुआ, जिसे हम आज एक बार फिर 'गणतंत्र दिवस’ के तौर पर इसकी 67 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संविधान यानि ऐसा निश्चित और अनिवार्य विधान या कानून जिसमें सभी को समानता देने की भावना निहित है।
दरअसल, गणतंत्र यानि ऐसा तंत्र जिसमें राज्य का प्रमुख अनुवांशिक न होकर जनता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित शख्स होगा। कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां शासन पद्धति लोकतांत्रिक होती है, पर राष्ट्राध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जाता। जैसे ब्रिटेन, जापान जहां राष्ट्राध्यक्ष सम्राट होता है, जिसके परिवार के सदस्य ही राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। इस मायने में ब्रिटेन और जापान रिपब्लिक नहीं है।
भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार है मगर राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) का चुनाव होता है, इसलिए यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार तो हो गया था, मगर इसे दो महीने बाद 26 जनवरी 195० को ही लागू क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कि 26 जनवरी 193० के लाहौर कांग्रेस-अधिवेशन में पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था और अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में इसकी मांग की थी।
हालांकि संविधान से नागरिकता, चुनाव और संसद जैसी व्यवस्थाएं तत्काल लागू हो गईं थीं। इसी प्रकार राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन वह 15 अगस्त 1947 से औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज बना था। इसी कार्यक्रम में श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्रध्वज डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भेंट किया।
आज भी गणतंत्र से मिली ताकत और कमजोरियों के सवाल हमारा ध्यान बरबस खींचते हैं। हालांकि 67 वर्षों का सफर कोई अधिक नहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हम गणतंत्र के अर्थ को समझ-बूझ न सकें हों। मगर विकास और नागरिक अधिकारों के संरक्षण में हमारा तंत्र धीमा रहा है। तो इसके पीछे दोहरे कारण हैं। पहला केन्द्र और राज्यों में स्थापित सरकारें रही हैं, तो दूसरा अधिकांश नागरिकों का देश के प्रति उदासीन रवैय्या। मोटे तौर पद देखें तो भारत में अवाम हर मुश्किल में सरकारों से आपेक्षा करती है कि वह उन्हें दामादों की तरह केयर करे। यह सही है कि सरकार का दायित्व है कि जनकल्याण उसके जिम्मे है, लेकिन नागरिक स्तर पर भी सजगता और देश के प्रति निष्ठा की प्रगाढ़ता दिखनी चाहिए। मगर सरकारी संसाधन हो या काम काज सबके प्रति हमारा लापरवाहीपूर्ण रुख नजर आता है।
मसलन, शिक्षा हो या व्यापार, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जहां निजी क्षेत्र काम कर रहा है और जहां सरकारी दोनों की व्यवस्थाओं और मानसिकता में साफ फर्क मौजूद है। एक निजी स्कूल या फैक्ट्री का प्रबंधन और एक सरकारी स्कूल या निगम का प्रबंधन। दोनों जगहों पर भारत के नागरिक ही कार्यरत हैं, मगर दोनों के दायित्वबोध का फर्क दर्शाता है कि हम देश के प्रति कितने संजीदा हैं। यह मात्र इसलिए है कि राष्ट्र हमारे लिए चारागाह है, जहां जो जी में आये करें, अधिकारों के लिए बात-बात पर बाहें मोड़ें, सरकार को आंखें तरेरें और कर्त्तव्यों से जी चुराएं और यह केवल इसलिए कि संविधान में दर्ज कर्त्तव्यों का पालन करना हम जरूरी नहीं मानते, क्योंकि इनके न मानने पर दंडात्मक व्यवस्था प्रभावी नहीं है।
गर गणतंत्र समारोहों में मौजूद किसी नेता, प्रशासक या नागरिक से पूछ लिया कि अनुच्छेद-51(क) में जिन कर्त्तव्यों की राष्ट्र आप से अपेक्षा करता है, वे क्या हैं तो कईयों को सांप सूंघ जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन की हंसी उड़ाते लोग नहीं अघाते, लेकिन इतना चिंतन कर सकें कि यह सफाई किसके लिए है? एक प्रधानमंत्री की चिंता को हमने नागरिक कर्त्तव्य के तौर क्यों नहीं देखा? गिरेबां मे झांकने का वक्त है।
अपने ही लोगों से भेदभाव और वैमनस्य न रखना भी मूल कर्त्तव्य का हिस्सा है। आतंकी दूसरे मुल्कों से हवा में उड़कर वार नहीं करते। वे गर देश में छुप कर किसी के सहयोग से हमला करते हैं तो ऐसे गद्दारों को अपने चरित्र के दोगलेपन को टटोलना होगा। इस देश की मिट्टी में हवा, पानी भोजन और जीवन जीने वाले ये समझें कि गद्दारों को न जीते जी, न मरने के बाद सम्मान नहीं मिला, न कभी मिल सकता है।यदि भारत के संविधान रूपी शास्त्र में हमें गलत कर्म करने पर सजा का प्रावधान है और अच्छे कर्म करने पर पुरस्कृत करने का विचार है।
सच्चाई यह है कि संविधान को समझना, जानना और अपनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी धार्मिक शास्त्र को समझना, जानना और मानना। आज एक और गणतंत्र दिवस ने हमारी चौखट पर दस्तक दी है। यह दिन है धन्यवाद का, यह दिन है देश के संविधान को समझने का। हमारे देश का संविधान ही हमारा वह सूत्र है जिसने पूरे देश को बांधा हुआ है। इस संविधान को एक शास्त्र की तरह ही समझना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब भी हम दुविधा में होते हैं तब शास्त्र ही हमें सही दिशा देते हैं और संविधान देश को।
श्रीश पांडे
हर पर्व की अपनी एक संस्कृति है, परम्परा है, उसका दर्शन है और इसीलिए इनका हर वर्ष हमारे जीवन में आगमन होता है, ताकि उसका न सिर्फ स्मरण बना रहे, बल्कि जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, का अहसास देश, समाज और वहां के नागरिक करते रहें।
भारत को सांस्कृतिक भिन्नता का अजायबघर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में और कोई मुल्क नहीं जहां भारत जैसी बहुरंगी संस्कृति, धर्म, भाषा-बोली, खान-पान और ऋतुओं की विविधता विद्यमान हो।
इस देश की विकास यात्रा को वर्तमान तक लाने में अनेक बलिदान, त्याग और संघर्ष की अनेक स्वर्णिम शौर्य गाथाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इसी स्वर्णिम इतिहास को स्मरण रखने के बरक्स आजादी के बाद से भारत में दो राष्ट्रीय पर्वों की परम्परा बरकरार रखी गई है। इन दोनों पर्वों से देश का हर कोना परिचित है। पहला है आजादी का पर्व जिसकी नाभिनाल 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि से जुड़ी है,जब ब्रितानी हुकूमत के यूनानी जैक को उतारकर देश में तिरंगे को फहराया गया था। आजादी अपने आप में वृहद अर्थ लिए हुए है।
एक आजाद देश का नागरिक होने का अनुभव उस पीढ़ी ने बारीकी से किया होगा जिसने होशोहवास में गुलाम भारत से आजाद भारत में न सिर्फ सांसें ली हो, बल्कि इसके लिए एक लम्बा संघर्ष देखा हो, झेला हो। लेकिन आजादी मिलना एक अवस्था है, मगर उसको बनाए रखना दूसरी और कहीं अधिक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए नागरिकों के अधिकार और कर्त्तव्य के साथ देश की कानून व्यवस्था की रूपरेखा व इसका संचालन कैसे हो इसके लिए देश का समग्र एवं स्पष्ट संविधान आवश्यक है।
इसी संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 195० है। यहीं भारत के दूसरे राष्ट्रीय पर्व का आरंभ हुआ, जिसे हम आज एक बार फिर 'गणतंत्र दिवस’ के तौर पर इसकी 67 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संविधान यानि ऐसा निश्चित और अनिवार्य विधान या कानून जिसमें सभी को समानता देने की भावना निहित है।
दरअसल, गणतंत्र यानि ऐसा तंत्र जिसमें राज्य का प्रमुख अनुवांशिक न होकर जनता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित शख्स होगा। कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां शासन पद्धति लोकतांत्रिक होती है, पर राष्ट्राध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जाता। जैसे ब्रिटेन, जापान जहां राष्ट्राध्यक्ष सम्राट होता है, जिसके परिवार के सदस्य ही राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। इस मायने में ब्रिटेन और जापान रिपब्लिक नहीं है।
भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार है मगर राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) का चुनाव होता है, इसलिए यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक प्रयासों के बाद 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार तो हो गया था, मगर इसे दो महीने बाद 26 जनवरी 195० को ही लागू क्यों किया गया? ऐसा इसलिए कि 26 जनवरी 193० के लाहौर कांग्रेस-अधिवेशन में पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया था और अध्यक्ष जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषण में इसकी मांग की थी।
हालांकि संविधान से नागरिकता, चुनाव और संसद जैसी व्यवस्थाएं तत्काल लागू हो गईं थीं। इसी प्रकार राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन वह 15 अगस्त 1947 से औपचारिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज बना था। इसी कार्यक्रम में श्रीमती हंसा मेहता ने राष्ट्रध्वज डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भेंट किया।
आज भी गणतंत्र से मिली ताकत और कमजोरियों के सवाल हमारा ध्यान बरबस खींचते हैं। हालांकि 67 वर्षों का सफर कोई अधिक नहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं कि हम गणतंत्र के अर्थ को समझ-बूझ न सकें हों। मगर विकास और नागरिक अधिकारों के संरक्षण में हमारा तंत्र धीमा रहा है। तो इसके पीछे दोहरे कारण हैं। पहला केन्द्र और राज्यों में स्थापित सरकारें रही हैं, तो दूसरा अधिकांश नागरिकों का देश के प्रति उदासीन रवैय्या। मोटे तौर पद देखें तो भारत में अवाम हर मुश्किल में सरकारों से आपेक्षा करती है कि वह उन्हें दामादों की तरह केयर करे। यह सही है कि सरकार का दायित्व है कि जनकल्याण उसके जिम्मे है, लेकिन नागरिक स्तर पर भी सजगता और देश के प्रति निष्ठा की प्रगाढ़ता दिखनी चाहिए। मगर सरकारी संसाधन हो या काम काज सबके प्रति हमारा लापरवाहीपूर्ण रुख नजर आता है।
मसलन, शिक्षा हो या व्यापार, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जहां निजी क्षेत्र काम कर रहा है और जहां सरकारी दोनों की व्यवस्थाओं और मानसिकता में साफ फर्क मौजूद है। एक निजी स्कूल या फैक्ट्री का प्रबंधन और एक सरकारी स्कूल या निगम का प्रबंधन। दोनों जगहों पर भारत के नागरिक ही कार्यरत हैं, मगर दोनों के दायित्वबोध का फर्क दर्शाता है कि हम देश के प्रति कितने संजीदा हैं। यह मात्र इसलिए है कि राष्ट्र हमारे लिए चारागाह है, जहां जो जी में आये करें, अधिकारों के लिए बात-बात पर बाहें मोड़ें, सरकार को आंखें तरेरें और कर्त्तव्यों से जी चुराएं और यह केवल इसलिए कि संविधान में दर्ज कर्त्तव्यों का पालन करना हम जरूरी नहीं मानते, क्योंकि इनके न मानने पर दंडात्मक व्यवस्था प्रभावी नहीं है।
गर गणतंत्र समारोहों में मौजूद किसी नेता, प्रशासक या नागरिक से पूछ लिया कि अनुच्छेद-51(क) में जिन कर्त्तव्यों की राष्ट्र आप से अपेक्षा करता है, वे क्या हैं तो कईयों को सांप सूंघ जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन की हंसी उड़ाते लोग नहीं अघाते, लेकिन इतना चिंतन कर सकें कि यह सफाई किसके लिए है? एक प्रधानमंत्री की चिंता को हमने नागरिक कर्त्तव्य के तौर क्यों नहीं देखा? गिरेबां मे झांकने का वक्त है।
अपने ही लोगों से भेदभाव और वैमनस्य न रखना भी मूल कर्त्तव्य का हिस्सा है। आतंकी दूसरे मुल्कों से हवा में उड़कर वार नहीं करते। वे गर देश में छुप कर किसी के सहयोग से हमला करते हैं तो ऐसे गद्दारों को अपने चरित्र के दोगलेपन को टटोलना होगा। इस देश की मिट्टी में हवा, पानी भोजन और जीवन जीने वाले ये समझें कि गद्दारों को न जीते जी, न मरने के बाद सम्मान नहीं मिला, न कभी मिल सकता है।यदि भारत के संविधान रूपी शास्त्र में हमें गलत कर्म करने पर सजा का प्रावधान है और अच्छे कर्म करने पर पुरस्कृत करने का विचार है।
सच्चाई यह है कि संविधान को समझना, जानना और अपनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी धार्मिक शास्त्र को समझना, जानना और मानना। आज एक और गणतंत्र दिवस ने हमारी चौखट पर दस्तक दी है। यह दिन है धन्यवाद का, यह दिन है देश के संविधान को समझने का। हमारे देश का संविधान ही हमारा वह सूत्र है जिसने पूरे देश को बांधा हुआ है। इस संविधान को एक शास्त्र की तरह ही समझना चाहिए। क्योंकि जीवन में जब भी हम दुविधा में होते हैं तब शास्त्र ही हमें सही दिशा देते हैं और संविधान देश को।
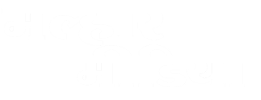
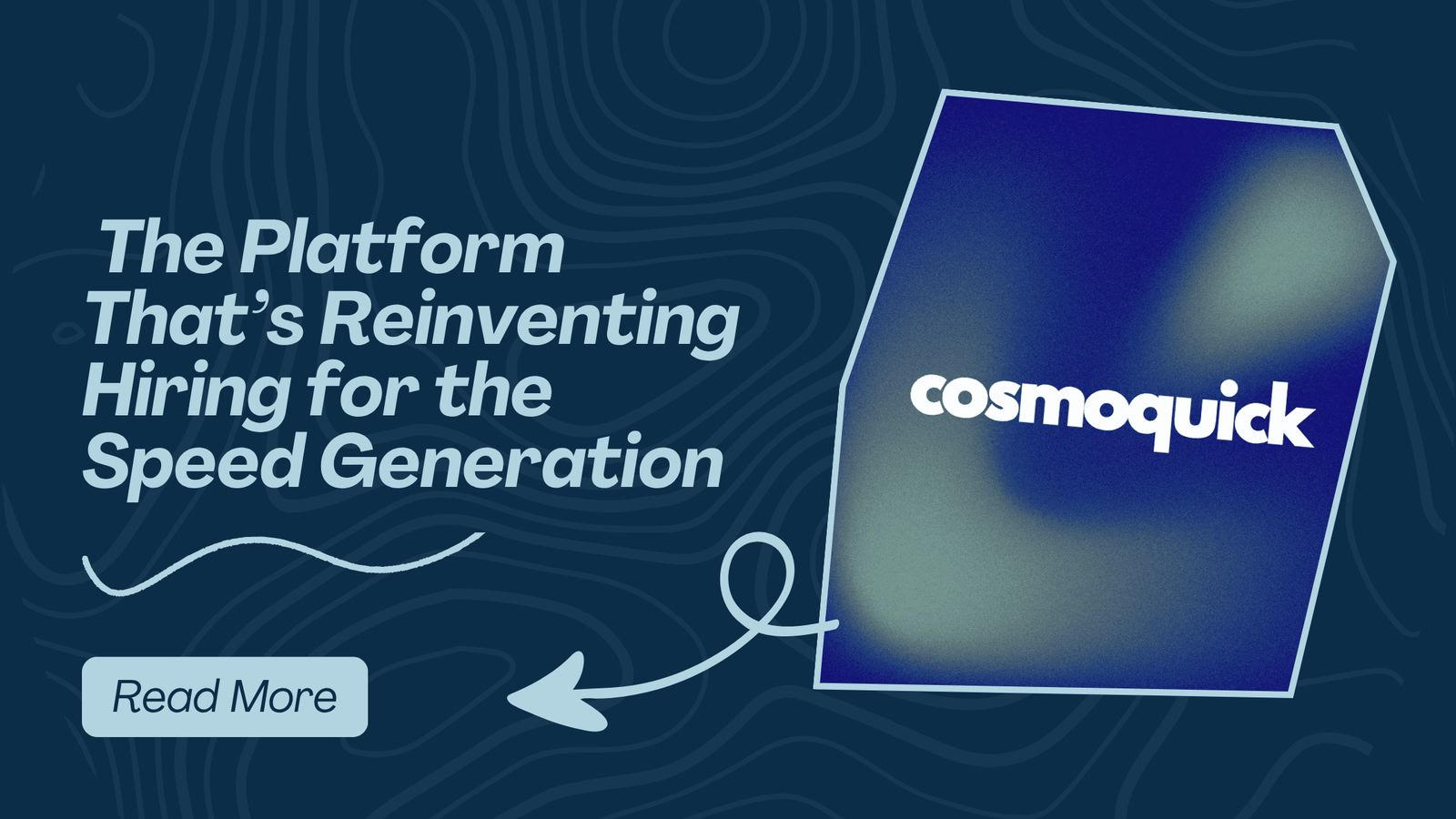





Comments