
अरुण कुमार डनायक।
चार दिन के सैन्य तनाव के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम लागू हुआ, जो शांति की दिशा में एक सकारात्मक लेकिन नाजुक कदम माना जा रहा है। संघर्षविराम के पश्चात सीमित स्तर पर हुई गोलीबारी को मीडिया द्वारा अत्यधिक प्रचारित किया गया, जिससे इस पहल की स्थायित्वशीलता पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संघर्षविराम लागू कराने संबंधी दावों ने भारत में एक नई बहस छेड़ दी है और भारत सरकार की ओर से अमेरिकी दावों पर समय रहते स्पष्ट व ठोस प्रतिक्रिया का अभाव आलोचना का विषय बना।
अमेरिका ने भारत-पाकिस्तान की एक तटस्थ जगह पर “रचनात्मक वार्ता” शुरू करने की बात कही | भारत अभी तक किसी भी ऐसी व्यवस्था को अस्वीकार करता आया है जिसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाए। यह प्रस्ताव, भारत द्वारा पूर्व में अस्वीकार किया जा चुका है और इससे स्पष्ट होता है कि ट्रंप प्रशासन भारत की कश्मीर नीति को भलीभांति नहीं समझता है। भारत ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी नीति स्पष्ट कर दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे नाकाफी माना जा रहा है ।
भारत की असहमति कश्मीर विवाद सहित बहुपक्षीय और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से जुड़े नकारात्मक अनुभवों का परिणाम है। भारतीयों का मानना है कि 1947-48 के कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन के प्रभाव में अमेरिका ने भेदभावपूर्ण तरीके से बहस को प्रभावित कर पाकिस्तान का समर्थन किया ।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र में उठाया। वहाँ शेख अब्दुल्ला सहित भारतीय कूटनीतिज्ञों के कानूनी और सुरक्षा तर्कों को पर्याप्त महत्व नहीं मिला। भारत ने सेना की सलाह व संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 31 दिसंबर 1948 को युद्धविराम लागू किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह प्रस्ताव को लागू नहीं होने दिया। 1960 के दशक की शुरुआत तक संयुक्त राष्ट्र ने इस मुद्दे पर रुचि खो दी। बाद में, पश्चिमी देशों के दबाव और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते भारत और पाकिस्तान ने कई बार आपसी मतभेदों को सुलझाने के लिए वार्ताएं कीं। हालांकि, ये प्रयास अधिकांशतः विफल ही रहे। अपवादस्वरूप 1960 में हुई सिंधु जल संधि को एक सफल जल-बंटवारा समझौता माना जाता है, जो अब स्थगित कर दी गई है। पंडित नेहरू ने भारत-पाक संबंध सुधारने के कई प्रयास किए, पर विपक्ष ने उनकी लगातार आलोचना की। आज भी कई लोग कश्मीर समस्या के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानते हैं।
1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद, पाकिस्तान के मित्र अमेरिका ने कश्मीर विवाद सुलझाने में रुचि खो दी, और सोवियत संघ ने ताशकंद में समझौता वार्ता कराई। भारत को इस बार भी पक्षपात का सामना करना पड़ा, उसे कोई लाभ नहीं मिला, ताशकंद वार्ता के दौरान सदमे का शिकार हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। पश्चिमी देशों की चालबाज़ी, अमेरिकी दबाव और पाकिस्तान के प्रति उनके झुकाव ने भारतीय नीति-निर्माताओं पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिससे पाकिस्तान के प्रति अधिक सतर्कता और सावधानी का भाव जागृत हुआ।
1971 के युद्ध ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को नया मोड़ दिया। बांग्लादेश का निर्माण, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण और पश्चिमी मोर्चे पर रणनीतिक बढ़त के बाद, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में वार्ता की। शिमला समझौते के ज़रिए पुत्री ने कश्मीर को अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में ले जाने वाली पिता की नीति को विराम देते हुए, इसे भारत-पाक के बीच एक द्विपक्षीय विषय के रूप में पुनर्परिभाषित कर दिया । दोनों पक्ष विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने और बल प्रयोग से बचने पर सहमत हुए। भारत ने स्थायी शांति, बेहतर द्विपक्षीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों का सम्मान करते हुए 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया और पश्चिमी मोर्चे की जीती हुई जमीन लौटा दी। हालांकि, पाकिस्तान ने बार-बार शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए विवाद को बहुपक्षीय मंचों पर उठाया, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया।
भारत ने पाकिस्तान के साथ विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। एक मजबूत लोकतंत्र होने के नाते कश्मीर जैसे मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद स्वाभाविक हैं, फिर भी अधिकांश भारतीय तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप या संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अस्वीकार करेंगे ।
वर्तमान संघर्षविराम, स्पष्ट रूप से, एक स्वागतयोग्य, पर नाजुक कदम है। यह लंबे संघर्ष के समाधान की दिशा में निर्णायक कदम होगा, इसमें संदेह है। इस्लामाबाद, भारत के विरुद्ध आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल कर भारत में हिंसा व अस्थिरता फैलाने के उद्देश्य से काम करता है। जिससे कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास बाधित हुए हैं। पहलगाम में धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा की घटना के माध्यम से उसने भारत में सांप्रदायिक अस्थिरता भड़काने की कोशिश की। साथ ही, खुद को भारतीय आक्रामकता का शिकार बताकर इस्लामाबाद ने ट्रंप प्रशासन को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता का भरोसा दिलाया, यह दावा करते हुए कि यह परमाणु युद्ध को रोक सकता है। उसे चीन, तुर्की, अजरबैजान का प्रत्यक्ष और इस्लामिक सहयोग संगठन का परोक्ष समर्थन प्राप्त है। भारत के विरोध के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 2.423 बिलियन डॉलर के दो ऋण अभी हाल में दिए हैं । हालांकि यह आर्थिक स्थिरता के लिए बताया गया, लेकिन इसका उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में हो सकता है। आर्थिक संकट से जूझता यह देश चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के कारण काफी हद तक चीन के प्रभाव में है। बांग्लादेश भी चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की अप्रभावी लोकतांत्रिक व्यवस्था, कमजोर सरकार और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, जो भारत के प्रति कट्टर रवैया रखते हैं, के नेतृत्व में भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण नीति जारी रहने की संभावना है।
इस प्रकार, वर्तमान संघर्षविराम न केवल दो देशों के बीच सीमित सैन्य राहत है, बल्कि यह उस जटिल कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य की भी याद दिलाता है जिसमें भारत को अपनी संप्रभुता, सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय स्थिति को संतुलित करना पड़ता है। अमेरिकी हस्तक्षेप के प्रयास हों या पाकिस्तान की छद्म युद्धनीति — भारत की विदेश नीति का परीक्षण अभी शेष है।
(लेखक गांधी विचारों के अध्येता और समाजसेवी हैं )
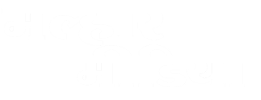
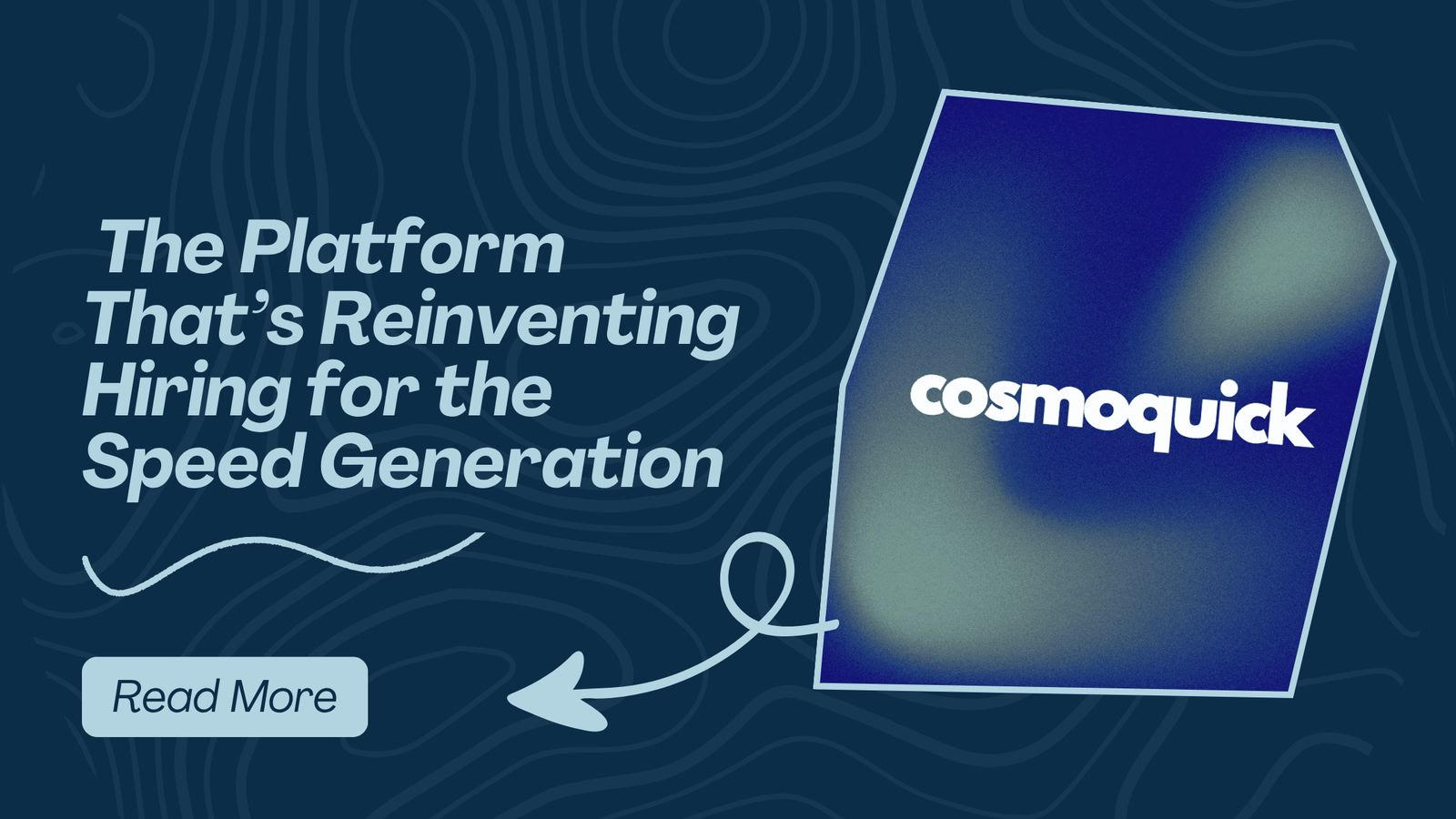






Comments