 श्रीश पांडे।
श्रीश पांडे।
वैश्वीकरण की अवधारणा और व्यवस्था ने विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। इसके पीछे संचार साधनों की भूमिका निर्विवाद है। आधुनिक संचार का पहला तंत्र प्रिंट मीडिया था, जिसमें अखबार पत्र-पत्रिकाएं, जर्नल आदि को शुमार किया जा सकता है। तब इनके प्रसार के लिए हॉकर और डाक विभाग का व्यवस्थित तंत्र सहयोगी बना। बाद के वर्षों में टेलीवीजन क्रांति ने संचार को न सिर्फ अविश्वसनीय गति बल्कि इसके सचित्र-चलचित्र को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकेंडों में पहुंचना मुमकिन कर दिया।
लेकिन वर्ष 1995 में आई 'इंटननेट क्रांति’ ने संचार के साधनों को और आद्यतन किया। यह क्रांति 2005 में किशोर हुई और बाद में तरल होकर अपने पांव तब पसारने शुरु किए जब स्मार्टफोन का विस्तार हुआ। 2014-15 आते-आते यह क्रांति युवा होकर हर हाथ में स्मार्ट फोन के रूप में दिखने लगी। संचार की अब तक हुई सबसे बड़ी क्रांति को स्मार्ट फोन और इंटरनेट के मेल ने मानो पंख लगा दिए हों।
इस मुकाम पर पहले से चले आ रहे मीडिया के दो स्वरूपों 'प्रिंट’ और 'इलेक्ट्रॉनिक’ में एक नया स्वरूप 'सोशल मीडिया’ के तौर जुड़ा। 'सोशल मीडिया’ नाम से ही अपने अर्थ को लिए है। यानि सामाजिक संचार सम्पर्क ने हर शख्स को देश दुनिया में हो रही हर अच्छी बुरी गतिविधि से जोड़ दिया। आज आलम है कि दुनिया में जो भी घट रहा है उसमें हर कोई बढ़-चढ़ कर अपनी राय देने को आतुर है। हालांकि इसने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के लिहाज से सर्वसुविधायुक्त समान अवसर पेश किये हैं, इसीलिए आज ऐसे लोग भी अपनी बात कह सुन पा रहे हैं, जो इससे मरहूम थे।
नि:संदेह इंटरनेट, लैपटॉप और स्मार्ट फोन के बढ़ते प्रयोग ने अभिव्यक्ति के संसाधनों में अभूतपूर्व इजाफा किया है। इसका लाभ यह हुआ कि एक स्थान पर जिन अखबारों को पढ़ने की साध हम पूरी नहीं कर सकते उन्हें अपने स्मार्ट फोन से पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज मीडिया में वेब मीडिया लोकप्रिय और चर्चित माध्यम बन चुका है।
आज दुनिया में दो तरह की सिविलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। 'वर्चुअल’ और 'फिजीकल’ सिविलाइजेशन। आने वाले समय में जल्द ही दुनिया की अधिकांश आबादी इंटरनेट पर होगी। दरअसल, इंटरनेट एक ऐसी तकनीक के रूप में हमारे सामने आया है, जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और सर्वहिताय है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया हैं, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रख पाते हैं। यहीं से सामाजिक मीडिया का स्वरूप विकसित हुआ है।
जन सामान्य तक पहुंच होने के कारण सामाजिक मीडिया को लोगों तक विज्ञापन पहुंचाने के सबसे अच्छा जरिया समझा जाता है। हाल ही के कुछ एक सालों में इंडस्ट्री में ऐसी क्रांति देखी जा रही है। फेसबुक, टिवटर जैसे सोशल मीडिया मंच पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाता है जिसमें उनकी आयु, रुचि, लिंग, गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं।
इन विज्ञापनों के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। जब कोई विषय वस्तु लोकप्रिय होती तो उसके लाभों के साथ उसकी चुनौतियां भी होती हैं। इसके दोनों पक्षों का परीक्षण करें तो वेब मीडिया की भूमिका को परखा जा सकता है। इसकी अन्य मीडिया माध्यमों से तुलना करके इसे सहज जांचा जा सकता है।
मध्यप्रदेश शासन ने समाचार वेबसाईट संचालकों को बाकायदा सम्पादक होने दर्जा देने का मन बनाया है। यह सम्भावना प्रिंट के बोझिल और खर्चीले साधनों का बड़ा विकल्प बन कर सामने आ रहा है। वेब मीडिया में खबरें त्वरित उपलब्ध होती हैं जिनमें निष्पक्षता का समावेश रहता है। क्योंकि फिलहाल विज्ञापन पार्टियों का वैसा दबाव यहां नहीं जैसा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राय: दिखता है। कई अखबार और चैनल तो 'खाओ-कमाओ’ की ठेकेनुमा संस्कृति पर संचालित हैं।
फिर अखबार और चैनल चलाना तभी सम्भव है जब बड़ी रकम के खर्च की व्यवस्था मालिकों के पास हो। क्योंकि पर्याप्त’ विज्ञापनों के आभाव में यह कार्य लम्बे समय तक असम्भव सा है। वहीं वेव मीडिया में यही काम कम खर्चे में संचालित होना मुमकिन है। हालांकि यहां भी विज्ञापनों की दरकार होती है, क्योंकि आपरेटर, रिपोर्टर, सम्पादकों की जरूरत होती है जिनकी तनख्वाह देना वेब मीडिया संचालक के जिम्मे होता है।
यद्यपि अब कुछ स्थापित और लोकप्रिय मीडिया साइडों को विज्ञापन मिलने लगे हैं, लेकिन अभी पर्याप्त’ नहीं। सरकार को इसे बढ़ावा देना होगा क्योंकि जहां वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाखों करोड़ों के विज्ञापन देने में गुरेज नहीं करते, तो उसे कम खर्चीले, कागज की बचत करने वाले वेब मीडिया को अधिक सहयोग प्रोत्साहन देने पर बल देना होगा।
यह सच है कि अभी स्मार्ट फोन और कम्पयूटर, इंटरनेट हर आदमी के हाथों में नहीं आया है, लेकिन स्मार्ट फोन जिस गति से अपना विस्तार कर रहे हैं उससे वह दिन दूर नहीं जब लोग समाचारों के लिए समाचार पत्रों या चैनलों की ओर जाने के बजाय वेब की तरफ जायेंगे।
देश में कई ऐसी वेब मीडिया साइड सक्रिय तौर कार्यरत हैं। यहां तक अखबार भी अब छापने के बजाय उसे बनाकर वेव मीडिया पर अपलोड कर जनता तक पहुंचने की कोशिशें शुरु हो गई हैं।
निश्चित तौर आने वाला समय वेब मीडिया का होगा। जीवन की कार्यसंस्कृति में जिस तरह से समयाभाव नमूदार हो रहा है उसमें अखबार पढ़ने और फुरसत में बैठ टीवी देखने की गुंजाइश कम ही होगी। ऐसे में स्मार्ट फोन जो 24 घंटे व्यक्ति के साथ रहता है समाचारों और जानकारियों से रू-ब-रू होने का प्रमुख साधन होगा। फिलहाल वेब मीडिया अपनी चुनौतियों और सरोकारों के साथ अवाम का ध्यान खींच रहा है। फेसबुक और टिवटर इसके बड़े वैश्विक उदाहरण सामने हैं। कोई भी शुरुआत भले छोटी लगे मगर समय के साथ वह अपनी पैठ और उपयोगिता साबित कर ही देती है और ऐसी सम्भावनाओं से वेब मीडिया भरपूर है।
लेखक मध्यप्रदेश जनसंदेश के संपादक हैं।
 श्रीश पांडे।
वैश्वीकरण की अवधारणा और व्यवस्था ने विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। इसके पीछे संचार साधनों की भूमिका निर्विवाद है। आधुनिक संचार का पहला तंत्र प्रिंट मीडिया था, जिसमें अखबार पत्र-पत्रिकाएं, जर्नल आदि को शुमार किया जा सकता है। तब इनके प्रसार के लिए हॉकर और डाक विभाग का व्यवस्थित तंत्र सहयोगी बना। बाद के वर्षों में टेलीवीजन क्रांति ने संचार को न सिर्फ अविश्वसनीय गति बल्कि इसके सचित्र-चलचित्र को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकेंडों में पहुंचना मुमकिन कर दिया।
लेकिन वर्ष 1995 में आई 'इंटननेट क्रांति’ ने संचार के साधनों को और आद्यतन किया। यह क्रांति 2005 में किशोर हुई और बाद में तरल होकर अपने पांव तब पसारने शुरु किए जब स्मार्टफोन का विस्तार हुआ। 2014-15 आते-आते यह क्रांति युवा होकर हर हाथ में स्मार्ट फोन के रूप में दिखने लगी। संचार की अब तक हुई सबसे बड़ी क्रांति को स्मार्ट फोन और इंटरनेट के मेल ने मानो पंख लगा दिए हों।
इस मुकाम पर पहले से चले आ रहे मीडिया के दो स्वरूपों 'प्रिंट’ और 'इलेक्ट्रॉनिक’ में एक नया स्वरूप 'सोशल मीडिया’ के तौर जुड़ा। 'सोशल मीडिया’ नाम से ही अपने अर्थ को लिए है। यानि सामाजिक संचार सम्पर्क ने हर शख्स को देश दुनिया में हो रही हर अच्छी बुरी गतिविधि से जोड़ दिया। आज आलम है कि दुनिया में जो भी घट रहा है उसमें हर कोई बढ़-चढ़ कर अपनी राय देने को आतुर है। हालांकि इसने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के लिहाज से सर्वसुविधायुक्त समान अवसर पेश किये हैं, इसीलिए आज ऐसे लोग भी अपनी बात कह सुन पा रहे हैं, जो इससे मरहूम थे।
नि:संदेह इंटरनेट, लैपटॉप और स्मार्ट फोन के बढ़ते प्रयोग ने अभिव्यक्ति के संसाधनों में अभूतपूर्व इजाफा किया है। इसका लाभ यह हुआ कि एक स्थान पर जिन अखबारों को पढ़ने की साध हम पूरी नहीं कर सकते उन्हें अपने स्मार्ट फोन से पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज मीडिया में वेब मीडिया लोकप्रिय और चर्चित माध्यम बन चुका है।
आज दुनिया में दो तरह की सिविलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। 'वर्चुअल’ और 'फिजीकल’ सिविलाइजेशन। आने वाले समय में जल्द ही दुनिया की अधिकांश आबादी इंटरनेट पर होगी। दरअसल, इंटरनेट एक ऐसी तकनीक के रूप में हमारे सामने आया है, जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और सर्वहिताय है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया हैं, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रख पाते हैं। यहीं से सामाजिक मीडिया का स्वरूप विकसित हुआ है।
जन सामान्य तक पहुंच होने के कारण सामाजिक मीडिया को लोगों तक विज्ञापन पहुंचाने के सबसे अच्छा जरिया समझा जाता है। हाल ही के कुछ एक सालों में इंडस्ट्री में ऐसी क्रांति देखी जा रही है। फेसबुक, टिवटर जैसे सोशल मीडिया मंच पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाता है जिसमें उनकी आयु, रुचि, लिंग, गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं।
इन विज्ञापनों के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। जब कोई विषय वस्तु लोकप्रिय होती तो उसके लाभों के साथ उसकी चुनौतियां भी होती हैं। इसके दोनों पक्षों का परीक्षण करें तो वेब मीडिया की भूमिका को परखा जा सकता है। इसकी अन्य मीडिया माध्यमों से तुलना करके इसे सहज जांचा जा सकता है।
मध्यप्रदेश शासन ने समाचार वेबसाईट संचालकों को बाकायदा सम्पादक होने दर्जा देने का मन बनाया है। यह सम्भावना प्रिंट के बोझिल और खर्चीले साधनों का बड़ा विकल्प बन कर सामने आ रहा है। वेब मीडिया में खबरें त्वरित उपलब्ध होती हैं जिनमें निष्पक्षता का समावेश रहता है। क्योंकि फिलहाल विज्ञापन पार्टियों का वैसा दबाव यहां नहीं जैसा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राय: दिखता है। कई अखबार और चैनल तो 'खाओ-कमाओ’ की ठेकेनुमा संस्कृति पर संचालित हैं।
फिर अखबार और चैनल चलाना तभी सम्भव है जब बड़ी रकम के खर्च की व्यवस्था मालिकों के पास हो। क्योंकि पर्याप्त’ विज्ञापनों के आभाव में यह कार्य लम्बे समय तक असम्भव सा है। वहीं वेव मीडिया में यही काम कम खर्चे में संचालित होना मुमकिन है। हालांकि यहां भी विज्ञापनों की दरकार होती है, क्योंकि आपरेटर, रिपोर्टर, सम्पादकों की जरूरत होती है जिनकी तनख्वाह देना वेब मीडिया संचालक के जिम्मे होता है।
यद्यपि अब कुछ स्थापित और लोकप्रिय मीडिया साइडों को विज्ञापन मिलने लगे हैं, लेकिन अभी पर्याप्त’ नहीं। सरकार को इसे बढ़ावा देना होगा क्योंकि जहां वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाखों करोड़ों के विज्ञापन देने में गुरेज नहीं करते, तो उसे कम खर्चीले, कागज की बचत करने वाले वेब मीडिया को अधिक सहयोग प्रोत्साहन देने पर बल देना होगा।
यह सच है कि अभी स्मार्ट फोन और कम्पयूटर, इंटरनेट हर आदमी के हाथों में नहीं आया है, लेकिन स्मार्ट फोन जिस गति से अपना विस्तार कर रहे हैं उससे वह दिन दूर नहीं जब लोग समाचारों के लिए समाचार पत्रों या चैनलों की ओर जाने के बजाय वेब की तरफ जायेंगे।
देश में कई ऐसी वेब मीडिया साइड सक्रिय तौर कार्यरत हैं। यहां तक अखबार भी अब छापने के बजाय उसे बनाकर वेव मीडिया पर अपलोड कर जनता तक पहुंचने की कोशिशें शुरु हो गई हैं।
निश्चित तौर आने वाला समय वेब मीडिया का होगा। जीवन की कार्यसंस्कृति में जिस तरह से समयाभाव नमूदार हो रहा है उसमें अखबार पढ़ने और फुरसत में बैठ टीवी देखने की गुंजाइश कम ही होगी। ऐसे में स्मार्ट फोन जो 24 घंटे व्यक्ति के साथ रहता है समाचारों और जानकारियों से रू-ब-रू होने का प्रमुख साधन होगा। फिलहाल वेब मीडिया अपनी चुनौतियों और सरोकारों के साथ अवाम का ध्यान खींच रहा है। फेसबुक और टिवटर इसके बड़े वैश्विक उदाहरण सामने हैं। कोई भी शुरुआत भले छोटी लगे मगर समय के साथ वह अपनी पैठ और उपयोगिता साबित कर ही देती है और ऐसी सम्भावनाओं से वेब मीडिया भरपूर है।
लेखक मध्यप्रदेश जनसंदेश के संपादक हैं।
श्रीश पांडे।
वैश्वीकरण की अवधारणा और व्यवस्था ने विश्व को एक गांव में तब्दील कर दिया है। इसके पीछे संचार साधनों की भूमिका निर्विवाद है। आधुनिक संचार का पहला तंत्र प्रिंट मीडिया था, जिसमें अखबार पत्र-पत्रिकाएं, जर्नल आदि को शुमार किया जा सकता है। तब इनके प्रसार के लिए हॉकर और डाक विभाग का व्यवस्थित तंत्र सहयोगी बना। बाद के वर्षों में टेलीवीजन क्रांति ने संचार को न सिर्फ अविश्वसनीय गति बल्कि इसके सचित्र-चलचित्र को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकेंडों में पहुंचना मुमकिन कर दिया।
लेकिन वर्ष 1995 में आई 'इंटननेट क्रांति’ ने संचार के साधनों को और आद्यतन किया। यह क्रांति 2005 में किशोर हुई और बाद में तरल होकर अपने पांव तब पसारने शुरु किए जब स्मार्टफोन का विस्तार हुआ। 2014-15 आते-आते यह क्रांति युवा होकर हर हाथ में स्मार्ट फोन के रूप में दिखने लगी। संचार की अब तक हुई सबसे बड़ी क्रांति को स्मार्ट फोन और इंटरनेट के मेल ने मानो पंख लगा दिए हों।
इस मुकाम पर पहले से चले आ रहे मीडिया के दो स्वरूपों 'प्रिंट’ और 'इलेक्ट्रॉनिक’ में एक नया स्वरूप 'सोशल मीडिया’ के तौर जुड़ा। 'सोशल मीडिया’ नाम से ही अपने अर्थ को लिए है। यानि सामाजिक संचार सम्पर्क ने हर शख्स को देश दुनिया में हो रही हर अच्छी बुरी गतिविधि से जोड़ दिया। आज आलम है कि दुनिया में जो भी घट रहा है उसमें हर कोई बढ़-चढ़ कर अपनी राय देने को आतुर है। हालांकि इसने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति के लिहाज से सर्वसुविधायुक्त समान अवसर पेश किये हैं, इसीलिए आज ऐसे लोग भी अपनी बात कह सुन पा रहे हैं, जो इससे मरहूम थे।
नि:संदेह इंटरनेट, लैपटॉप और स्मार्ट फोन के बढ़ते प्रयोग ने अभिव्यक्ति के संसाधनों में अभूतपूर्व इजाफा किया है। इसका लाभ यह हुआ कि एक स्थान पर जिन अखबारों को पढ़ने की साध हम पूरी नहीं कर सकते उन्हें अपने स्मार्ट फोन से पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज मीडिया में वेब मीडिया लोकप्रिय और चर्चित माध्यम बन चुका है।
आज दुनिया में दो तरह की सिविलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। 'वर्चुअल’ और 'फिजीकल’ सिविलाइजेशन। आने वाले समय में जल्द ही दुनिया की अधिकांश आबादी इंटरनेट पर होगी। दरअसल, इंटरनेट एक ऐसी तकनीक के रूप में हमारे सामने आया है, जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और सर्वहिताय है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया हैं, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रख पाते हैं। यहीं से सामाजिक मीडिया का स्वरूप विकसित हुआ है।
जन सामान्य तक पहुंच होने के कारण सामाजिक मीडिया को लोगों तक विज्ञापन पहुंचाने के सबसे अच्छा जरिया समझा जाता है। हाल ही के कुछ एक सालों में इंडस्ट्री में ऐसी क्रांति देखी जा रही है। फेसबुक, टिवटर जैसे सोशल मीडिया मंच पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाता है जिसमें उनकी आयु, रुचि, लिंग, गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं।
इन विज्ञापनों के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं। जब कोई विषय वस्तु लोकप्रिय होती तो उसके लाभों के साथ उसकी चुनौतियां भी होती हैं। इसके दोनों पक्षों का परीक्षण करें तो वेब मीडिया की भूमिका को परखा जा सकता है। इसकी अन्य मीडिया माध्यमों से तुलना करके इसे सहज जांचा जा सकता है।
मध्यप्रदेश शासन ने समाचार वेबसाईट संचालकों को बाकायदा सम्पादक होने दर्जा देने का मन बनाया है। यह सम्भावना प्रिंट के बोझिल और खर्चीले साधनों का बड़ा विकल्प बन कर सामने आ रहा है। वेब मीडिया में खबरें त्वरित उपलब्ध होती हैं जिनमें निष्पक्षता का समावेश रहता है। क्योंकि फिलहाल विज्ञापन पार्टियों का वैसा दबाव यहां नहीं जैसा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्राय: दिखता है। कई अखबार और चैनल तो 'खाओ-कमाओ’ की ठेकेनुमा संस्कृति पर संचालित हैं।
फिर अखबार और चैनल चलाना तभी सम्भव है जब बड़ी रकम के खर्च की व्यवस्था मालिकों के पास हो। क्योंकि पर्याप्त’ विज्ञापनों के आभाव में यह कार्य लम्बे समय तक असम्भव सा है। वहीं वेव मीडिया में यही काम कम खर्चे में संचालित होना मुमकिन है। हालांकि यहां भी विज्ञापनों की दरकार होती है, क्योंकि आपरेटर, रिपोर्टर, सम्पादकों की जरूरत होती है जिनकी तनख्वाह देना वेब मीडिया संचालक के जिम्मे होता है।
यद्यपि अब कुछ स्थापित और लोकप्रिय मीडिया साइडों को विज्ञापन मिलने लगे हैं, लेकिन अभी पर्याप्त’ नहीं। सरकार को इसे बढ़ावा देना होगा क्योंकि जहां वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाखों करोड़ों के विज्ञापन देने में गुरेज नहीं करते, तो उसे कम खर्चीले, कागज की बचत करने वाले वेब मीडिया को अधिक सहयोग प्रोत्साहन देने पर बल देना होगा।
यह सच है कि अभी स्मार्ट फोन और कम्पयूटर, इंटरनेट हर आदमी के हाथों में नहीं आया है, लेकिन स्मार्ट फोन जिस गति से अपना विस्तार कर रहे हैं उससे वह दिन दूर नहीं जब लोग समाचारों के लिए समाचार पत्रों या चैनलों की ओर जाने के बजाय वेब की तरफ जायेंगे।
देश में कई ऐसी वेब मीडिया साइड सक्रिय तौर कार्यरत हैं। यहां तक अखबार भी अब छापने के बजाय उसे बनाकर वेव मीडिया पर अपलोड कर जनता तक पहुंचने की कोशिशें शुरु हो गई हैं।
निश्चित तौर आने वाला समय वेब मीडिया का होगा। जीवन की कार्यसंस्कृति में जिस तरह से समयाभाव नमूदार हो रहा है उसमें अखबार पढ़ने और फुरसत में बैठ टीवी देखने की गुंजाइश कम ही होगी। ऐसे में स्मार्ट फोन जो 24 घंटे व्यक्ति के साथ रहता है समाचारों और जानकारियों से रू-ब-रू होने का प्रमुख साधन होगा। फिलहाल वेब मीडिया अपनी चुनौतियों और सरोकारों के साथ अवाम का ध्यान खींच रहा है। फेसबुक और टिवटर इसके बड़े वैश्विक उदाहरण सामने हैं। कोई भी शुरुआत भले छोटी लगे मगर समय के साथ वह अपनी पैठ और उपयोगिता साबित कर ही देती है और ऐसी सम्भावनाओं से वेब मीडिया भरपूर है।
लेखक मध्यप्रदेश जनसंदेश के संपादक हैं।
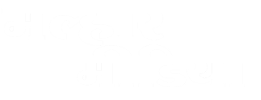
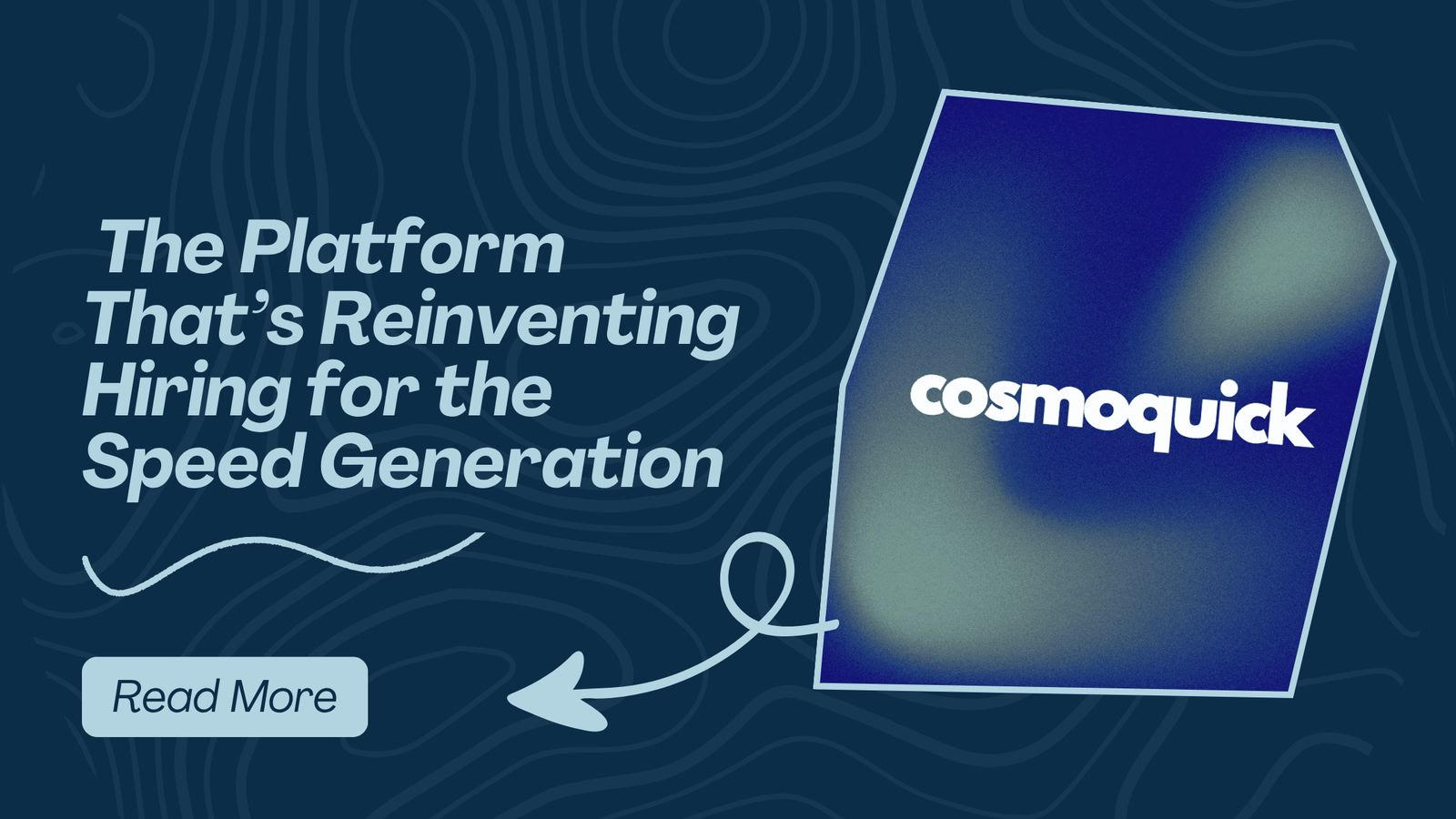





Comments