 अमित बैजनाथ गर्ग।
अमित बैजनाथ गर्ग।
आजादी से लेकर आज तक असमिया संघर्ष सभी का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। चाय के बागानों और आदिवासी इलाकों के लिए मशहूर असम में बोडो संघर्ष उसकी खूबसूरती पर दाग लगने जैसा है। बहरहाल, संघर्ष की इस कड़ी में बोडोलैंड के चिरांग जिले के रौमई गांव में कपड़े बुनते महिलाओं के समूह दुनिया को स्वावलंबी बनने की सीख दे रहे हैं। असमिया महिला बुनकरों की यह सीख महात्मा गांधी के मंत्र को साकार कर रही है। हालांकि इन महिलाओं में से कई के चेहरों पर कोई भाव नहीं होता। जिंदगी की कशमकश में उन्होंने खुद को पहचानना और यहां तक कि सजना-संवरना भी छोड़ दिया है। शायद यही कुछ ऐसा है, जो असमिया संघर्ष को आज भी एक आवाज दिए हुए है। ऐसी आवाज, जो कभी दिल्ली तक ठीक ढंग से नहीं पहुंची।
अक्सर हम असम को केवल बोडो समस्या के लिए याद करते हैं, लेकिन इसके इतर भी वहां बहुत कुछ है। असम के इन्हीं बोडोलैंड क्षेत्रों की महिला बोडो बुनकरों ने अपने हुनर से महिला सशक्तीकरण की नई ईबारत लिखना शुरू कर दिया है। राजस्थान की तरह असम की इन आदिवासी महिलाओं को भी कुदरत ने पिछड़ेपन का अभिशाप देकर भेजा है। बावजूद इसके, इन बोडो महिलाओं ने बुनकरी की कला के जरिए अपने हाथों का हुनर दुनिया के सामने पेश किया है। खास बात यह भी है कि इनके बुने हुए कपड़े इनकी कार्य-कुशलता को खुद-ब-खुद बयां करते हैं।
असम के चिरांग जिले के रौमेरी गांव की इन महिला बुनकरों के बनाए कपड़ों की पहचान सात समंदर पार तक है। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आंट संस्था की ओर से संचालित की जा रही है 'आगोर डागरा अफाद' यानी कि बोडो बुनकरों के हस्तनिर्मित कपड़े। ये केवल कपड़े नहीं हैं, बल्कि उन हजारों बोडो महिलाओं का जुनून है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। कपड़े बुनते महिलाओं के समूह के समूह पूरी दुनिया को स्वावलंबी बनने की सीख देते हुए भी नजर आते हैं। ऐसी सीख, जो कभी महात्मा गांधी ने दी थी।

सात समंदर पार की यात्रा।
इन महिलाओं के द्वारा देसी तकनीक-तरीके से अपने कौशल से बुने धागों और उनसे बनी साड़ी सात समंदर पार की यात्रा कर गई है। इस साड़ी को पहनने वाली विदेशी मैम भी इन हुनरमंदों की तारीफ करते नहीं थकती। मजे की बात देखिए कि दुनियाभर की महिलाओं के लिए साड़ी बुन रही ये असमिया महिलाएं अपना तन पूरी तरह से नहीं ढंक पातीं। इन महिला बुनकरों के बनाए कपड़े आज अमेरिका, जर्मनी और दुबई में बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं। महिलाओं द्वारा संचालित आगोर का सबसे बड़ा शोरूम बेंगलूरु में खोला गया है। असम में भी कई छोटे-छोटे स्टोर संचालित किए जा रहे हैं। इन महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहे डॉ. सुनील कौल कहते हैं कि कच्चा माल बेंगलूरु से असम आता है और रंगाई तमिलनाडु में होती है। हालांकि अब असम में ही रंगाई शुरू करने की कोशिश की जा रही है।
कपड़ों पर ग्रामीण सभ्यता
इन महिलाओं के द्वारा बनाई जा रही साडिय़ों की डिजाइनों में ग्रामीण सभ्यता बेहद खूबसूरती से झांकती है। इनमें मोर, पत्तियां, कछुए की छाती, डाउराई और दिनखियां जैसी डिजाइनें सबसे जयादा पसंदीदा हैं। करीब तीन सौ से अधिक महिला बुनकरों के कपड़ों का यह कारोबार सालाना एक करोड़ तक पहुंच गया है। खास बात यह भी है कि करीब तीन मीटर का दुकना (साड़ी जैसा कपड़ा) पहनने वाली ये बुनकर अपने ठेठ और आदिवासी अंदाज को भूलती नहीं हैं। शायद यही कुछ ऐसा है, जो असमिया संघर्ष को आज भी एक आवाज दिए हुए है। ऐसी आवाज, जो कभी दिल्ली तक ठीक ढंग से नहीं पहुंची।
एक ही मंत्र 'सहकारिता'
असल में ये महिला बुनकर सहकारिता के मूलमंत्र को लेकर काम कर रही हैं। रौमई के पास स्थित बड़े कस्बे बोंगाईगांव के सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी ये महिलाएं अपने घरों पर ही कपड़ों का निर्माण करती हैं। एक खासियत यह भी है कि जिस महिला के यहां काम हो रहा है, उसकी मदद के लिए अन्य महिलाएं भी आ जाती हैं। इन महिलाओं ने वीवर कमेटी एवं आगोर ट्रस्ट भी बनाया हुआ है, जिसके आज करीब 180 सदस्य हैं। ये महिलाएं मिलकर वेलफेयर सोसाइटी भी चलाती हैं। सोसाइटी में रहने से लेकर खाने तक में सहभागिता देखी जा सकती है।देसी

तकनीक, सबका साथ
देसी तकनीक से बनी मशीनों पर धागा और साड़ी बुनने का काम पर ये महिलाएं सात-आठ हजार रुपए महीने तक कमा लेती हैं। अमूमन एक महिला का लक्ष्य तीस मीटर साड़ी या अन्य कपड़ा बुनने का होता है। यदि कोई महिला तीस मीटर की साड़ी निर्धारित समय में बना पाने में असमर्थ रहती है, तो समूह की अन्य महिलाएं उसे सहयोग करने में जुट जाती हैं। ये महिलाएं बुनाई की एवज में मिलने वाले मेहनताने में अपना हिस्सा नहीं मांगतीं, बल्कि मेहनताने पर पूरा हक जरूरतमंद महिला का ही रहता है।
चेहरे पर भावों की शून्यता
वीवर कमेटी एवं आगोर ट्रस्ट इन महिला बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस मशीन पर कपड़ा बुना जाता है, वह मशीन और कच्चा माल इन महिलाओं को संस्था उपलब्ध कराती है। असल में अभावों में जीने वाली इन महिलाओं को अपने बूते जीवन जीने की सीख दी जा रही है। साथ ही इनकी अस्मिता की रक्षा करते हुए स्वाभिमान बचाए रखने का बीड़ा भी आंट ने उठाया है। संस्था का संचालन सेना से सेवानिवृत्त डॉ. सुनील कौल कर रहे हैं। उनकी मेहनत इन महिलाओं को जीने की नई राह दिखा रही है। हालांकि इन महिलाओं में से कई के चेहरों पर कोई भाव नहीं होता। ऐसा लगता है कि जिंदगी की कशमकश में उन्होंने खुद को पहचानना और यहां तक कि सजना-संवरना भी छोड़ दिया है।
कोई एमबीबीएस नहीं टिकता
इन महिलाओं के समुचित विकास की दिशा में काम कर रहे डॉ. सुनील पर झोलाछाप डॉक्टरों व नीम-हकीमों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगते रहे हैं। इस बारे में उनका कहना है कि यहां पर कोई एमबीबीएस टिकना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को मरीजों की जांच करने तथा दवाई लिखने का तरीका सिखाता हूं। इससे इमरजेंसी में स्थिति को संभालने में मदद मिल जाती है। वे कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिहाज से बोडोलैंड क्षेत्रों में हालात भयानक हैं, जिन्हें संभालने के लिए सामूहिक प्रयासों की दरकार है।

खुद ही बनाया साइकिल बैंक
इन महिला बुनकरों को अपने रोजमर्रा के काम जैसे पानी लाना, सब्जी लाना आदि के लिए करीब दो किमी. पैदल जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय जाया होता था। इसके लिए संस्था ने महिलाओं को लोन पर साइकिल उपलब्ध कराना शुरू किया। इसके बाद इन महिलाओं ने आपसी समझ से अक्टूबर, 2013 में खुद का साइकिल बैंक बना लिया। बैंक की संचालक रीमा बताती है कि बैंक के तहत 11 ग्रुप बनाए गए। प्रत्येक ग्रुप में 12 सदस्य शामिल की गईं। प्रत्येक महिला ने 40 से 60 रुपए प्रतिमाह एकत्र करना शुरू किया। जिस महिला को बैंक से साइकिल लेनी होती है, उसे अमानत के रूप में 1100 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। साथ ही प्रतिमाह किश्त के रूप में 100 रुपए और ब्याज के रूप में 60 रुपए देने पड़ते हैं। अब तक 68 महिलाओं ने साइकिल खरीद ली हैं। साइकिल न केवल इनकी सुविधा बन गई है, बल्कि मनोरंजन का साधन भी है। माह में एक बार धीमी और तेज गति की साइकिल रेस आयोजित की जाती है। जीतने वाली पांच महिलाओं का आपस में जुटाई गई राशि से पुरस्कार भी दिए जाते हैं। इस दौरान असमिया चाय का भी लुत्फ उठाया जाता है।
हाल ही में लेखक का चयन असम के इन गांवों में रिसर्च के लिए हुआ था है।



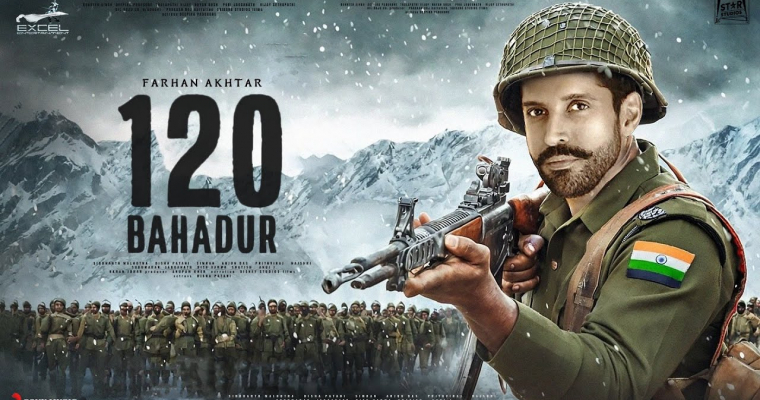




Comments