 संजीव पांडे
संजीव पांडे
2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान पेड न्यूज का मसला जोर-शोर से उठा था। इसी दौरान मीडिया के मालिकाना हक, मीडिया में एकाधिकारी प्रवृत्ति, मीडिया का मुनाफा आदि का मामला भी उठा। मीडिया में कॉरपोरेट निवेश, कॉरपोरेट हिस्सेदारी, मीडिया घरानों का मुनाफा, इनके सामाजिक दायित्व आदि को लेकर सवाल उठाए गए। चूंकि पश्चिम के देशों में ये सवाल बहुत पहले उठे थे, बहसें हुर्इं और वहां की सरकारें इस पर कानून बना चुकी हैं, इसलिए भारत में समय के साथ यह सवाल उठना स्वाभाविक था।
भारत में मीडिया का कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का हो चुका है। चूंकि अब सवाल सिर्फ पेड न्यूज तक सीमित नहीं है, इसलिए तीसरे प्रेस आयोग की मांग हो रही है। पेड न्यूज, मीडिया घरानों के अन्य कारोबार, पत्रकारों की स्थिति पर संसदीय समिति भी अध्ययन कर चुकी है। रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट मई, 2013 में दे दी थी। पर उस रिपोर्ट की सिफारिशों को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भी अगस्त, 2014 में मीडिया स्वामित्व, कारोबार और मुनाफे आदि को लेकर तीन अध्ययन रिपोर्टें और विस्तृत सिफारिश पेश की थी। लेकिन उस रिपोर्ट पर भी सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है।
तीसरे प्रेस आयोग के गठन को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रस्ताव भेजा गया था। तब उनके मीडिया सलाहकार हरीश खरे ने इस पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया था। मगर बाद में सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने तीसरे प्रेस आयोग के गठन के लिए खुद मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन दिया था। लेकिन तब भी उन्होंने आश्वासन देने के बाद चुप्पी साध ली थी।
मीडिया में विशुद्ध मुनाफा और व्यापार का खेल 1990 के आसपास खुलकर शुरू हुआ। इसका एक बुरा परिणाम पेड न्यूज के रूप में सामने आया। मीडिया घरानों ने व्यापारिक लाभ के चक्कर में सिर्फ पेड न्यूज का खेल नहीं किया, बल्कि प्रिंटिंग, टेक्सटाइल्स, तेल, होटल, रियल एस्टेट और बिजली उत्पादन में निवेश भी किया। कुछ मीडिया घराने फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ एयरलाइन के क्षेत्र में भी चले गए। आज मीडिया कंपनियों का होटल, सीमेंट, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, क्रिकेट, सूचना तकनीक और रियल एस्टेट में भारी निवेश है।
यही नहीं, मीडिया घरानों पर आर्थिक अपराधों के आरोप ने मीडिया की साख पर बट्टा लगाया है। मीडिया घरानों पर लगे आर्थिक अपराधों के आरोप के बाद मीडिया की सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, इनके आर्थिक मुनाफे को भी परिभाषित करने की मांग की जाने लगी है। इसे रोकने के लिए नए कानून बनाने की मांग उठ रही है।
तीसरा प्रेस आयोग क्यों चाहिए? इसके ठोस कारण हैं। आबादी के हिसाब से भी 1947 और अब की स्थितियों में काफी अंतर है। 1947 में भारत की आबादी साढ़े चौंतीस करोड़ थी, आज सवा करोड़ तक पहुंच गई है। 1947 में देश में अठारह प्रतिशत लोग साक्षर थे, आज साक्षरता की दर 75 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 1947 में देश में कुल दो सौ चौदह अखबार छपते थे। इसमें 44 अंगरेजी के अखबार थे, वर्तमान में 70 हजार अखबार छप रहे हैं। अब पाठक संख्या के प्रामाणिक आंकड़े हैं, जबकि 1947 में इसके आंकड़े तक उपलब्ध नहीं थे। इस समय पूरे देश में 34 करोड़ लोग अखबारों के पाठक हैं। 1947 में पूरे देश में छह रेडियो स्टेशन थे, आज छह सौ रेडियो स्टेशन हैं। दूरसंचार क्रांति ने मीडिया का रूप बदला और आज भारत में सैकड़ों टीवी चैनल चल रहे हैं। 1947 में देश में कोई टीवी चैनल नहीं था, आज करीब साढ़े आठ सौ टीवी चैनलों को लाइसेंस प्राप्त है। इन टीवी चैनलों की पहुंच सत्तर करोड़ लोगों तक है।
इस समय देश में जिन टीवी चैनलों को लाइसेंस प्राप्त है, उनमें से करीब साढ़े छह सौ चैनल चालू स्थिति में हैं। इनमें से करीब साढ़े तीन सौ टीवी चैनलों पर समाचार प्रसारित होते हैं। इन बदलती परिस्थितियों में मीडिया में एकाधिकारी प्रवृत्ति देश के हित में नहीं कही जा सकती। आज ऐसी कई कंपनियां हैं, जिनके पास टेलीविजन नेटवर्क है, उन्हीं के पास प्रिंट का मालिकाना हक भी है, उनके पास एफएम रेडियो भी है।
इसे रोकने के लिए कोई नियम नहीं है। इसमें किसका पैसा लगा है, उसकी पूरी जानकारी न तो जनता के पास है, न ही सरकार के। यह गोपनीयता इस हद तक है कि आपको यह नहीं पता चलता कि आप जो अखबार पढ़ रहे हैं या जो चैनल देख रहे हैं, उसमें कहीं अपराध जगत का पैसा तो नहीं लगा है? मीडिया का मुनाफा, उसका एकाधिकार, पेड न्यूज एक ज्वलंत विषय है। इनकी परिभाषा निर्धारित करना और इसके लिए नए कानून बनाना समय की मांग है। इसलिए तीसरे प्रेस आयोग का गठन जरूरी है।
जनसत्ता से साभार संजीव पांडे
2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान पेड न्यूज का मसला जोर-शोर से उठा था। इसी दौरान मीडिया के मालिकाना हक, मीडिया में एकाधिकारी प्रवृत्ति, मीडिया का मुनाफा आदि का मामला भी उठा। मीडिया में कॉरपोरेट निवेश, कॉरपोरेट हिस्सेदारी, मीडिया घरानों का मुनाफा, इनके सामाजिक दायित्व आदि को लेकर सवाल उठाए गए। चूंकि पश्चिम के देशों में ये सवाल बहुत पहले उठे थे, बहसें हुर्इं और वहां की सरकारें इस पर कानून बना चुकी हैं, इसलिए भारत में समय के साथ यह सवाल उठना स्वाभाविक था।
भारत में मीडिया का कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का हो चुका है। चूंकि अब सवाल सिर्फ पेड न्यूज तक सीमित नहीं है, इसलिए तीसरे प्रेस आयोग की मांग हो रही है। पेड न्यूज, मीडिया घरानों के अन्य कारोबार, पत्रकारों की स्थिति पर संसदीय समिति भी अध्ययन कर चुकी है। रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट मई, 2013 में दे दी थी। पर उस रिपोर्ट की सिफारिशों को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भी अगस्त, 2014 में मीडिया स्वामित्व, कारोबार और मुनाफे आदि को लेकर तीन अध्ययन रिपोर्टें और विस्तृत सिफारिश पेश की थी। लेकिन उस रिपोर्ट पर भी सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है।
तीसरे प्रेस आयोग के गठन को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रस्ताव भेजा गया था। तब उनके मीडिया सलाहकार हरीश खरे ने इस पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया था। मगर बाद में सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने तीसरे प्रेस आयोग के गठन के लिए खुद मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन दिया था। लेकिन तब भी उन्होंने आश्वासन देने के बाद चुप्पी साध ली थी।
मीडिया में विशुद्ध मुनाफा और व्यापार का खेल 1990 के आसपास खुलकर शुरू हुआ। इसका एक बुरा परिणाम पेड न्यूज के रूप में सामने आया। मीडिया घरानों ने व्यापारिक लाभ के चक्कर में सिर्फ पेड न्यूज का खेल नहीं किया, बल्कि प्रिंटिंग, टेक्सटाइल्स, तेल, होटल, रियल एस्टेट और बिजली उत्पादन में निवेश भी किया। कुछ मीडिया घराने फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ एयरलाइन के क्षेत्र में भी चले गए। आज मीडिया कंपनियों का होटल, सीमेंट, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, क्रिकेट, सूचना तकनीक और रियल एस्टेट में भारी निवेश है।
यही नहीं, मीडिया घरानों पर आर्थिक अपराधों के आरोप ने मीडिया की साख पर बट्टा लगाया है। मीडिया घरानों पर लगे आर्थिक अपराधों के आरोप के बाद मीडिया की सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, इनके आर्थिक मुनाफे को भी परिभाषित करने की मांग की जाने लगी है। इसे रोकने के लिए नए कानून बनाने की मांग उठ रही है।
तीसरा प्रेस आयोग क्यों चाहिए? इसके ठोस कारण हैं। आबादी के हिसाब से भी 1947 और अब की स्थितियों में काफी अंतर है। 1947 में भारत की आबादी साढ़े चौंतीस करोड़ थी, आज सवा करोड़ तक पहुंच गई है। 1947 में देश में अठारह प्रतिशत लोग साक्षर थे, आज साक्षरता की दर 75 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 1947 में देश में कुल दो सौ चौदह अखबार छपते थे। इसमें 44 अंगरेजी के अखबार थे, वर्तमान में 70 हजार अखबार छप रहे हैं। अब पाठक संख्या के प्रामाणिक आंकड़े हैं, जबकि 1947 में इसके आंकड़े तक उपलब्ध नहीं थे। इस समय पूरे देश में 34 करोड़ लोग अखबारों के पाठक हैं। 1947 में पूरे देश में छह रेडियो स्टेशन थे, आज छह सौ रेडियो स्टेशन हैं। दूरसंचार क्रांति ने मीडिया का रूप बदला और आज भारत में सैकड़ों टीवी चैनल चल रहे हैं। 1947 में देश में कोई टीवी चैनल नहीं था, आज करीब साढ़े आठ सौ टीवी चैनलों को लाइसेंस प्राप्त है। इन टीवी चैनलों की पहुंच सत्तर करोड़ लोगों तक है।
इस समय देश में जिन टीवी चैनलों को लाइसेंस प्राप्त है, उनमें से करीब साढ़े छह सौ चैनल चालू स्थिति में हैं। इनमें से करीब साढ़े तीन सौ टीवी चैनलों पर समाचार प्रसारित होते हैं। इन बदलती परिस्थितियों में मीडिया में एकाधिकारी प्रवृत्ति देश के हित में नहीं कही जा सकती। आज ऐसी कई कंपनियां हैं, जिनके पास टेलीविजन नेटवर्क है, उन्हीं के पास प्रिंट का मालिकाना हक भी है, उनके पास एफएम रेडियो भी है।
इसे रोकने के लिए कोई नियम नहीं है। इसमें किसका पैसा लगा है, उसकी पूरी जानकारी न तो जनता के पास है, न ही सरकार के। यह गोपनीयता इस हद तक है कि आपको यह नहीं पता चलता कि आप जो अखबार पढ़ रहे हैं या जो चैनल देख रहे हैं, उसमें कहीं अपराध जगत का पैसा तो नहीं लगा है? मीडिया का मुनाफा, उसका एकाधिकार, पेड न्यूज एक ज्वलंत विषय है। इनकी परिभाषा निर्धारित करना और इसके लिए नए कानून बनाना समय की मांग है। इसलिए तीसरे प्रेस आयोग का गठन जरूरी है।
जनसत्ता से साभार
संजीव पांडे
2009 के लोकसभा चुनावों के दौरान पेड न्यूज का मसला जोर-शोर से उठा था। इसी दौरान मीडिया के मालिकाना हक, मीडिया में एकाधिकारी प्रवृत्ति, मीडिया का मुनाफा आदि का मामला भी उठा। मीडिया में कॉरपोरेट निवेश, कॉरपोरेट हिस्सेदारी, मीडिया घरानों का मुनाफा, इनके सामाजिक दायित्व आदि को लेकर सवाल उठाए गए। चूंकि पश्चिम के देशों में ये सवाल बहुत पहले उठे थे, बहसें हुर्इं और वहां की सरकारें इस पर कानून बना चुकी हैं, इसलिए भारत में समय के साथ यह सवाल उठना स्वाभाविक था।
भारत में मीडिया का कारोबार कई हजार करोड़ रुपए का हो चुका है। चूंकि अब सवाल सिर्फ पेड न्यूज तक सीमित नहीं है, इसलिए तीसरे प्रेस आयोग की मांग हो रही है। पेड न्यूज, मीडिया घरानों के अन्य कारोबार, पत्रकारों की स्थिति पर संसदीय समिति भी अध्ययन कर चुकी है। रक्षा राज्यमंत्री राव इंद्रजीत के नेतृत्व वाली संसदीय समिति ने इस संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट मई, 2013 में दे दी थी। पर उस रिपोर्ट की सिफारिशों को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भी अगस्त, 2014 में मीडिया स्वामित्व, कारोबार और मुनाफे आदि को लेकर तीन अध्ययन रिपोर्टें और विस्तृत सिफारिश पेश की थी। लेकिन उस रिपोर्ट पर भी सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया है।
तीसरे प्रेस आयोग के गठन को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रस्ताव भेजा गया था। तब उनके मीडिया सलाहकार हरीश खरे ने इस पर ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया था। मगर बाद में सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने तीसरे प्रेस आयोग के गठन के लिए खुद मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन दिया था। लेकिन तब भी उन्होंने आश्वासन देने के बाद चुप्पी साध ली थी।
मीडिया में विशुद्ध मुनाफा और व्यापार का खेल 1990 के आसपास खुलकर शुरू हुआ। इसका एक बुरा परिणाम पेड न्यूज के रूप में सामने आया। मीडिया घरानों ने व्यापारिक लाभ के चक्कर में सिर्फ पेड न्यूज का खेल नहीं किया, बल्कि प्रिंटिंग, टेक्सटाइल्स, तेल, होटल, रियल एस्टेट और बिजली उत्पादन में निवेश भी किया। कुछ मीडिया घराने फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ एयरलाइन के क्षेत्र में भी चले गए। आज मीडिया कंपनियों का होटल, सीमेंट, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, क्रिकेट, सूचना तकनीक और रियल एस्टेट में भारी निवेश है।
यही नहीं, मीडिया घरानों पर आर्थिक अपराधों के आरोप ने मीडिया की साख पर बट्टा लगाया है। मीडिया घरानों पर लगे आर्थिक अपराधों के आरोप के बाद मीडिया की सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, इनके आर्थिक मुनाफे को भी परिभाषित करने की मांग की जाने लगी है। इसे रोकने के लिए नए कानून बनाने की मांग उठ रही है।
तीसरा प्रेस आयोग क्यों चाहिए? इसके ठोस कारण हैं। आबादी के हिसाब से भी 1947 और अब की स्थितियों में काफी अंतर है। 1947 में भारत की आबादी साढ़े चौंतीस करोड़ थी, आज सवा करोड़ तक पहुंच गई है। 1947 में देश में अठारह प्रतिशत लोग साक्षर थे, आज साक्षरता की दर 75 प्रतिशत तक पहुंच गई है। 1947 में देश में कुल दो सौ चौदह अखबार छपते थे। इसमें 44 अंगरेजी के अखबार थे, वर्तमान में 70 हजार अखबार छप रहे हैं। अब पाठक संख्या के प्रामाणिक आंकड़े हैं, जबकि 1947 में इसके आंकड़े तक उपलब्ध नहीं थे। इस समय पूरे देश में 34 करोड़ लोग अखबारों के पाठक हैं। 1947 में पूरे देश में छह रेडियो स्टेशन थे, आज छह सौ रेडियो स्टेशन हैं। दूरसंचार क्रांति ने मीडिया का रूप बदला और आज भारत में सैकड़ों टीवी चैनल चल रहे हैं। 1947 में देश में कोई टीवी चैनल नहीं था, आज करीब साढ़े आठ सौ टीवी चैनलों को लाइसेंस प्राप्त है। इन टीवी चैनलों की पहुंच सत्तर करोड़ लोगों तक है।
इस समय देश में जिन टीवी चैनलों को लाइसेंस प्राप्त है, उनमें से करीब साढ़े छह सौ चैनल चालू स्थिति में हैं। इनमें से करीब साढ़े तीन सौ टीवी चैनलों पर समाचार प्रसारित होते हैं। इन बदलती परिस्थितियों में मीडिया में एकाधिकारी प्रवृत्ति देश के हित में नहीं कही जा सकती। आज ऐसी कई कंपनियां हैं, जिनके पास टेलीविजन नेटवर्क है, उन्हीं के पास प्रिंट का मालिकाना हक भी है, उनके पास एफएम रेडियो भी है।
इसे रोकने के लिए कोई नियम नहीं है। इसमें किसका पैसा लगा है, उसकी पूरी जानकारी न तो जनता के पास है, न ही सरकार के। यह गोपनीयता इस हद तक है कि आपको यह नहीं पता चलता कि आप जो अखबार पढ़ रहे हैं या जो चैनल देख रहे हैं, उसमें कहीं अपराध जगत का पैसा तो नहीं लगा है? मीडिया का मुनाफा, उसका एकाधिकार, पेड न्यूज एक ज्वलंत विषय है। इनकी परिभाषा निर्धारित करना और इसके लिए नए कानून बनाना समय की मांग है। इसलिए तीसरे प्रेस आयोग का गठन जरूरी है।
जनसत्ता से साभार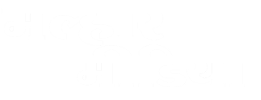
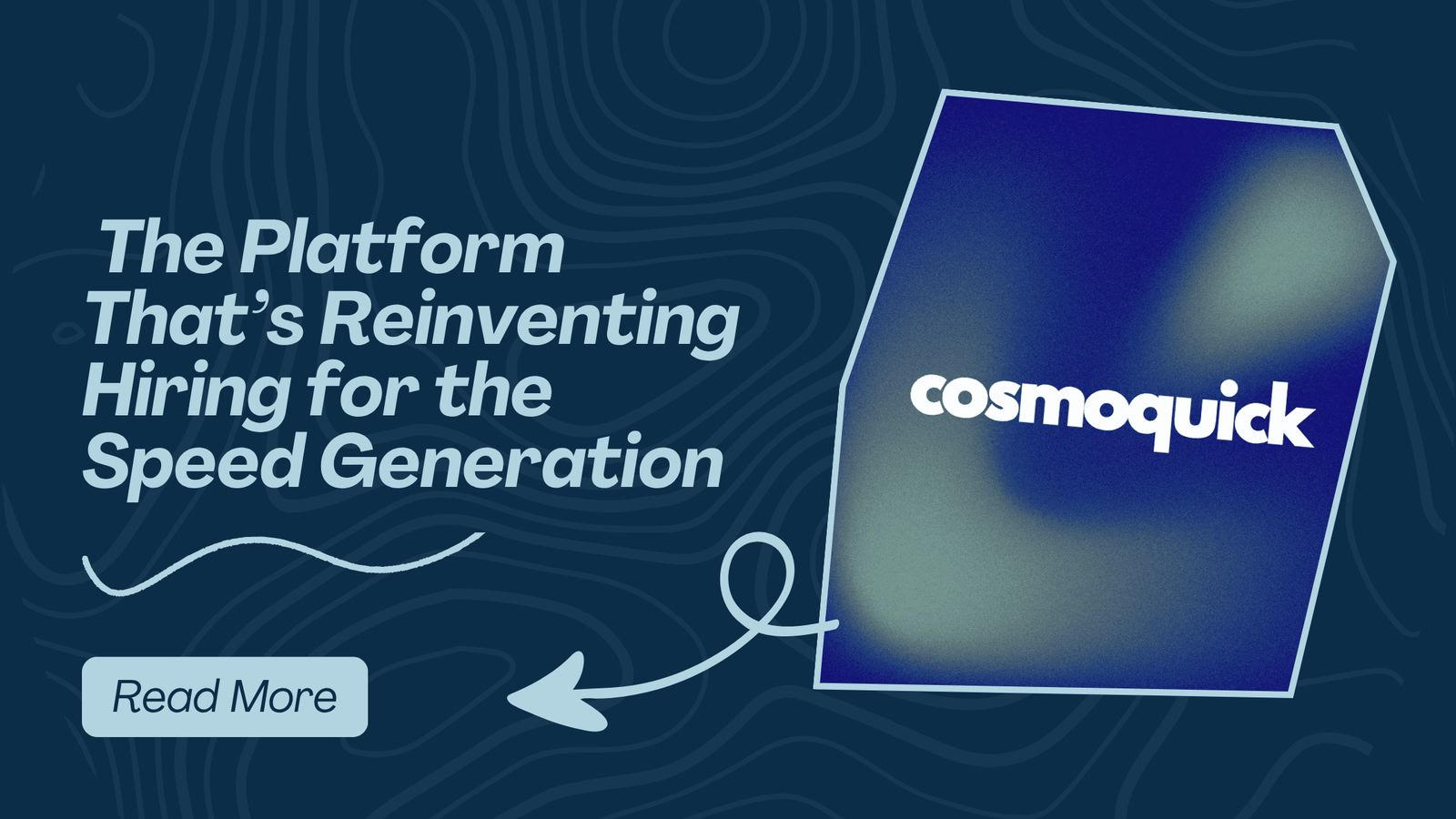





Comments