 मनोज कुमार
मनोज कुमार
उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के अनेक उपक्रम संचालित हो रहे हैं। केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों में यह अभियान चला हुआ है। करोड़ों रुपयों के विज्ञापन प्रकाशित किये और कराये जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की श्रेणी में उन्हें रखा जा रहा है जो टीवी, फ्रिज, कूलर से लेकर दवाएं खरीदते हैं। इस श्रेणी में संभवतः पत्र-पत्रिकाएं और केबल कनेक्शन लेने वालों को शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण शायद इनकी श्रेणी अलग है क्योंकि इन्हें उपभोक्ता न कहकर पाठक और दर्शक कहा जाता है अर्थात इनका संबंध बाजार से न होकर बौद्धिक दुनिया से है।
कानून की नजर में भले ही पाठक या दर्शक उपभोक्ता नहीं कहलाते हों किन्तु प्राथमिक रूप से यह उपभोक्ता की ही श्रेणी में आते हैं। पढ़ने के पहले की प्रक्रिया पत्र-पत्रिका खरीदना अथवा केबल कनेक्शन के लिये तयशुदा रकम चुकाना है, ऐसे में वे पहले उपभोक्ता होते हैं और बाद में पाठक या दर्शक। पाठक और दर्शकों के हिस्से में सेंधमारी लम्बे समय से की जा रही है, वह अन्यायपूर्ण है बल्कि ये पाठक और दर्शक तानाशाही के शिकार हो चले हैं। सीधे तौर पर पाठक और दर्शकों के हिस्से में सेंधमारी का मामला साफ नहीं होता है किन्तु मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि एक साल में पाठकों के हिस्से में लगभग पच्चीस फीसदी हक पर सेंधमारी की जाती है।
सभी अखबारों की कीमत तय है, वैसे ही जैसे साबुन की टिकिया की। वह कम या ज्यादा हो सकती है किन्तु यह प्रबंधन का फैसला है कि वह अखबार की कीमत क्या तय करे किन्तु जो कीमत तय की जाती है, वह पाठकों से वसूली जाती है। कीमत में कमी अथवा बढ़ोत्तरी भी की जाती है। यह सब ठीक है किन्तु जब तयशुदा कीमत आप वसूल रहे हैं तो आपकी जवाबदारी बन जाती है कि जितने पन्नों के अखबार का वायदा किया है, वह पाठकों को दिया जाए।

पन्ने ही नहीं बल्कि खबरों वाले पन्ने दिये जाएं किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है कि किसी समय अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों के लिये एक हिस्सा तय होता था। पहले अस्सी प्रतिशत खबरें और बीस प्रतिशत विज्ञापन और बाद में यह प्रतिशत बदल गया और साठ प्रतिशत खबरें और चालीस प्रतिशत विज्ञापन की जगह हो गई। शायद अभी भी यही फार्मूला काम कर रहा है किन्तु कागज में, वास्तविकता में नहीं। अखबार जब तब पाठकों के हिस्से में सेंधमारी कर देते हैं।
हर साल एबीसी अर्थात आडिट ब्यूरो सर्कुलेशन पड़ताल कर यह जानकारी देता है कि किन अखबारों की बिक्री में कितना इजाफा हुआ अथवा कितना ग्राफ उसका गिरा। एबीसी मशीन पर छपने वाले अखबार की प्रतियों गिनने के बाद अपना निर्णय सुनाता है। लिहाजा हर अखबारों की संख्या अलग अलग होती है तथा इसमें भी शहरवार अलग—अलग होते हैं। एबीसी के ये आंकड़ें प्रबंधन तक होते हैं, आंकड़ों को सार्वजनिक करने का काम उनका नहीं है किन्तु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये अखबार वाले तत्काल एक पूरा पेज कौन किससे आगे, कौन किससे पीछे और वे किस मायने में श्रेष्ठ हैं बताने के लिये छाप देते हैं। साल में एक बार पूरा का पूरा पेज जो खबरों के लिये होता है, पाठकों के हिस्से में सेंधमारी कर स्वयं की वाहवाही में निकाल दिया जाता है।
यह तो एक उदाहरण मात्र है। त्यौहारों के समय तो विज्ञापनों के बीच खबरों को तलाश करना पड़ता है। दीपावली के पांच दिनों के अखबारों का विश्लेशण करेंगे तो पाएंगे कि बीस प्रतिशत खबरें होती हैं और अस्सी प्रतिशत विज्ञापन किन्तु अखबार के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई बार का अनुभव यह रहा है कि विज्ञापनों के लिये बढ़ाये गये पन्ने की कीमत भी पाठकों से वसूल कर ली जाती है। इसे कहना चाहिए आम के आम और गुठलियों के दाम भी प्रबंधन ले लेता है। इसी तरह चुनाव के समय अखबारों में भी पाठकों के साथ अन्याय होता है तो राजनीतिक दलों में नियुक्तियां, आगमन, स्वागत आदि के पूरे पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित कर खबरों को कम कर दिया जाता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की अधिसूचना प्रकाशन के समय भी अतिरिक्त पष्ठ नहीं जोड़े जाते हैं। एक तरफ तो विज्ञापन प्रकाशित कर पाठकों के हिस्से में सेंधमारी की जाती है तो दूसरी तरफ रविवार के परिशिष्ट की कीमत सामान्य दिनों से अतिरिक्त वसूली जाती है।
पेड न्यूज का हल्ला मचाने वाले लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा, यह कहना गैरवाजिब है किन्तु पाठकों के हक में जो सेंधमारी हो रही है, उसके बारे में खामोश बने रहना ठीक नहीं है। पाठकों की हिस्सेदारी में सेंधमारी का एक और तरीका है पाठकों की राय के बिना नियमित स्तंभों को बदलना। इस बारे में कुछ लोगों से बात करने पर उनका यह कहना था कि यह प्रबंधन का सर्वाधिकार है कि वह अखबार को किस तरह निकालता है अथवा में उसमें संशोधन करता है जब कुछ लेखक और पाठकों से बात की गई तो उनका कहना था कि अखबार प्रकाशन में लाभ का मामला प्रबंधन का हो सकता है किन्तु अखबार तो पाठक की पसंद और उसकी जरूरत के अनुरूप निकलना चाहिए। इस बारे में उनका कहना था कि हिन्दी अखबारों में अंग्रेजी की अनुदित सामग्री प्रकाशित की जा रही है जिससे हिन्दी के मूल विचारों से पाठकों का वास्ता खत्म हो रहा है।
एक बड़े वर्ग की चिंता पाठकों के पत्र कॉलम को लेकर भी जाहिर हुई। इस वर्ग का कहना यह था कि पाठकों के पत्र के माध्यम से न केवल विचारों का आदान प्रदान होता था बल्कि वह समस्याएं जिनका हल मुद्दत से नहीं होता था, उसके निदान में भी मदद मिलती थी। अब पाठकों के पत्र औपचारिक रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस वर्ग की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि इससे पाठकों की हिस्सेदारी खत्म हो रही है जो अखबारों की गंभीरता के लिये खतरनाक है।
पाठकों के हिस्से पर सेंधमारी के सवाल पर महिला पाठकों से चर्चा करने पर यह बात भी सामने आयी कि जो अखबार प्राथमिक शाला की भूमिका में थे, उनका लोप हो गया है बल्कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये ईनाम बांटे जा रहे हैं। अखबारों से हम बाजार से सौदा कैसे करें सीखते थे किन्तु अखबारों की यह सामाजिक जवाबदारी भी कम होती जा रही है। बाजार में ठगने से कैसे बचें, लालच में खरीददारी नहीं करें जैसे नैतिक बातें सिखाने वाले अखबार स्वयं लालच देकर अखबार बेचने की कोशिश में जुटे हुए हैं।

लगभग सभी पाठकों को इस बात की निराशा थी कि हर अखबार अपने आपको सर्वाधिक लोकप्रिय बताने पर जुटा है किन्तु सबका दावा पाठक संख्या पर है न कि बिक्री पर। अखबारों का स्लोगन होता है कि उनकी पाठक संख्या कितनी है। इस बारे में मीडिया पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से हुई बातचीत में उनका कहना था कि अपने को श्रेष्ठ बताने का यह शॉर्टकट रास्ता है। मैंनेजमेंट की टर्मानोलॉजी के मुताबिक एक परिवार पांच सदस्यों का माना जाता है और एक अखबार के पांच पाठक होते हैं। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर अखबारों का पठन पाठन करने वालों की संख्या को अखबार चौगुनी करके देखता है और इस हिसाब से वह तुलना कर अपनी प्रसार संख्या के स्थान पर पाठकों की संख्या बता देता था।
पाठकों के हिस्सेदारी में सेंधमारी के संदर्भ में अध्ययन के दौरान मुझे याद आया कि अपनी पत्रकारिता के आरंभिक दिनों में हम लोगों को सिखाया जाता था कि अखबार के पाठक नहीं बल्कि पाठकों की आंखों की संख्या से अखबार की रीडरशिप गिनी जाए अर्थात एक व्यक्ति की दो आंखें और पाठक पाठक यानि दस आंखें। हालांकि यह बातें हमें अखबार की सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी के मद्देनजर बताया जाता था कि हमारी एक गलती से किसी भी व्यक्ति की मानहानि किस स्तर पर और कैसे हो सकती है जिसकी भरपाई करना अखबार के लिये नामुमकिन होगा।
तथ्यों की पड़ताल और संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुन लेने के बाद खबर लिखना चाहिए। हालांकि तीस वर्श पुरानी पत्रकारिता की नैतिक बातें आज भी उतनी मूल्यवान हैं किन्तु व्यवहार से परे हो चली हैं। फिलवक्त चिंता इस बात की है कि पाठकों की हिस्सेदारी पर जो सेंधमारी हो रही है, उसे कैसे रोका जाए। यह चिंता मामूली नहीं है क्योंकि साबुन की टिकिया एक समय के बाद अपना अस्तित्व खो देती है किन्तु एक अखबार इतिहास बन जाता है और इतिहास में पाठकों के हिस्से की सेंधमारी हिस्सा न बन पाये, इसकी चिंता पाठक को, पत्रकार को और प्रबंधन को करना होगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं भोपाल से प्रकाशित शोध पत्रिका "समागम" के संपादक है मनोज कुमार
उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के अनेक उपक्रम संचालित हो रहे हैं। केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों में यह अभियान चला हुआ है। करोड़ों रुपयों के विज्ञापन प्रकाशित किये और कराये जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की श्रेणी में उन्हें रखा जा रहा है जो टीवी, फ्रिज, कूलर से लेकर दवाएं खरीदते हैं। इस श्रेणी में संभवतः पत्र-पत्रिकाएं और केबल कनेक्शन लेने वालों को शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण शायद इनकी श्रेणी अलग है क्योंकि इन्हें उपभोक्ता न कहकर पाठक और दर्शक कहा जाता है अर्थात इनका संबंध बाजार से न होकर बौद्धिक दुनिया से है।
कानून की नजर में भले ही पाठक या दर्शक उपभोक्ता नहीं कहलाते हों किन्तु प्राथमिक रूप से यह उपभोक्ता की ही श्रेणी में आते हैं। पढ़ने के पहले की प्रक्रिया पत्र-पत्रिका खरीदना अथवा केबल कनेक्शन के लिये तयशुदा रकम चुकाना है, ऐसे में वे पहले उपभोक्ता होते हैं और बाद में पाठक या दर्शक। पाठक और दर्शकों के हिस्से में सेंधमारी लम्बे समय से की जा रही है, वह अन्यायपूर्ण है बल्कि ये पाठक और दर्शक तानाशाही के शिकार हो चले हैं। सीधे तौर पर पाठक और दर्शकों के हिस्से में सेंधमारी का मामला साफ नहीं होता है किन्तु मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि एक साल में पाठकों के हिस्से में लगभग पच्चीस फीसदी हक पर सेंधमारी की जाती है।
सभी अखबारों की कीमत तय है, वैसे ही जैसे साबुन की टिकिया की। वह कम या ज्यादा हो सकती है किन्तु यह प्रबंधन का फैसला है कि वह अखबार की कीमत क्या तय करे किन्तु जो कीमत तय की जाती है, वह पाठकों से वसूली जाती है। कीमत में कमी अथवा बढ़ोत्तरी भी की जाती है। यह सब ठीक है किन्तु जब तयशुदा कीमत आप वसूल रहे हैं तो आपकी जवाबदारी बन जाती है कि जितने पन्नों के अखबार का वायदा किया है, वह पाठकों को दिया जाए।
मनोज कुमार
उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के अनेक उपक्रम संचालित हो रहे हैं। केन्द्र से लेकर राज्य सरकारों में यह अभियान चला हुआ है। करोड़ों रुपयों के विज्ञापन प्रकाशित किये और कराये जा रहे हैं। उपभोक्ताओं की श्रेणी में उन्हें रखा जा रहा है जो टीवी, फ्रिज, कूलर से लेकर दवाएं खरीदते हैं। इस श्रेणी में संभवतः पत्र-पत्रिकाएं और केबल कनेक्शन लेने वालों को शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण शायद इनकी श्रेणी अलग है क्योंकि इन्हें उपभोक्ता न कहकर पाठक और दर्शक कहा जाता है अर्थात इनका संबंध बाजार से न होकर बौद्धिक दुनिया से है।
कानून की नजर में भले ही पाठक या दर्शक उपभोक्ता नहीं कहलाते हों किन्तु प्राथमिक रूप से यह उपभोक्ता की ही श्रेणी में आते हैं। पढ़ने के पहले की प्रक्रिया पत्र-पत्रिका खरीदना अथवा केबल कनेक्शन के लिये तयशुदा रकम चुकाना है, ऐसे में वे पहले उपभोक्ता होते हैं और बाद में पाठक या दर्शक। पाठक और दर्शकों के हिस्से में सेंधमारी लम्बे समय से की जा रही है, वह अन्यायपूर्ण है बल्कि ये पाठक और दर्शक तानाशाही के शिकार हो चले हैं। सीधे तौर पर पाठक और दर्शकों के हिस्से में सेंधमारी का मामला साफ नहीं होता है किन्तु मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि एक साल में पाठकों के हिस्से में लगभग पच्चीस फीसदी हक पर सेंधमारी की जाती है।
सभी अखबारों की कीमत तय है, वैसे ही जैसे साबुन की टिकिया की। वह कम या ज्यादा हो सकती है किन्तु यह प्रबंधन का फैसला है कि वह अखबार की कीमत क्या तय करे किन्तु जो कीमत तय की जाती है, वह पाठकों से वसूली जाती है। कीमत में कमी अथवा बढ़ोत्तरी भी की जाती है। यह सब ठीक है किन्तु जब तयशुदा कीमत आप वसूल रहे हैं तो आपकी जवाबदारी बन जाती है कि जितने पन्नों के अखबार का वायदा किया है, वह पाठकों को दिया जाए।
 पन्ने ही नहीं बल्कि खबरों वाले पन्ने दिये जाएं किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है कि किसी समय अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों के लिये एक हिस्सा तय होता था। पहले अस्सी प्रतिशत खबरें और बीस प्रतिशत विज्ञापन और बाद में यह प्रतिशत बदल गया और साठ प्रतिशत खबरें और चालीस प्रतिशत विज्ञापन की जगह हो गई। शायद अभी भी यही फार्मूला काम कर रहा है किन्तु कागज में, वास्तविकता में नहीं। अखबार जब तब पाठकों के हिस्से में सेंधमारी कर देते हैं।
हर साल एबीसी अर्थात आडिट ब्यूरो सर्कुलेशन पड़ताल कर यह जानकारी देता है कि किन अखबारों की बिक्री में कितना इजाफा हुआ अथवा कितना ग्राफ उसका गिरा। एबीसी मशीन पर छपने वाले अखबार की प्रतियों गिनने के बाद अपना निर्णय सुनाता है। लिहाजा हर अखबारों की संख्या अलग अलग होती है तथा इसमें भी शहरवार अलग—अलग होते हैं। एबीसी के ये आंकड़ें प्रबंधन तक होते हैं, आंकड़ों को सार्वजनिक करने का काम उनका नहीं है किन्तु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये अखबार वाले तत्काल एक पूरा पेज कौन किससे आगे, कौन किससे पीछे और वे किस मायने में श्रेष्ठ हैं बताने के लिये छाप देते हैं। साल में एक बार पूरा का पूरा पेज जो खबरों के लिये होता है, पाठकों के हिस्से में सेंधमारी कर स्वयं की वाहवाही में निकाल दिया जाता है।
यह तो एक उदाहरण मात्र है। त्यौहारों के समय तो विज्ञापनों के बीच खबरों को तलाश करना पड़ता है। दीपावली के पांच दिनों के अखबारों का विश्लेशण करेंगे तो पाएंगे कि बीस प्रतिशत खबरें होती हैं और अस्सी प्रतिशत विज्ञापन किन्तु अखबार के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई बार का अनुभव यह रहा है कि विज्ञापनों के लिये बढ़ाये गये पन्ने की कीमत भी पाठकों से वसूल कर ली जाती है। इसे कहना चाहिए आम के आम और गुठलियों के दाम भी प्रबंधन ले लेता है। इसी तरह चुनाव के समय अखबारों में भी पाठकों के साथ अन्याय होता है तो राजनीतिक दलों में नियुक्तियां, आगमन, स्वागत आदि के पूरे पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित कर खबरों को कम कर दिया जाता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की अधिसूचना प्रकाशन के समय भी अतिरिक्त पष्ठ नहीं जोड़े जाते हैं। एक तरफ तो विज्ञापन प्रकाशित कर पाठकों के हिस्से में सेंधमारी की जाती है तो दूसरी तरफ रविवार के परिशिष्ट की कीमत सामान्य दिनों से अतिरिक्त वसूली जाती है।
पेड न्यूज का हल्ला मचाने वाले लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा, यह कहना गैरवाजिब है किन्तु पाठकों के हक में जो सेंधमारी हो रही है, उसके बारे में खामोश बने रहना ठीक नहीं है। पाठकों की हिस्सेदारी में सेंधमारी का एक और तरीका है पाठकों की राय के बिना नियमित स्तंभों को बदलना। इस बारे में कुछ लोगों से बात करने पर उनका यह कहना था कि यह प्रबंधन का सर्वाधिकार है कि वह अखबार को किस तरह निकालता है अथवा में उसमें संशोधन करता है जब कुछ लेखक और पाठकों से बात की गई तो उनका कहना था कि अखबार प्रकाशन में लाभ का मामला प्रबंधन का हो सकता है किन्तु अखबार तो पाठक की पसंद और उसकी जरूरत के अनुरूप निकलना चाहिए। इस बारे में उनका कहना था कि हिन्दी अखबारों में अंग्रेजी की अनुदित सामग्री प्रकाशित की जा रही है जिससे हिन्दी के मूल विचारों से पाठकों का वास्ता खत्म हो रहा है।
एक बड़े वर्ग की चिंता पाठकों के पत्र कॉलम को लेकर भी जाहिर हुई। इस वर्ग का कहना यह था कि पाठकों के पत्र के माध्यम से न केवल विचारों का आदान प्रदान होता था बल्कि वह समस्याएं जिनका हल मुद्दत से नहीं होता था, उसके निदान में भी मदद मिलती थी। अब पाठकों के पत्र औपचारिक रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस वर्ग की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि इससे पाठकों की हिस्सेदारी खत्म हो रही है जो अखबारों की गंभीरता के लिये खतरनाक है।
पाठकों के हिस्से पर सेंधमारी के सवाल पर महिला पाठकों से चर्चा करने पर यह बात भी सामने आयी कि जो अखबार प्राथमिक शाला की भूमिका में थे, उनका लोप हो गया है बल्कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये ईनाम बांटे जा रहे हैं। अखबारों से हम बाजार से सौदा कैसे करें सीखते थे किन्तु अखबारों की यह सामाजिक जवाबदारी भी कम होती जा रही है। बाजार में ठगने से कैसे बचें, लालच में खरीददारी नहीं करें जैसे नैतिक बातें सिखाने वाले अखबार स्वयं लालच देकर अखबार बेचने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
पन्ने ही नहीं बल्कि खबरों वाले पन्ने दिये जाएं किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं हो रहा है। हमें पढ़ाया गया है, बताया गया है कि किसी समय अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों के लिये एक हिस्सा तय होता था। पहले अस्सी प्रतिशत खबरें और बीस प्रतिशत विज्ञापन और बाद में यह प्रतिशत बदल गया और साठ प्रतिशत खबरें और चालीस प्रतिशत विज्ञापन की जगह हो गई। शायद अभी भी यही फार्मूला काम कर रहा है किन्तु कागज में, वास्तविकता में नहीं। अखबार जब तब पाठकों के हिस्से में सेंधमारी कर देते हैं।
हर साल एबीसी अर्थात आडिट ब्यूरो सर्कुलेशन पड़ताल कर यह जानकारी देता है कि किन अखबारों की बिक्री में कितना इजाफा हुआ अथवा कितना ग्राफ उसका गिरा। एबीसी मशीन पर छपने वाले अखबार की प्रतियों गिनने के बाद अपना निर्णय सुनाता है। लिहाजा हर अखबारों की संख्या अलग अलग होती है तथा इसमें भी शहरवार अलग—अलग होते हैं। एबीसी के ये आंकड़ें प्रबंधन तक होते हैं, आंकड़ों को सार्वजनिक करने का काम उनका नहीं है किन्तु अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिये अखबार वाले तत्काल एक पूरा पेज कौन किससे आगे, कौन किससे पीछे और वे किस मायने में श्रेष्ठ हैं बताने के लिये छाप देते हैं। साल में एक बार पूरा का पूरा पेज जो खबरों के लिये होता है, पाठकों के हिस्से में सेंधमारी कर स्वयं की वाहवाही में निकाल दिया जाता है।
यह तो एक उदाहरण मात्र है। त्यौहारों के समय तो विज्ञापनों के बीच खबरों को तलाश करना पड़ता है। दीपावली के पांच दिनों के अखबारों का विश्लेशण करेंगे तो पाएंगे कि बीस प्रतिशत खबरें होती हैं और अस्सी प्रतिशत विज्ञापन किन्तु अखबार के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कई बार का अनुभव यह रहा है कि विज्ञापनों के लिये बढ़ाये गये पन्ने की कीमत भी पाठकों से वसूल कर ली जाती है। इसे कहना चाहिए आम के आम और गुठलियों के दाम भी प्रबंधन ले लेता है। इसी तरह चुनाव के समय अखबारों में भी पाठकों के साथ अन्याय होता है तो राजनीतिक दलों में नियुक्तियां, आगमन, स्वागत आदि के पूरे पूरे पन्ने का विज्ञापन प्रकाशित कर खबरों को कम कर दिया जाता है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की अधिसूचना प्रकाशन के समय भी अतिरिक्त पष्ठ नहीं जोड़े जाते हैं। एक तरफ तो विज्ञापन प्रकाशित कर पाठकों के हिस्से में सेंधमारी की जाती है तो दूसरी तरफ रविवार के परिशिष्ट की कीमत सामान्य दिनों से अतिरिक्त वसूली जाती है।
पेड न्यूज का हल्ला मचाने वाले लोगों को इस बात का इल्म नहीं होगा, यह कहना गैरवाजिब है किन्तु पाठकों के हक में जो सेंधमारी हो रही है, उसके बारे में खामोश बने रहना ठीक नहीं है। पाठकों की हिस्सेदारी में सेंधमारी का एक और तरीका है पाठकों की राय के बिना नियमित स्तंभों को बदलना। इस बारे में कुछ लोगों से बात करने पर उनका यह कहना था कि यह प्रबंधन का सर्वाधिकार है कि वह अखबार को किस तरह निकालता है अथवा में उसमें संशोधन करता है जब कुछ लेखक और पाठकों से बात की गई तो उनका कहना था कि अखबार प्रकाशन में लाभ का मामला प्रबंधन का हो सकता है किन्तु अखबार तो पाठक की पसंद और उसकी जरूरत के अनुरूप निकलना चाहिए। इस बारे में उनका कहना था कि हिन्दी अखबारों में अंग्रेजी की अनुदित सामग्री प्रकाशित की जा रही है जिससे हिन्दी के मूल विचारों से पाठकों का वास्ता खत्म हो रहा है।
एक बड़े वर्ग की चिंता पाठकों के पत्र कॉलम को लेकर भी जाहिर हुई। इस वर्ग का कहना यह था कि पाठकों के पत्र के माध्यम से न केवल विचारों का आदान प्रदान होता था बल्कि वह समस्याएं जिनका हल मुद्दत से नहीं होता था, उसके निदान में भी मदद मिलती थी। अब पाठकों के पत्र औपचारिक रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस वर्ग की चिंता इस बात को लेकर भी थी कि इससे पाठकों की हिस्सेदारी खत्म हो रही है जो अखबारों की गंभीरता के लिये खतरनाक है।
पाठकों के हिस्से पर सेंधमारी के सवाल पर महिला पाठकों से चर्चा करने पर यह बात भी सामने आयी कि जो अखबार प्राथमिक शाला की भूमिका में थे, उनका लोप हो गया है बल्कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिये ईनाम बांटे जा रहे हैं। अखबारों से हम बाजार से सौदा कैसे करें सीखते थे किन्तु अखबारों की यह सामाजिक जवाबदारी भी कम होती जा रही है। बाजार में ठगने से कैसे बचें, लालच में खरीददारी नहीं करें जैसे नैतिक बातें सिखाने वाले अखबार स्वयं लालच देकर अखबार बेचने की कोशिश में जुटे हुए हैं।
 लगभग सभी पाठकों को इस बात की निराशा थी कि हर अखबार अपने आपको सर्वाधिक लोकप्रिय बताने पर जुटा है किन्तु सबका दावा पाठक संख्या पर है न कि बिक्री पर। अखबारों का स्लोगन होता है कि उनकी पाठक संख्या कितनी है। इस बारे में मीडिया पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से हुई बातचीत में उनका कहना था कि अपने को श्रेष्ठ बताने का यह शॉर्टकट रास्ता है। मैंनेजमेंट की टर्मानोलॉजी के मुताबिक एक परिवार पांच सदस्यों का माना जाता है और एक अखबार के पांच पाठक होते हैं। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर अखबारों का पठन पाठन करने वालों की संख्या को अखबार चौगुनी करके देखता है और इस हिसाब से वह तुलना कर अपनी प्रसार संख्या के स्थान पर पाठकों की संख्या बता देता था।
पाठकों के हिस्सेदारी में सेंधमारी के संदर्भ में अध्ययन के दौरान मुझे याद आया कि अपनी पत्रकारिता के आरंभिक दिनों में हम लोगों को सिखाया जाता था कि अखबार के पाठक नहीं बल्कि पाठकों की आंखों की संख्या से अखबार की रीडरशिप गिनी जाए अर्थात एक व्यक्ति की दो आंखें और पाठक पाठक यानि दस आंखें। हालांकि यह बातें हमें अखबार की सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी के मद्देनजर बताया जाता था कि हमारी एक गलती से किसी भी व्यक्ति की मानहानि किस स्तर पर और कैसे हो सकती है जिसकी भरपाई करना अखबार के लिये नामुमकिन होगा।
तथ्यों की पड़ताल और संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुन लेने के बाद खबर लिखना चाहिए। हालांकि तीस वर्श पुरानी पत्रकारिता की नैतिक बातें आज भी उतनी मूल्यवान हैं किन्तु व्यवहार से परे हो चली हैं। फिलवक्त चिंता इस बात की है कि पाठकों की हिस्सेदारी पर जो सेंधमारी हो रही है, उसे कैसे रोका जाए। यह चिंता मामूली नहीं है क्योंकि साबुन की टिकिया एक समय के बाद अपना अस्तित्व खो देती है किन्तु एक अखबार इतिहास बन जाता है और इतिहास में पाठकों के हिस्से की सेंधमारी हिस्सा न बन पाये, इसकी चिंता पाठक को, पत्रकार को और प्रबंधन को करना होगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं भोपाल से प्रकाशित शोध पत्रिका "समागम" के संपादक है
लगभग सभी पाठकों को इस बात की निराशा थी कि हर अखबार अपने आपको सर्वाधिक लोकप्रिय बताने पर जुटा है किन्तु सबका दावा पाठक संख्या पर है न कि बिक्री पर। अखबारों का स्लोगन होता है कि उनकी पाठक संख्या कितनी है। इस बारे में मीडिया पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से हुई बातचीत में उनका कहना था कि अपने को श्रेष्ठ बताने का यह शॉर्टकट रास्ता है। मैंनेजमेंट की टर्मानोलॉजी के मुताबिक एक परिवार पांच सदस्यों का माना जाता है और एक अखबार के पांच पाठक होते हैं। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर अखबारों का पठन पाठन करने वालों की संख्या को अखबार चौगुनी करके देखता है और इस हिसाब से वह तुलना कर अपनी प्रसार संख्या के स्थान पर पाठकों की संख्या बता देता था।
पाठकों के हिस्सेदारी में सेंधमारी के संदर्भ में अध्ययन के दौरान मुझे याद आया कि अपनी पत्रकारिता के आरंभिक दिनों में हम लोगों को सिखाया जाता था कि अखबार के पाठक नहीं बल्कि पाठकों की आंखों की संख्या से अखबार की रीडरशिप गिनी जाए अर्थात एक व्यक्ति की दो आंखें और पाठक पाठक यानि दस आंखें। हालांकि यह बातें हमें अखबार की सामाजिक एवं नैतिक जिम्मेदारी के मद्देनजर बताया जाता था कि हमारी एक गलती से किसी भी व्यक्ति की मानहानि किस स्तर पर और कैसे हो सकती है जिसकी भरपाई करना अखबार के लिये नामुमकिन होगा।
तथ्यों की पड़ताल और संबंधित व्यक्ति का पक्ष सुन लेने के बाद खबर लिखना चाहिए। हालांकि तीस वर्श पुरानी पत्रकारिता की नैतिक बातें आज भी उतनी मूल्यवान हैं किन्तु व्यवहार से परे हो चली हैं। फिलवक्त चिंता इस बात की है कि पाठकों की हिस्सेदारी पर जो सेंधमारी हो रही है, उसे कैसे रोका जाए। यह चिंता मामूली नहीं है क्योंकि साबुन की टिकिया एक समय के बाद अपना अस्तित्व खो देती है किन्तु एक अखबार इतिहास बन जाता है और इतिहास में पाठकों के हिस्से की सेंधमारी हिस्सा न बन पाये, इसकी चिंता पाठक को, पत्रकार को और प्रबंधन को करना होगी।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं भोपाल से प्रकाशित शोध पत्रिका "समागम" के संपादक है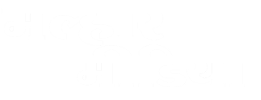
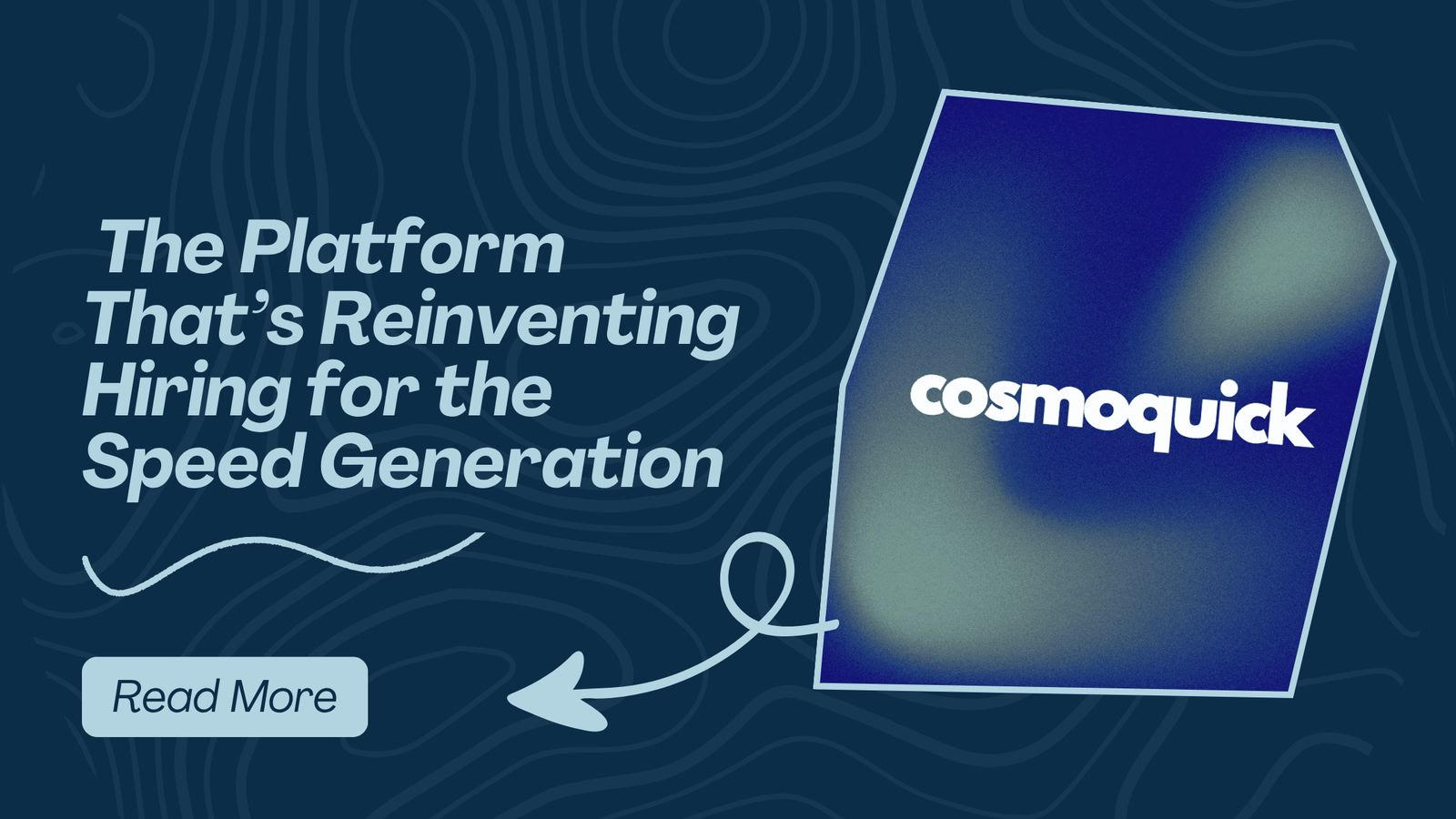





Comments