 पुण्य प्रसून वाजपेयी
पुण्य प्रसून वाजपेयी
अमेरिका में रूपर्ट मर्डोक प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो मर्डोक ने मोदी को आजादी के बाद से भारत का सबसे शानदार पीएम करार दे दिया। मर्डोक अब अमेरिकी राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। ओबामा पर अश्वेत प्रेजिडेंट न मानने के मर्डोक के बयान पर बवाल मचा ही हुआ है। अमेरिका में अपने न्यूज चैनल को चलाने के लिए मर्डोक आस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़ अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं, तो क्या मीडिया टाइकून इस भूमिका में आ चुके हैं कि वह सीधे सरकार और सियासत को प्रभावित कर सकें या कहें राजनीतिक तौर पर सक्रिय ना होते हुए भी राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए काम कर सके।
अगर ऐसा हो चला है तो यकीन मानिए अब भारत में भी सत्ता-मीडिया का नैक्सेस पेड न्यूज से कहीं आगे निकल चुका है। जहां अब सत्ता के लिए खबरों को नए सिरे से बुनने का है या कहे सत्तानुकुल हालात बने रहें, इसके लिए दर्शकों के सामने ऐसे हालात बनाने का है जिसे देखते वक्त दर्शक महसूस करें कि अगर सत्ता के विरोध की खबर है तो खबर दिखाने वाला देश के साथ गद्दारी कर रहा है।
यानी पहली बार मीडिया या पत्रकारिता की इस धारणा को ही मीडिया हाउस जड़-मूल से खत्म करने की राह पर निकल पड़े हैं कि पत्रकारिता का मतलब यह कतई नहीं है कि चुनी हुई सरकार के कामकाज पर निगरानी रखी जाए। यानी सत्ता को जनता ने पांच साल के लिए चुना है तो पांच बरस के दौर में सत्ता जो करे जैसा करे वह देश हित में ही होगा। जाहिर है यह बेहद महीन लकीर है, जहां मीडिया का सत्ता के साथ गठजोड़ मीडिया को भी राजनीतिक तौर खड़ा कर दें और सत्ता भी मीडिया को अपना कैडर मान कर बर्ताव करें।
यह घालमेल व्यवसायिक तौर पर भी लाभदायक साबित हो जाता है। यानी सत्ता के साथ खड़े होने की पत्रकारिता इसका एहसास होने ही नहीं देती है कि सत्ता कोई लाभ मीडिया हाउस को दे रही है या मीडिया सत्ता की राजनीति का प्यादा बनकर पत्रकारिता कर रही है। इसके कई उदाहरणों को पहले समझें। बिहार चुनाव में किसी भी अखबार या न्यूज चैनल की हेडलाइन नीतीश कुमार को पहले अहमियत देती है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का नंबर आएगा और फिर लालू प्रसाद यादव का।
यानी कोई भी खबर जिसमें नीतीश कह रहे होंगे या नीतीश को निशाने पर लिया जा रहा होगा वह खबर नंबर एक हो जाएगी। इसी तर्ज पर मोदी जो कह रहे होंगे या मोदी निशाने पर होंगे उसका नंबर दो होगा। कोई भी कह सकता है कि जब टक्कर इन्हीं दो नेताओं के बीच है, तो खबर भी इन्हीं दो नेताओं को लेकर होगी।
तो सवाल है कि जब सुशील मोदी कहते हैं कि सत्ता में आए तो गो-वध पर पांबदी होगी। तो उस खबर को ना तो कोई पत्रकार परखेगा और ना ही अखबार में उसे प्रमुखता के साथ जगह मिलेगी। लेकिन जब नीतीश इसके जबाब में कहेंगे कि बिहार में तो साठ बरस से गो-वध पर पाबंदी है तो पत्रकार के लिए वह बड़ी खबर होगी। इसी तर्ज पर केन्द्र का कोई भी मंत्री बिहार चुनाव के वक्त आकर कोई भी बड़े से बड़ा नीतिगत फैसले की जानकारी चुनावी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें, उसको अखबार में जगह नहीं मिलेगी। ना ही प्रधानमंत्री मोदी के किसी बड़े फैसले की जानकारी देने को अखबार या न्यूज चैनल दिखाएंगे। यानी पीएम मोदी के बयान में जब तक नीतीश–लालू को निशाने पर लेने का मुलम्मा ना चढ़ा हो, वह खबर बन ही नहीं सकती।
यानी खबरों का आधार नेता या कहें सियासी चेहरों को उस दौर में बना दिया गया जब सबसे ज्यादा जरूरत ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उसके बाद चेहरों की प्राथमिकता सत्ता के साथ गठजोड़ के जरिए कुछ इस तरह से पाठकों में या कहें दर्शकों में बनाते हुए उभर कर आयी, जिससे ग्राउंड रिपोर्टिंग या आम जनता से जुड़े सरकारी फैसलों को परखने की जरुरत ही ना पड़े। उसकी एवज में सरकार के किसी भी फैसले को सकारात्मक तौर पर तमाम आयामों के साथ इस तरह रखा जाये जिससे पत्रकारिता सूचना संसार में खो जाये।
मसलन, झारखंड विश्व बैंक की फेरहिस्त में नंबर 29 से खिसक कर नंबर तीन पर आ गया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी बांका की अपनी चुनावी रैली में यह कहते हुए देते है कि नीतीश बिहार को 27वें नंबर से आगे ना बढ़ा पाए, तो खबरों के लिहाज से नीतीश पर हमले या उनकी नाकामी या झारखंड में बीजेपी की सत्ता आने के बाद उसके उपलब्धि से आगे कोई पत्रकारिता जाएगी ही नहीं। यानी झारखंड में कैसे सिर्फ खनन का लाइसेंस नए तरीके से सत्ता के करीबियो को बांटा गया और खनन प्रक्रिया का लाभ झरखंड की जनता को कम उघोगपतियों को ज्यादा हो रहा है। इसपर कोई रिपोर्टिंग नहीं और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट झारखंड के लोगों की बदहाली या इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में सबकुछ कैसे ठप पड़ा है या फिर रोजगार के साधन और ज्यादा सिमट गये हैं, इस पर केन्द्रित होता ही नहीं है।
तो नई मुश्किल यह नहीं है कि कोई पत्रकार इन आधारों को टटोलने क्यों नहीं निकलता। मुश्किल यह है कि जो प्रधानमंत्री कह दें या बिहार में जो नीतीश कह दें उसके आगे कोई लकीर इस दौर में पत्रकारिता खिंचती नहीं है या पत्रकारिता के नए तौर तरीके ऐसे बना दिए गए हैं जिससे सत्ता के दिए बयान या दावों को ही आखिरी सच करार दे दिया जाए।
अब यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसे हालात पेड मीडिया के आगे कैसे हैं और इस नए हालात के मायने हैं क्या? असल में मीडिया के सरोकार जनता से हटते हुए कैसे सत्ता से ज्यादा बनते चले गए और सत्ता किस तरह मीडिया पर निर्भर होते हुए मीडिया के तौर तरीकों को ही बदलने में सफल हो गया। समझना यह भी जरुरी है। मौजूदा वक्त में मीडिया हाउस में कॉरपोरेट की रुची क्या सिर्फ इसलिए है कि मीडिया से मुनाफा बनाया कमाया जा सकता है? या फिर मीडिया को दूसरे धंधो के लिए ढाल बनाया जा सकता है, तो पहला सच तो यही है कि मीडिया कभी अपने आप में बहुत लाभ कमाने का धंधा रहा ही नहीं है। यानी मीडिया के जरिए सत्ता से सौदेबाजी करते हुए दूसरे धंधों से लाभ कमाने के हालात देखे जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात जिस तेजी से बदले हैं या कहें बदल रहे हैं उसमें मीडिया की मौजूदगी अपनी आप में सत्ता होना हो चला है और उसकी सबसे बड़ी वजह है, बाजार का विस्तार। उपभोक्ताओं की बढ़ती तादाद और देश को देखने समझने का नजरिया। तमाम टेक्नॉलाजी या कहें सूचना क्रांति के बाद कहीं ज्यादा तेजी से शहर और गांव में संवाद खत्म हुआ है।
भारत जैसे देश में आदिवासियों का एक बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या से कोई संवाद देश की मुख्यधारा का है ही नहीं है। इतना ही नहीं दुनिया में आवाजाही का विस्तार जरूर हुआ लेकिन संवाद बनाना कहीं ज्यादा तेजी से सिकुड़ा है, क्योंकि सुविधाओं को जुगाड़ना, या जीने की वस्तुओं को पाने के तरीके या फिर जिंदगी जीने के लिए जो मागदौल बाजारनुकुल है उसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी या मीडिया की ही हो चली है। यानी कल तो हर वस्तु के साथ जो संबंध मनुष्य का बना हुआ था वह घटते-घटते मानव संसाधन को हाशिए पर ले आया है। यानी कोई संवाद किसी से बनाए बगैर सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए आपके घर तक पहुंच सकती है। चाहे सब्जी फल हो या टीवी-फ्रिज या फिर किताब खरीदना हो या कंप्यूटर। रेलवे और हवाई जहाज के टिकट के लिए भी अब उफभोक्ताओं को किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की कोई जरुरत है ही नहीं। सारे काम, सारी सुविधा की वस्तु, या जीने की जरूरत के सामान मोबाइल–कंप्यूटर के जरिए अगर आपके घर तक पहुंच सकते हैं तो उपभोक्ता समाज के लिए मीडिया की जरूरत सामाजिक संकट, मानवीय मूल्यों से रूबरू होना या देश के हालात हैं क्या या किसी भी घटना विशेष को लेकर जानकारी तलब करना क्यों जरुरी होगा?
खासकर भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश में जहां उपभोक्ताओं की तादाद किसी भी यूरोप के देश से ज्यादा हो और दो जून के लिए संघर्ष करते लोगों की तादाद भी इतनी ज्यादा हो कि यूरोप के कई देश उसमें समा जाए, तो पहला सवाल यही है कि समाज की असमानता और ज्यादा बढ़ सके। इसके लिए मीडिया काम करेगा या दूरियां पाटने की दिशा में रिपोर्ट दिखाएगा। जाहिर है मीडिया भी पूंजी से विकसित होता माध्यम ही जब बना दिया गया है और असमानता की सबसे बड़ी वजह पूंजी कमाने के असमान तरीके ही सत्ता की नीतियों के जरिए विस्तार पा रहे हो तो रास्ता जाएगा किधर। लेकिन यह तर्क सतही है। असल सच यह है कि धीरे-धीरे मीडिया को भी उत्पाद में तब्दील किया गया। फिर मीडिया को भी एहसास कराया गया कि उत्पाद के लिए उपभोक्ता चाहिए। फिर उपभोक्ता को मीडिया के जरिए ही यह सियासी समझ दी गई कि विकास की जो रेखा राज्य सत्ता खींचे वही आखरी सच है।
ध्यान दें तो 1991 के बाद आर्थिक सुधार के तीन स्तर देश ने देखें। नरसिंह राव के दौर में सरकारी मीडिया के सामानांतर सरकारी मंच पर निजी मीडिया हाउस को जगह मिली। उसके बाद वाजपेयी के दौर में निजीकरण का विस्तार हुआ। यानी सरकारी कोटा या सब्सिडी भी खत्म हुई। सरकारी उपक्रम तक की उपयोगिता पर सवालिया निशान लगे।
मनमोहन सिंह के दौर में बाजार को पूंजी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। यानी पूंजी ही बाजार का मानक बन गई और मोदी के दौर में पहली बार उस भारत को मुख्यधारा में लाने के लिए पूंजी और बाजार की खोज शुरू हुई जिस भारत को सरकारी पैकेज तले बीते ढाई दशक से हाशिए पर रखा गया था। पहली बार खुले तौर पर यह मान लिया गया कि 80 करोड़ भारतीयों को तभी कुछ दिया जा सकता है जब बाकी तीस करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एक सुंदर और विकसित भारत बनाया जा सके। लेकिन इस सोच में यह कोई समझ नहीं पाया कि जब पूंजी ही विकास का रास्ता तय करेगी तो सत्ता कोई भी हो वह पूंजी पर ही निर्भर होगी और वह पूंजी कही से भी आए और सत्ता के पूंजी पर निर्भर होने का मतलब है वह तमाम आधार भी उसी पूंजी के मातहत खुद को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत पाएंगें जो चुनी हुई सत्ता के हाथ में नहीं बल्कि पूंजी के जरिए बाजार से मुनाफा बनाने के लिए देश की सीमा नहीं बल्कि सीमाहीन बाजार का खुलापन तलाशेंगे।
ध्यान दें तो मीडिया हाउसों की साख खबरों से इतर टर्न ओवर पर टिकी है। सेल्स या मार्केटिंग टीम न्यूज रूम पर भारी पड़ने लगी, तो संपादक भी मैनेजर से होते हुए पूंजी बनाने और जुगाड़ कराने से आगे निकलते हुए सत्ता से वसूली करते हुए खुद में ही सत्ता बनने के दरवाजे पर टिका। प्रोपराइटर का संपादक हो जाना। समाचार पत्र या न्यूज चैनल के लिए पूंजी का जुगाड़ करने वाले का संपादक हो जाना। यह सब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चलता रहा। लेकिन जिस तर्ज पर 2014 के लोकसभा चुनाव ने सत्ता के बहुआयामी व्यापार को खुल कर सामने रख दिया उसमें खबरों की दुनिया से जुड़ें पत्रकारों और मालिकों को सामने पहली बार यह विकल्प उभरा कि वह सरकार की नीतियों को उसके जरिए बनाये जाने वाली व्यवस्था के साथ कैसे हो सकते हैं और राज्य के हालात खुद ब खुद उसे मदद दे देगा या फिर उसे खत्म कर देगा। यानी साथ खड़े हैं तो ठीक नहीं तो दुश्मन।
यह हालात इसलिए पेड न्यूज से आगे आकर खड़े हो गए क्योंकि चाहे अनचाहे अब राज्य को अपने मीडिया बजट का बंदर बांट अपने साथ खड़े मीडिया हाउस में बांटने के नहीं थे। बल्कि सत्ता की अकूत ताकत ने खबरों को परोसने के सलीके में भी सत्ता की खुशबू बिखेरनी शुरू कर दी। सामाजिक तौर पर सत्ता मीडिया के साथ कैसे खड़ी होगी यह मीडिया के सत्ता के लिए काम करने के मिजाज पर आ टिका। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं पत्रकारों के साथ डिनर करेंगे जो उनकी चापलूसी में माहिर होगा और पटना में नीतीश कुमार उन्हीं पत्रकारों को आगे बढ़ाने में सहयोग देगें जो उनके गुणगाण करने से हिचकेगा नहीं। इसलिए कोई पत्रकार दिल्ली में मोदी हो गया तो कोई पत्रकार पटना में नीतीश कुमार और जो-जो पत्रकार सत्ता से खुले तौर पर जुड़ा नजर आया उसे लगा कि वह खुद में सत्ता है। यानी सबसे ताकतवर है।
असल में बिहार चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो चला है कि पहली बार नायकों की खोज से चुनाव जा जुड़ा है। यानी 1989 में लालू यादव मंडल के नायक बनें तो 2010 में नीतीश सुशासन के नायक बनें और 2014 के चुनाव में नरेन्द्र मोदी देश के विकास नायक बन कर उभरे। ध्यान दें तो इसके अलावा सिर्फ दिल्ली के चुनाव ने केजरीवाल के तौर पर नायक की छवि गढ़ी। लेकिन केजरीवाल का नायककत्व पारंपरिक राजनीतिक को बदलने के लिए था ना कि नायक बन कर उसमें ढलने के लिए।
लेकिन 2015 के आखिर में बिहार चुनाव की जीत हार में तय यही होना है कि विदेशी पूंजी और खुले बाजार व्यवस्था के जरिए भारत को बदलने वाला नायक चाहिये या फिर जातिय गठबंधन के आसरे सामाजिक न्याय की सोच को आगे बढ़ाने वाला नायक चाहिये। जाहिर है बिहार जिस रास्ते पर जाएगा उसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की नायक छवि है और दूसरी तरफ चकाचौंध नायकत्व को चुनौती देने वाले नीतीश– लालू हैं। यानी यही हालात यूपी में भी टकराएंगें। अगर बिहार लालू नीतीश का रास्ता चुनता है तो यकीन मानिए मुलायम-मायावती भी दुश्मनी छोड़ गद्दी के लिए साथ आ खड़े होंगे ही। यानी 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड एक याद भर रह जाएगा और इससे पहले जो थ्योरी गठबंधन के फॉर्मूले में फेल होती रही वह फॉर्मूला चल पड़ेगा। यानी दो बराबर की पार्टियों में गठबंधन।
जाहिर है राजनीतिक बदलाव का असर मीडिया पर भी पड़ेगा। क्योंकि सत्ता के साथ वैचारिक तौर पर खड़े होकर पूंजी या मुनाफा बनाने से आगे खुद को सत्ता मानने की सोच को मान्यता मिले या सत्ता के सामाजिक सरोकार का ताना-बाना बुनते हुए कॉरपोरेट या पूंजी की सत्ता को ही चुनौती देनी वाली पत्रकारिता रहे। फैसला इसका भी होना है, लेकिन दोनों हालात छोटे घेरे में मीडिया को वैसे ही बड़ा कर रहे है जैसे अमेरिका में मर्डोक सत्ता को प्रभावित करने की स्थिति में है वैसे ही भारत में सत्ता के लिए मीडिया सबसे असरकारक हथियार बन चुका है। फर्क इतना ही है कि वहां पूंजी तय कर रही है और भारत में सत्ता की ताकत।
ब्लॉग से साभार पुण्य प्रसून वाजपेयी
अमेरिका में रूपर्ट मर्डोक प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो मर्डोक ने मोदी को आजादी के बाद से भारत का सबसे शानदार पीएम करार दे दिया। मर्डोक अब अमेरिकी राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। ओबामा पर अश्वेत प्रेजिडेंट न मानने के मर्डोक के बयान पर बवाल मचा ही हुआ है। अमेरिका में अपने न्यूज चैनल को चलाने के लिए मर्डोक आस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़ अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं, तो क्या मीडिया टाइकून इस भूमिका में आ चुके हैं कि वह सीधे सरकार और सियासत को प्रभावित कर सकें या कहें राजनीतिक तौर पर सक्रिय ना होते हुए भी राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए काम कर सके।
अगर ऐसा हो चला है तो यकीन मानिए अब भारत में भी सत्ता-मीडिया का नैक्सेस पेड न्यूज से कहीं आगे निकल चुका है। जहां अब सत्ता के लिए खबरों को नए सिरे से बुनने का है या कहे सत्तानुकुल हालात बने रहें, इसके लिए दर्शकों के सामने ऐसे हालात बनाने का है जिसे देखते वक्त दर्शक महसूस करें कि अगर सत्ता के विरोध की खबर है तो खबर दिखाने वाला देश के साथ गद्दारी कर रहा है।
यानी पहली बार मीडिया या पत्रकारिता की इस धारणा को ही मीडिया हाउस जड़-मूल से खत्म करने की राह पर निकल पड़े हैं कि पत्रकारिता का मतलब यह कतई नहीं है कि चुनी हुई सरकार के कामकाज पर निगरानी रखी जाए। यानी सत्ता को जनता ने पांच साल के लिए चुना है तो पांच बरस के दौर में सत्ता जो करे जैसा करे वह देश हित में ही होगा। जाहिर है यह बेहद महीन लकीर है, जहां मीडिया का सत्ता के साथ गठजोड़ मीडिया को भी राजनीतिक तौर खड़ा कर दें और सत्ता भी मीडिया को अपना कैडर मान कर बर्ताव करें।
यह घालमेल व्यवसायिक तौर पर भी लाभदायक साबित हो जाता है। यानी सत्ता के साथ खड़े होने की पत्रकारिता इसका एहसास होने ही नहीं देती है कि सत्ता कोई लाभ मीडिया हाउस को दे रही है या मीडिया सत्ता की राजनीति का प्यादा बनकर पत्रकारिता कर रही है। इसके कई उदाहरणों को पहले समझें। बिहार चुनाव में किसी भी अखबार या न्यूज चैनल की हेडलाइन नीतीश कुमार को पहले अहमियत देती है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का नंबर आएगा और फिर लालू प्रसाद यादव का।
यानी कोई भी खबर जिसमें नीतीश कह रहे होंगे या नीतीश को निशाने पर लिया जा रहा होगा वह खबर नंबर एक हो जाएगी। इसी तर्ज पर मोदी जो कह रहे होंगे या मोदी निशाने पर होंगे उसका नंबर दो होगा। कोई भी कह सकता है कि जब टक्कर इन्हीं दो नेताओं के बीच है, तो खबर भी इन्हीं दो नेताओं को लेकर होगी।
तो सवाल है कि जब सुशील मोदी कहते हैं कि सत्ता में आए तो गो-वध पर पांबदी होगी। तो उस खबर को ना तो कोई पत्रकार परखेगा और ना ही अखबार में उसे प्रमुखता के साथ जगह मिलेगी। लेकिन जब नीतीश इसके जबाब में कहेंगे कि बिहार में तो साठ बरस से गो-वध पर पाबंदी है तो पत्रकार के लिए वह बड़ी खबर होगी। इसी तर्ज पर केन्द्र का कोई भी मंत्री बिहार चुनाव के वक्त आकर कोई भी बड़े से बड़ा नीतिगत फैसले की जानकारी चुनावी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें, उसको अखबार में जगह नहीं मिलेगी। ना ही प्रधानमंत्री मोदी के किसी बड़े फैसले की जानकारी देने को अखबार या न्यूज चैनल दिखाएंगे। यानी पीएम मोदी के बयान में जब तक नीतीश–लालू को निशाने पर लेने का मुलम्मा ना चढ़ा हो, वह खबर बन ही नहीं सकती।
यानी खबरों का आधार नेता या कहें सियासी चेहरों को उस दौर में बना दिया गया जब सबसे ज्यादा जरूरत ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उसके बाद चेहरों की प्राथमिकता सत्ता के साथ गठजोड़ के जरिए कुछ इस तरह से पाठकों में या कहें दर्शकों में बनाते हुए उभर कर आयी, जिससे ग्राउंड रिपोर्टिंग या आम जनता से जुड़े सरकारी फैसलों को परखने की जरुरत ही ना पड़े। उसकी एवज में सरकार के किसी भी फैसले को सकारात्मक तौर पर तमाम आयामों के साथ इस तरह रखा जाये जिससे पत्रकारिता सूचना संसार में खो जाये।
मसलन, झारखंड विश्व बैंक की फेरहिस्त में नंबर 29 से खिसक कर नंबर तीन पर आ गया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी बांका की अपनी चुनावी रैली में यह कहते हुए देते है कि नीतीश बिहार को 27वें नंबर से आगे ना बढ़ा पाए, तो खबरों के लिहाज से नीतीश पर हमले या उनकी नाकामी या झारखंड में बीजेपी की सत्ता आने के बाद उसके उपलब्धि से आगे कोई पत्रकारिता जाएगी ही नहीं। यानी झारखंड में कैसे सिर्फ खनन का लाइसेंस नए तरीके से सत्ता के करीबियो को बांटा गया और खनन प्रक्रिया का लाभ झरखंड की जनता को कम उघोगपतियों को ज्यादा हो रहा है। इसपर कोई रिपोर्टिंग नहीं और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट झारखंड के लोगों की बदहाली या इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में सबकुछ कैसे ठप पड़ा है या फिर रोजगार के साधन और ज्यादा सिमट गये हैं, इस पर केन्द्रित होता ही नहीं है।
तो नई मुश्किल यह नहीं है कि कोई पत्रकार इन आधारों को टटोलने क्यों नहीं निकलता। मुश्किल यह है कि जो प्रधानमंत्री कह दें या बिहार में जो नीतीश कह दें उसके आगे कोई लकीर इस दौर में पत्रकारिता खिंचती नहीं है या पत्रकारिता के नए तौर तरीके ऐसे बना दिए गए हैं जिससे सत्ता के दिए बयान या दावों को ही आखिरी सच करार दे दिया जाए।
अब यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसे हालात पेड मीडिया के आगे कैसे हैं और इस नए हालात के मायने हैं क्या? असल में मीडिया के सरोकार जनता से हटते हुए कैसे सत्ता से ज्यादा बनते चले गए और सत्ता किस तरह मीडिया पर निर्भर होते हुए मीडिया के तौर तरीकों को ही बदलने में सफल हो गया। समझना यह भी जरुरी है। मौजूदा वक्त में मीडिया हाउस में कॉरपोरेट की रुची क्या सिर्फ इसलिए है कि मीडिया से मुनाफा बनाया कमाया जा सकता है? या फिर मीडिया को दूसरे धंधो के लिए ढाल बनाया जा सकता है, तो पहला सच तो यही है कि मीडिया कभी अपने आप में बहुत लाभ कमाने का धंधा रहा ही नहीं है। यानी मीडिया के जरिए सत्ता से सौदेबाजी करते हुए दूसरे धंधों से लाभ कमाने के हालात देखे जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात जिस तेजी से बदले हैं या कहें बदल रहे हैं उसमें मीडिया की मौजूदगी अपनी आप में सत्ता होना हो चला है और उसकी सबसे बड़ी वजह है, बाजार का विस्तार। उपभोक्ताओं की बढ़ती तादाद और देश को देखने समझने का नजरिया। तमाम टेक्नॉलाजी या कहें सूचना क्रांति के बाद कहीं ज्यादा तेजी से शहर और गांव में संवाद खत्म हुआ है।
भारत जैसे देश में आदिवासियों का एक बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या से कोई संवाद देश की मुख्यधारा का है ही नहीं है। इतना ही नहीं दुनिया में आवाजाही का विस्तार जरूर हुआ लेकिन संवाद बनाना कहीं ज्यादा तेजी से सिकुड़ा है, क्योंकि सुविधाओं को जुगाड़ना, या जीने की वस्तुओं को पाने के तरीके या फिर जिंदगी जीने के लिए जो मागदौल बाजारनुकुल है उसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी या मीडिया की ही हो चली है। यानी कल तो हर वस्तु के साथ जो संबंध मनुष्य का बना हुआ था वह घटते-घटते मानव संसाधन को हाशिए पर ले आया है। यानी कोई संवाद किसी से बनाए बगैर सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए आपके घर तक पहुंच सकती है। चाहे सब्जी फल हो या टीवी-फ्रिज या फिर किताब खरीदना हो या कंप्यूटर। रेलवे और हवाई जहाज के टिकट के लिए भी अब उफभोक्ताओं को किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की कोई जरुरत है ही नहीं। सारे काम, सारी सुविधा की वस्तु, या जीने की जरूरत के सामान मोबाइल–कंप्यूटर के जरिए अगर आपके घर तक पहुंच सकते हैं तो उपभोक्ता समाज के लिए मीडिया की जरूरत सामाजिक संकट, मानवीय मूल्यों से रूबरू होना या देश के हालात हैं क्या या किसी भी घटना विशेष को लेकर जानकारी तलब करना क्यों जरुरी होगा?
खासकर भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश में जहां उपभोक्ताओं की तादाद किसी भी यूरोप के देश से ज्यादा हो और दो जून के लिए संघर्ष करते लोगों की तादाद भी इतनी ज्यादा हो कि यूरोप के कई देश उसमें समा जाए, तो पहला सवाल यही है कि समाज की असमानता और ज्यादा बढ़ सके। इसके लिए मीडिया काम करेगा या दूरियां पाटने की दिशा में रिपोर्ट दिखाएगा। जाहिर है मीडिया भी पूंजी से विकसित होता माध्यम ही जब बना दिया गया है और असमानता की सबसे बड़ी वजह पूंजी कमाने के असमान तरीके ही सत्ता की नीतियों के जरिए विस्तार पा रहे हो तो रास्ता जाएगा किधर। लेकिन यह तर्क सतही है। असल सच यह है कि धीरे-धीरे मीडिया को भी उत्पाद में तब्दील किया गया। फिर मीडिया को भी एहसास कराया गया कि उत्पाद के लिए उपभोक्ता चाहिए। फिर उपभोक्ता को मीडिया के जरिए ही यह सियासी समझ दी गई कि विकास की जो रेखा राज्य सत्ता खींचे वही आखरी सच है।
ध्यान दें तो 1991 के बाद आर्थिक सुधार के तीन स्तर देश ने देखें। नरसिंह राव के दौर में सरकारी मीडिया के सामानांतर सरकारी मंच पर निजी मीडिया हाउस को जगह मिली। उसके बाद वाजपेयी के दौर में निजीकरण का विस्तार हुआ। यानी सरकारी कोटा या सब्सिडी भी खत्म हुई। सरकारी उपक्रम तक की उपयोगिता पर सवालिया निशान लगे।
मनमोहन सिंह के दौर में बाजार को पूंजी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। यानी पूंजी ही बाजार का मानक बन गई और मोदी के दौर में पहली बार उस भारत को मुख्यधारा में लाने के लिए पूंजी और बाजार की खोज शुरू हुई जिस भारत को सरकारी पैकेज तले बीते ढाई दशक से हाशिए पर रखा गया था। पहली बार खुले तौर पर यह मान लिया गया कि 80 करोड़ भारतीयों को तभी कुछ दिया जा सकता है जब बाकी तीस करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एक सुंदर और विकसित भारत बनाया जा सके। लेकिन इस सोच में यह कोई समझ नहीं पाया कि जब पूंजी ही विकास का रास्ता तय करेगी तो सत्ता कोई भी हो वह पूंजी पर ही निर्भर होगी और वह पूंजी कही से भी आए और सत्ता के पूंजी पर निर्भर होने का मतलब है वह तमाम आधार भी उसी पूंजी के मातहत खुद को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत पाएंगें जो चुनी हुई सत्ता के हाथ में नहीं बल्कि पूंजी के जरिए बाजार से मुनाफा बनाने के लिए देश की सीमा नहीं बल्कि सीमाहीन बाजार का खुलापन तलाशेंगे।
ध्यान दें तो मीडिया हाउसों की साख खबरों से इतर टर्न ओवर पर टिकी है। सेल्स या मार्केटिंग टीम न्यूज रूम पर भारी पड़ने लगी, तो संपादक भी मैनेजर से होते हुए पूंजी बनाने और जुगाड़ कराने से आगे निकलते हुए सत्ता से वसूली करते हुए खुद में ही सत्ता बनने के दरवाजे पर टिका। प्रोपराइटर का संपादक हो जाना। समाचार पत्र या न्यूज चैनल के लिए पूंजी का जुगाड़ करने वाले का संपादक हो जाना। यह सब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चलता रहा। लेकिन जिस तर्ज पर 2014 के लोकसभा चुनाव ने सत्ता के बहुआयामी व्यापार को खुल कर सामने रख दिया उसमें खबरों की दुनिया से जुड़ें पत्रकारों और मालिकों को सामने पहली बार यह विकल्प उभरा कि वह सरकार की नीतियों को उसके जरिए बनाये जाने वाली व्यवस्था के साथ कैसे हो सकते हैं और राज्य के हालात खुद ब खुद उसे मदद दे देगा या फिर उसे खत्म कर देगा। यानी साथ खड़े हैं तो ठीक नहीं तो दुश्मन।
यह हालात इसलिए पेड न्यूज से आगे आकर खड़े हो गए क्योंकि चाहे अनचाहे अब राज्य को अपने मीडिया बजट का बंदर बांट अपने साथ खड़े मीडिया हाउस में बांटने के नहीं थे। बल्कि सत्ता की अकूत ताकत ने खबरों को परोसने के सलीके में भी सत्ता की खुशबू बिखेरनी शुरू कर दी। सामाजिक तौर पर सत्ता मीडिया के साथ कैसे खड़ी होगी यह मीडिया के सत्ता के लिए काम करने के मिजाज पर आ टिका। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं पत्रकारों के साथ डिनर करेंगे जो उनकी चापलूसी में माहिर होगा और पटना में नीतीश कुमार उन्हीं पत्रकारों को आगे बढ़ाने में सहयोग देगें जो उनके गुणगाण करने से हिचकेगा नहीं। इसलिए कोई पत्रकार दिल्ली में मोदी हो गया तो कोई पत्रकार पटना में नीतीश कुमार और जो-जो पत्रकार सत्ता से खुले तौर पर जुड़ा नजर आया उसे लगा कि वह खुद में सत्ता है। यानी सबसे ताकतवर है।
असल में बिहार चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो चला है कि पहली बार नायकों की खोज से चुनाव जा जुड़ा है। यानी 1989 में लालू यादव मंडल के नायक बनें तो 2010 में नीतीश सुशासन के नायक बनें और 2014 के चुनाव में नरेन्द्र मोदी देश के विकास नायक बन कर उभरे। ध्यान दें तो इसके अलावा सिर्फ दिल्ली के चुनाव ने केजरीवाल के तौर पर नायक की छवि गढ़ी। लेकिन केजरीवाल का नायककत्व पारंपरिक राजनीतिक को बदलने के लिए था ना कि नायक बन कर उसमें ढलने के लिए।
लेकिन 2015 के आखिर में बिहार चुनाव की जीत हार में तय यही होना है कि विदेशी पूंजी और खुले बाजार व्यवस्था के जरिए भारत को बदलने वाला नायक चाहिये या फिर जातिय गठबंधन के आसरे सामाजिक न्याय की सोच को आगे बढ़ाने वाला नायक चाहिये। जाहिर है बिहार जिस रास्ते पर जाएगा उसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की नायक छवि है और दूसरी तरफ चकाचौंध नायकत्व को चुनौती देने वाले नीतीश– लालू हैं। यानी यही हालात यूपी में भी टकराएंगें। अगर बिहार लालू नीतीश का रास्ता चुनता है तो यकीन मानिए मुलायम-मायावती भी दुश्मनी छोड़ गद्दी के लिए साथ आ खड़े होंगे ही। यानी 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड एक याद भर रह जाएगा और इससे पहले जो थ्योरी गठबंधन के फॉर्मूले में फेल होती रही वह फॉर्मूला चल पड़ेगा। यानी दो बराबर की पार्टियों में गठबंधन।
जाहिर है राजनीतिक बदलाव का असर मीडिया पर भी पड़ेगा। क्योंकि सत्ता के साथ वैचारिक तौर पर खड़े होकर पूंजी या मुनाफा बनाने से आगे खुद को सत्ता मानने की सोच को मान्यता मिले या सत्ता के सामाजिक सरोकार का ताना-बाना बुनते हुए कॉरपोरेट या पूंजी की सत्ता को ही चुनौती देनी वाली पत्रकारिता रहे। फैसला इसका भी होना है, लेकिन दोनों हालात छोटे घेरे में मीडिया को वैसे ही बड़ा कर रहे है जैसे अमेरिका में मर्डोक सत्ता को प्रभावित करने की स्थिति में है वैसे ही भारत में सत्ता के लिए मीडिया सबसे असरकारक हथियार बन चुका है। फर्क इतना ही है कि वहां पूंजी तय कर रही है और भारत में सत्ता की ताकत।
ब्लॉग से साभार
पुण्य प्रसून वाजपेयी
अमेरिका में रूपर्ट मर्डोक प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो मर्डोक ने मोदी को आजादी के बाद से भारत का सबसे शानदार पीएम करार दे दिया। मर्डोक अब अमेरिकी राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। ओबामा पर अश्वेत प्रेजिडेंट न मानने के मर्डोक के बयान पर बवाल मचा ही हुआ है। अमेरिका में अपने न्यूज चैनल को चलाने के लिए मर्डोक आस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़ अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं, तो क्या मीडिया टाइकून इस भूमिका में आ चुके हैं कि वह सीधे सरकार और सियासत को प्रभावित कर सकें या कहें राजनीतिक तौर पर सक्रिय ना होते हुए भी राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए काम कर सके।
अगर ऐसा हो चला है तो यकीन मानिए अब भारत में भी सत्ता-मीडिया का नैक्सेस पेड न्यूज से कहीं आगे निकल चुका है। जहां अब सत्ता के लिए खबरों को नए सिरे से बुनने का है या कहे सत्तानुकुल हालात बने रहें, इसके लिए दर्शकों के सामने ऐसे हालात बनाने का है जिसे देखते वक्त दर्शक महसूस करें कि अगर सत्ता के विरोध की खबर है तो खबर दिखाने वाला देश के साथ गद्दारी कर रहा है।
यानी पहली बार मीडिया या पत्रकारिता की इस धारणा को ही मीडिया हाउस जड़-मूल से खत्म करने की राह पर निकल पड़े हैं कि पत्रकारिता का मतलब यह कतई नहीं है कि चुनी हुई सरकार के कामकाज पर निगरानी रखी जाए। यानी सत्ता को जनता ने पांच साल के लिए चुना है तो पांच बरस के दौर में सत्ता जो करे जैसा करे वह देश हित में ही होगा। जाहिर है यह बेहद महीन लकीर है, जहां मीडिया का सत्ता के साथ गठजोड़ मीडिया को भी राजनीतिक तौर खड़ा कर दें और सत्ता भी मीडिया को अपना कैडर मान कर बर्ताव करें।
यह घालमेल व्यवसायिक तौर पर भी लाभदायक साबित हो जाता है। यानी सत्ता के साथ खड़े होने की पत्रकारिता इसका एहसास होने ही नहीं देती है कि सत्ता कोई लाभ मीडिया हाउस को दे रही है या मीडिया सत्ता की राजनीति का प्यादा बनकर पत्रकारिता कर रही है। इसके कई उदाहरणों को पहले समझें। बिहार चुनाव में किसी भी अखबार या न्यूज चैनल की हेडलाइन नीतीश कुमार को पहले अहमियत देती है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का नंबर आएगा और फिर लालू प्रसाद यादव का।
यानी कोई भी खबर जिसमें नीतीश कह रहे होंगे या नीतीश को निशाने पर लिया जा रहा होगा वह खबर नंबर एक हो जाएगी। इसी तर्ज पर मोदी जो कह रहे होंगे या मोदी निशाने पर होंगे उसका नंबर दो होगा। कोई भी कह सकता है कि जब टक्कर इन्हीं दो नेताओं के बीच है, तो खबर भी इन्हीं दो नेताओं को लेकर होगी।
तो सवाल है कि जब सुशील मोदी कहते हैं कि सत्ता में आए तो गो-वध पर पांबदी होगी। तो उस खबर को ना तो कोई पत्रकार परखेगा और ना ही अखबार में उसे प्रमुखता के साथ जगह मिलेगी। लेकिन जब नीतीश इसके जबाब में कहेंगे कि बिहार में तो साठ बरस से गो-वध पर पाबंदी है तो पत्रकार के लिए वह बड़ी खबर होगी। इसी तर्ज पर केन्द्र का कोई भी मंत्री बिहार चुनाव के वक्त आकर कोई भी बड़े से बड़ा नीतिगत फैसले की जानकारी चुनावी रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें, उसको अखबार में जगह नहीं मिलेगी। ना ही प्रधानमंत्री मोदी के किसी बड़े फैसले की जानकारी देने को अखबार या न्यूज चैनल दिखाएंगे। यानी पीएम मोदी के बयान में जब तक नीतीश–लालू को निशाने पर लेने का मुलम्मा ना चढ़ा हो, वह खबर बन ही नहीं सकती।
यानी खबरों का आधार नेता या कहें सियासी चेहरों को उस दौर में बना दिया गया जब सबसे ज्यादा जरूरत ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उसके बाद चेहरों की प्राथमिकता सत्ता के साथ गठजोड़ के जरिए कुछ इस तरह से पाठकों में या कहें दर्शकों में बनाते हुए उभर कर आयी, जिससे ग्राउंड रिपोर्टिंग या आम जनता से जुड़े सरकारी फैसलों को परखने की जरुरत ही ना पड़े। उसकी एवज में सरकार के किसी भी फैसले को सकारात्मक तौर पर तमाम आयामों के साथ इस तरह रखा जाये जिससे पत्रकारिता सूचना संसार में खो जाये।
मसलन, झारखंड विश्व बैंक की फेरहिस्त में नंबर 29 से खिसक कर नंबर तीन पर आ गया। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी बांका की अपनी चुनावी रैली में यह कहते हुए देते है कि नीतीश बिहार को 27वें नंबर से आगे ना बढ़ा पाए, तो खबरों के लिहाज से नीतीश पर हमले या उनकी नाकामी या झारखंड में बीजेपी की सत्ता आने के बाद उसके उपलब्धि से आगे कोई पत्रकारिता जाएगी ही नहीं। यानी झारखंड में कैसे सिर्फ खनन का लाइसेंस नए तरीके से सत्ता के करीबियो को बांटा गया और खनन प्रक्रिया का लाभ झरखंड की जनता को कम उघोगपतियों को ज्यादा हो रहा है। इसपर कोई रिपोर्टिंग नहीं और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट झारखंड के लोगों की बदहाली या इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में सबकुछ कैसे ठप पड़ा है या फिर रोजगार के साधन और ज्यादा सिमट गये हैं, इस पर केन्द्रित होता ही नहीं है।
तो नई मुश्किल यह नहीं है कि कोई पत्रकार इन आधारों को टटोलने क्यों नहीं निकलता। मुश्किल यह है कि जो प्रधानमंत्री कह दें या बिहार में जो नीतीश कह दें उसके आगे कोई लकीर इस दौर में पत्रकारिता खिंचती नहीं है या पत्रकारिता के नए तौर तरीके ऐसे बना दिए गए हैं जिससे सत्ता के दिए बयान या दावों को ही आखिरी सच करार दे दिया जाए।
अब यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसे हालात पेड मीडिया के आगे कैसे हैं और इस नए हालात के मायने हैं क्या? असल में मीडिया के सरोकार जनता से हटते हुए कैसे सत्ता से ज्यादा बनते चले गए और सत्ता किस तरह मीडिया पर निर्भर होते हुए मीडिया के तौर तरीकों को ही बदलने में सफल हो गया। समझना यह भी जरुरी है। मौजूदा वक्त में मीडिया हाउस में कॉरपोरेट की रुची क्या सिर्फ इसलिए है कि मीडिया से मुनाफा बनाया कमाया जा सकता है? या फिर मीडिया को दूसरे धंधो के लिए ढाल बनाया जा सकता है, तो पहला सच तो यही है कि मीडिया कभी अपने आप में बहुत लाभ कमाने का धंधा रहा ही नहीं है। यानी मीडिया के जरिए सत्ता से सौदेबाजी करते हुए दूसरे धंधों से लाभ कमाने के हालात देखे जा सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालात जिस तेजी से बदले हैं या कहें बदल रहे हैं उसमें मीडिया की मौजूदगी अपनी आप में सत्ता होना हो चला है और उसकी सबसे बड़ी वजह है, बाजार का विस्तार। उपभोक्ताओं की बढ़ती तादाद और देश को देखने समझने का नजरिया। तमाम टेक्नॉलाजी या कहें सूचना क्रांति के बाद कहीं ज्यादा तेजी से शहर और गांव में संवाद खत्म हुआ है।
भारत जैसे देश में आदिवासियों का एक बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या से कोई संवाद देश की मुख्यधारा का है ही नहीं है। इतना ही नहीं दुनिया में आवाजाही का विस्तार जरूर हुआ लेकिन संवाद बनाना कहीं ज्यादा तेजी से सिकुड़ा है, क्योंकि सुविधाओं को जुगाड़ना, या जीने की वस्तुओं को पाने के तरीके या फिर जिंदगी जीने के लिए जो मागदौल बाजारनुकुल है उसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी या मीडिया की ही हो चली है। यानी कल तो हर वस्तु के साथ जो संबंध मनुष्य का बना हुआ था वह घटते-घटते मानव संसाधन को हाशिए पर ले आया है। यानी कोई संवाद किसी से बनाए बगैर सिर्फ टेक्नोलॉजी के जरिए आपके घर तक पहुंच सकती है। चाहे सब्जी फल हो या टीवी-फ्रिज या फिर किताब खरीदना हो या कंप्यूटर। रेलवे और हवाई जहाज के टिकट के लिए भी अब उफभोक्ताओं को किसी व्यक्ति के संपर्क में आने की कोई जरुरत है ही नहीं। सारे काम, सारी सुविधा की वस्तु, या जीने की जरूरत के सामान मोबाइल–कंप्यूटर के जरिए अगर आपके घर तक पहुंच सकते हैं तो उपभोक्ता समाज के लिए मीडिया की जरूरत सामाजिक संकट, मानवीय मूल्यों से रूबरू होना या देश के हालात हैं क्या या किसी भी घटना विशेष को लेकर जानकारी तलब करना क्यों जरुरी होगा?
खासकर भारत जैसे तीसरी दुनिया के देश में जहां उपभोक्ताओं की तादाद किसी भी यूरोप के देश से ज्यादा हो और दो जून के लिए संघर्ष करते लोगों की तादाद भी इतनी ज्यादा हो कि यूरोप के कई देश उसमें समा जाए, तो पहला सवाल यही है कि समाज की असमानता और ज्यादा बढ़ सके। इसके लिए मीडिया काम करेगा या दूरियां पाटने की दिशा में रिपोर्ट दिखाएगा। जाहिर है मीडिया भी पूंजी से विकसित होता माध्यम ही जब बना दिया गया है और असमानता की सबसे बड़ी वजह पूंजी कमाने के असमान तरीके ही सत्ता की नीतियों के जरिए विस्तार पा रहे हो तो रास्ता जाएगा किधर। लेकिन यह तर्क सतही है। असल सच यह है कि धीरे-धीरे मीडिया को भी उत्पाद में तब्दील किया गया। फिर मीडिया को भी एहसास कराया गया कि उत्पाद के लिए उपभोक्ता चाहिए। फिर उपभोक्ता को मीडिया के जरिए ही यह सियासी समझ दी गई कि विकास की जो रेखा राज्य सत्ता खींचे वही आखरी सच है।
ध्यान दें तो 1991 के बाद आर्थिक सुधार के तीन स्तर देश ने देखें। नरसिंह राव के दौर में सरकारी मीडिया के सामानांतर सरकारी मंच पर निजी मीडिया हाउस को जगह मिली। उसके बाद वाजपेयी के दौर में निजीकरण का विस्तार हुआ। यानी सरकारी कोटा या सब्सिडी भी खत्म हुई। सरकारी उपक्रम तक की उपयोगिता पर सवालिया निशान लगे।
मनमोहन सिंह के दौर में बाजार को पूंजी के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। यानी पूंजी ही बाजार का मानक बन गई और मोदी के दौर में पहली बार उस भारत को मुख्यधारा में लाने के लिए पूंजी और बाजार की खोज शुरू हुई जिस भारत को सरकारी पैकेज तले बीते ढाई दशक से हाशिए पर रखा गया था। पहली बार खुले तौर पर यह मान लिया गया कि 80 करोड़ भारतीयों को तभी कुछ दिया जा सकता है जब बाकी तीस करोड़ उपभोक्ताओं के लिए एक सुंदर और विकसित भारत बनाया जा सके। लेकिन इस सोच में यह कोई समझ नहीं पाया कि जब पूंजी ही विकास का रास्ता तय करेगी तो सत्ता कोई भी हो वह पूंजी पर ही निर्भर होगी और वह पूंजी कही से भी आए और सत्ता के पूंजी पर निर्भर होने का मतलब है वह तमाम आधार भी उसी पूंजी के मातहत खुद को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत पाएंगें जो चुनी हुई सत्ता के हाथ में नहीं बल्कि पूंजी के जरिए बाजार से मुनाफा बनाने के लिए देश की सीमा नहीं बल्कि सीमाहीन बाजार का खुलापन तलाशेंगे।
ध्यान दें तो मीडिया हाउसों की साख खबरों से इतर टर्न ओवर पर टिकी है। सेल्स या मार्केटिंग टीम न्यूज रूम पर भारी पड़ने लगी, तो संपादक भी मैनेजर से होते हुए पूंजी बनाने और जुगाड़ कराने से आगे निकलते हुए सत्ता से वसूली करते हुए खुद में ही सत्ता बनने के दरवाजे पर टिका। प्रोपराइटर का संपादक हो जाना। समाचार पत्र या न्यूज चैनल के लिए पूंजी का जुगाड़ करने वाले का संपादक हो जाना। यह सब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चलता रहा। लेकिन जिस तर्ज पर 2014 के लोकसभा चुनाव ने सत्ता के बहुआयामी व्यापार को खुल कर सामने रख दिया उसमें खबरों की दुनिया से जुड़ें पत्रकारों और मालिकों को सामने पहली बार यह विकल्प उभरा कि वह सरकार की नीतियों को उसके जरिए बनाये जाने वाली व्यवस्था के साथ कैसे हो सकते हैं और राज्य के हालात खुद ब खुद उसे मदद दे देगा या फिर उसे खत्म कर देगा। यानी साथ खड़े हैं तो ठीक नहीं तो दुश्मन।
यह हालात इसलिए पेड न्यूज से आगे आकर खड़े हो गए क्योंकि चाहे अनचाहे अब राज्य को अपने मीडिया बजट का बंदर बांट अपने साथ खड़े मीडिया हाउस में बांटने के नहीं थे। बल्कि सत्ता की अकूत ताकत ने खबरों को परोसने के सलीके में भी सत्ता की खुशबू बिखेरनी शुरू कर दी। सामाजिक तौर पर सत्ता मीडिया के साथ कैसे खड़ी होगी यह मीडिया के सत्ता के लिए काम करने के मिजाज पर आ टिका। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं पत्रकारों के साथ डिनर करेंगे जो उनकी चापलूसी में माहिर होगा और पटना में नीतीश कुमार उन्हीं पत्रकारों को आगे बढ़ाने में सहयोग देगें जो उनके गुणगाण करने से हिचकेगा नहीं। इसलिए कोई पत्रकार दिल्ली में मोदी हो गया तो कोई पत्रकार पटना में नीतीश कुमार और जो-जो पत्रकार सत्ता से खुले तौर पर जुड़ा नजर आया उसे लगा कि वह खुद में सत्ता है। यानी सबसे ताकतवर है।
असल में बिहार चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण हो चला है कि पहली बार नायकों की खोज से चुनाव जा जुड़ा है। यानी 1989 में लालू यादव मंडल के नायक बनें तो 2010 में नीतीश सुशासन के नायक बनें और 2014 के चुनाव में नरेन्द्र मोदी देश के विकास नायक बन कर उभरे। ध्यान दें तो इसके अलावा सिर्फ दिल्ली के चुनाव ने केजरीवाल के तौर पर नायक की छवि गढ़ी। लेकिन केजरीवाल का नायककत्व पारंपरिक राजनीतिक को बदलने के लिए था ना कि नायक बन कर उसमें ढलने के लिए।
लेकिन 2015 के आखिर में बिहार चुनाव की जीत हार में तय यही होना है कि विदेशी पूंजी और खुले बाजार व्यवस्था के जरिए भारत को बदलने वाला नायक चाहिये या फिर जातिय गठबंधन के आसरे सामाजिक न्याय की सोच को आगे बढ़ाने वाला नायक चाहिये। जाहिर है बिहार जिस रास्ते पर जाएगा उसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव के केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की नायक छवि है और दूसरी तरफ चकाचौंध नायकत्व को चुनौती देने वाले नीतीश– लालू हैं। यानी यही हालात यूपी में भी टकराएंगें। अगर बिहार लालू नीतीश का रास्ता चुनता है तो यकीन मानिए मुलायम-मायावती भी दुश्मनी छोड़ गद्दी के लिए साथ आ खड़े होंगे ही। यानी 2 जून 1995 का गेस्ट हाउस कांड एक याद भर रह जाएगा और इससे पहले जो थ्योरी गठबंधन के फॉर्मूले में फेल होती रही वह फॉर्मूला चल पड़ेगा। यानी दो बराबर की पार्टियों में गठबंधन।
जाहिर है राजनीतिक बदलाव का असर मीडिया पर भी पड़ेगा। क्योंकि सत्ता के साथ वैचारिक तौर पर खड़े होकर पूंजी या मुनाफा बनाने से आगे खुद को सत्ता मानने की सोच को मान्यता मिले या सत्ता के सामाजिक सरोकार का ताना-बाना बुनते हुए कॉरपोरेट या पूंजी की सत्ता को ही चुनौती देनी वाली पत्रकारिता रहे। फैसला इसका भी होना है, लेकिन दोनों हालात छोटे घेरे में मीडिया को वैसे ही बड़ा कर रहे है जैसे अमेरिका में मर्डोक सत्ता को प्रभावित करने की स्थिति में है वैसे ही भारत में सत्ता के लिए मीडिया सबसे असरकारक हथियार बन चुका है। फर्क इतना ही है कि वहां पूंजी तय कर रही है और भारत में सत्ता की ताकत।
ब्लॉग से साभार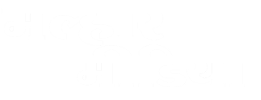
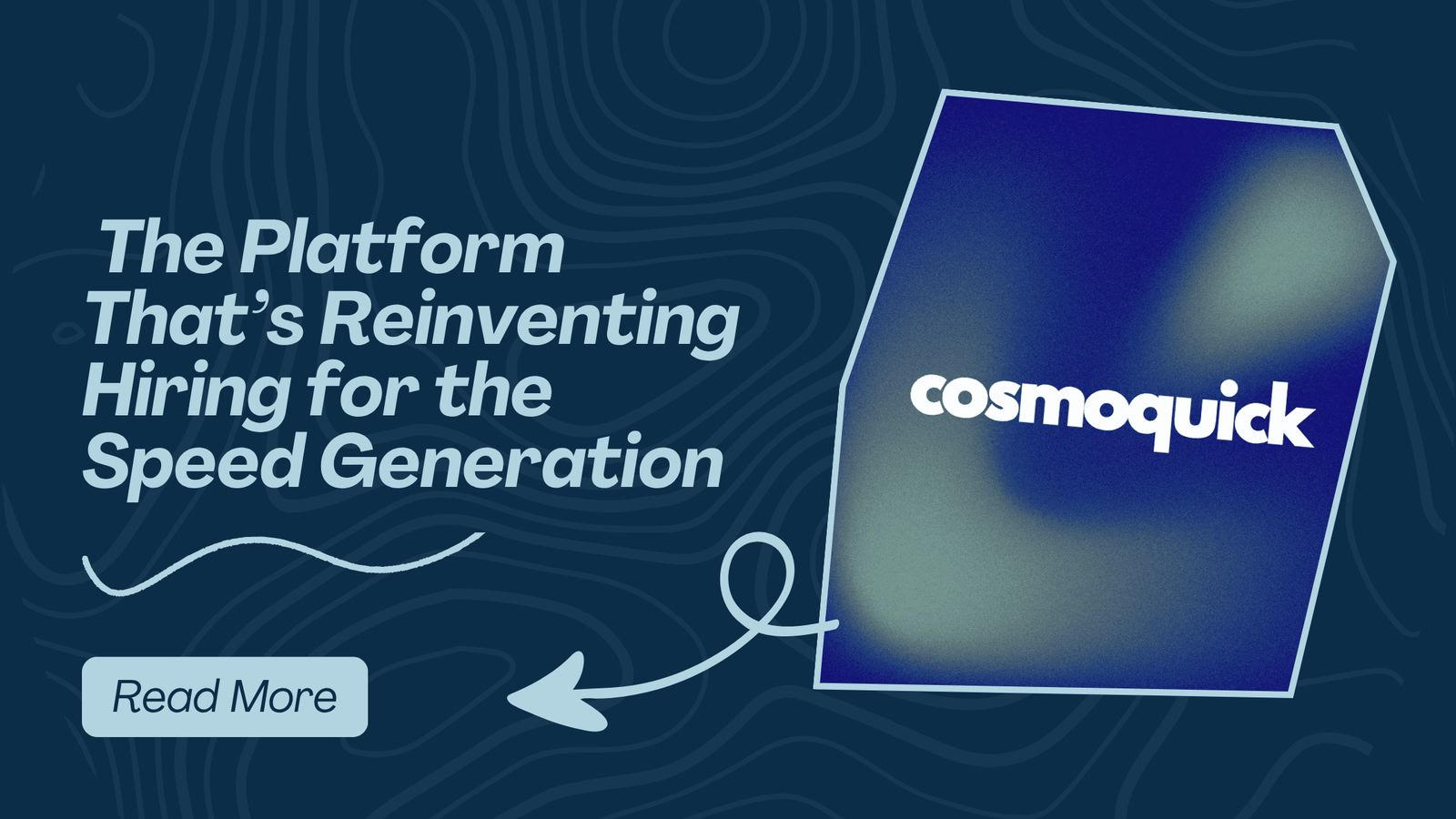





Comments