
ममता यादव।
पत्रकारों के प्रोफेशनल कार्यव्यवहार को प्रभावित करती हैं यह मूल व्यवहारिक समस्याएं जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के दायरे में भी आती हैं।
पत्रकारिता को मूल पेशा नहीं बना पाना मजबूरी, सामाजिक पारिवारिक असुरक्षा का भाव, नौकरियों की अनिश्चितता, वेतन विसंगती, भरण-पोषण का संघर्ष, बाकी अन्य खतरे तो मूल पत्रकारों के सामने जगजाहिर हैं ही।
पत्रकारिता के क्षेत्र में एक शब्द का काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसे पिंक स्लिप कहते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह संपादक हो या रिपोर्टर, जो कार्यालय जाता है, उसे यह पता नहीं होता कि उसका कल भी काम पर जाना जारी रहेगा।
पत्रकारों के अधिकार भी महत्त्वपूर्ण हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। क्योंकि दावे और प्रतिवाद हैं और जब तक पत्रकार को इससे सुरक्षा नहीं मिलती, वे ठीक से और ईमानदारी से काम नहीं कर सकते हैं। पत्रकार समाज की बेहतर सेवा के लिए मानवाधिकारों के ज्ञान से खुद को मजबूत करें।
वर्ष 2018 में मीडिया क्षेत्र में नौकरियों की अनिश्चितता के मुद्दे की चर्चा करते हुए भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआइ) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सीके प्रसाद ने यह बात कही थी।
वर्ष 2018 के पहले और बाद में भी पत्रकारों की सामाजिक स्थिति में बहुत बदलाव नहीं आया है। न काम के घंटे तय हैं, न नौकरी की निश्चितता है न ही जीवनयापन का कोई ठोस आधार।
पत्रकार को जनता की आवाज उठाने वाला एक सशक्त माध्यम माना जाता है।
जनता को उम्मीद होती है कि पत्रकार हमारी बात को सही जगह सही लोगों तक पहुंचाने में सक्षम है। अघोषित रूप से तमाम तरह की आवाजों, समस्याओं को उठाने वाले पत्रकारों को व्यवहारिक रूप में ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
संवैधानिक नजरिए से देखें तो पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का न तो संरक्षण हो पाता है न ही उनका वे ठीक से उपयोग कर पाते हैं। अगर जीने के अधिकार की ही तो बात करें तो सामान्य जीवनयापन के लिए भी पत्रकारों को कड़ा संघर्ष हर स्तर पर करना होता है।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवनयापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं।
ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं । विधि के शासन की स्थापना करना, संविधान में मोलिक अधिकारों को शामिल करने का एक उद्देश्य है।
पत्रकार भी एक मानव है और उसके भी वही अधिकार हैं जो कि एक सामान्य भारतीय नागरिक के हैं। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो बतौर मानव सबसे ज्यादा प्रभावित अगर मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो पत्रकारों के अधिकार न सिर्फ प्रभावित होते हैं बल्कि उनका हनन भी होता रहता है।
वेतन विसंगती, आय की अनिश्चतता ही पत्रकारों की व्यवहारिक समस्याओं का मूल है और यह उनके व्यक्तिगत जीवन को इस कदर प्रभावित करता है कि कहीं न कहीं उसके मूल अधिकार ही खोने लगते हैं और पत्रकार जीवनयापन की मजबूरी और अन्य दबावों के कारण इसे चुपचाप झेलते भी हैं।
एक सामान्य जीवनशैली के यापन के लिए भी अमूमन पत्रकारों को जूझना पड़ता है। अगर गंभीर बीमारी हो जाए तो इलाज के लिए मोहताज, मृत्यु हो जाए तो कई बार कफन-दफन के लिए भी मोहताज।
इसी बात को तथ्यपूर्ण तरीके से रखते हुए नवीन रंगियाल कहते हैं श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम लंबे समय से लागू है, लेकिन हकीकत में देश में कोई भी संस्थान उसका पालन नहीं करता, ना ही खुद पत्रकार इसके लिए मुखर हैं।
कुल मिलाकर इस अधिनियम का कोई फायदा नहीं।
यह सही है की पत्रकारिता कोई 9 से 5 का व्यवसाय नहीं है, लेकिन फिर भी काम के घंटे की कोई तो सीमा हो।
बीमारी, हादसों आदि में मरने वाले पत्रकारों के परिवार वालों को कोई नहीं पूछता। उनके लिए कोई सरकारी योजना नहीं, जितना पत्रकार खुद अपने स्तर पर कर लेते हैं बस उतना ही है उनके लिए।
न संस्थान की तरफ से और न ही सरकार की तरफ से कोई राहत है पत्रकारों के परिवार के लिए।
मानिसाना आयोग, पालेकर आयोग और मजीठिया जैसे आयोग पत्रकारों के लिए बने। बावजूद इसके पत्रकारों की हालात ज्यादा खराब हो गई।
मजीठिया आयोग के बाद तो उल्टे पत्रकार ही दबाव में आ गए, जिन्होंने अपने मुद्दों के लिए आवाज उठाने की कोशिश की वे नौकरी से भी गए।
किसी को कोर्ट में प्रताड़ित किया गया तो किसी को अपनी प्रेस की ताकत से दबा दिया गया।
पत्रकारों के लिए ईमानदारी से काम करने वाला, उनकी आवाज उठाने वाला अब तक कोई संगठन नहीं है।
90 प्रतिशत ऐसे पत्रकार जो ईमानदार हैं, वे अपनी ईमानदारी की सजा भुगत रहे हैं।
दूसरों के मुद्दे उठाने वाला पत्रकार खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता, वो आज भी असुरक्षा के भाव में जी रहा है।
लगातार बढ़ते तनाव की वजह से पत्रकारिता उसका मिशन नहीं मजबूरी हो गई है।
क्या आपने भारतीय संविधान पढ़ा, जाना और समझा है? के जवाब में नवीन कहते हैं
पत्रकारिता में रहते हुए जितना अपने मौलिक अधिकारों को जान पाए, जितना संविधान के बारे में समझ और सुन पाए उतना ही पता है।
कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ काम करने की वजह से वाचिक परंपरा के जरिए जानने समझने को मिला।
इसके अलावा संविधान के बारे में कभी गहनता से जानने या पढ़ने की कोशिश नहीं की और न ही समय ही मिल सका।
बात वही आ जाती है की दूसरों के मुद्दे और विषय उठाने, प्रकाशित करने और उनके सरोकारों के चलते खुद के प्रति कभी उतनी जागरूकता महसूस ही नहीं की।
हां, एक नागरिक होने के नाते हम अपने सिविक सेंस के प्रति हमेशा सचेत रहे, नियमों का पालन किया। कभी प्रेस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, किसी को धौंस नहीं दी और न ही पत्रकार होने के नाते किसी तरह की अराजकता को बढ़ावा दिया। इसी सेंस की वजह से हमने अपने साथ होने वाले अन्याय को कई बार let it go किया, जाने दिया।
हां, यह पेशा निजी तौर पर अब इतना प्रिय इसलिए बन गया है कि इसकी वजह से हम ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा सजग महसूस करते हैं।
अपने आसपास चलने वाले तमाम हजारों गैर पत्रकार लोगों और अपने बीच के इस फर्क की खाई हमेशा महसूस होती रही है।
इंदौर के ही वरिष्ठ पत्रकार अमित त्रिवेदी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की पहली लाईन ही पूरे पत्रकारिता जगत की मूल समस्या और मौलिक अधिकारों की उपेक्षा को इंगित करती है।
अमित कहते हैं पत्रकारों की सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या है पत्रकारिता को अपना मूल पेशा नहीं बना पाना। पत्रकारिता से घर नहीं चल सकता है।
हां अगर हालात पक्षधर हों तो सबकुछ हो सकता है। क्योंकि फिर आप सत्तापक्ष या अधिकारियों से बुराई नहीं ले सकते। इसका सीधा मतलब हुआ आप पत्रकार होकर भी पत्रकार नहीं बचते।
फिर आपको विज्ञापन अखबार या आपका चैनल सिफर कर सके उन स्थितियों से समझौता करना पड़ता है। लिहाजा आपकी कलम की धार तेज नहीं रह जायेगी।
अखबार मालिक भी परिस्थियों से समझौता कर रहे हैं, ज्यादा कुछ सच्चाई बयान करने की कोशिश की जाए तो फिर कार्यवाही या परंपरागत आरोप पैसे मांगने के लिए तैयार रहिए।
अमित आगे कहते हैं बात रही संविधान की तो यह कड़वा सच है की संविधान द्वारा पत्रकारों को कोई भी शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है।
यह कहना सही होगा पत्रकारिता स्वयंभू चौथा स्तंभ है। दरअसल पत्रकारिता की शुरुआत भारत में तो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर की गई थी।
अंग्रेजों के समय इतनी बंदिशे नही थी जो आज के परिदृश्य में पत्रकारों के ऊपर लगाई जा चुकी हैं। यह हालात पत्रकारिता को खत्म करने के लिए काफी हैं।
वे कहते हैं मैं इंदौर में पिछले 15 सालों से पत्रकार हूं लेकिन जो स्थिति पत्रकारिता की होती जा रही है वह सीधे तौर पर पत्रकार और पत्रकारिता का अंत जैसा महसूस कराने के लिए काफी हैं।
20 साल से पत्रकारिता कर रहे सागर के चैतन्य सोनी पत्रकारों की कार्य व्यावहारिक समस्याएँ बताते हुए कहते हैं परिवार के भरण पोषण के दबाव, बँधी सेलरी की आस में पत्रकार ही सबसे शोषित वर्ग बन गया है।
मीडिया संस्थानों में रिपोर्टर स्तर और अब रिपोर्टिंग के साथ लाखों रुपए के विज्ञापन लाने का दबाव बनाया जा रहा है।
सरकार, मंत्रियों, आला अधिकारियों के खिलाफ लिखने की मनाही, कारण 15 अगस्त, 26 जनवरी पर विज्ञापन के नाम पर मोटा पैकेज वसूली।
ऑफिस में स्टॉफ की छटनी, दो या तीन रिपोर्टर के भरोसे पूरा जिले का कवरेज। काम का माहौल ही नहीं रहा।
मौलिक अधिकारों को बिलकुल पढ़ा है, लेकिन बतौर पत्रकार इसे अपने अपने संस्थान में अपना नहीं पाते।
सागर के जैसीनगर जैसे ग्रामीण कस्बे में पत्रकारिता कर रहे बृजेंद्र रायकवार कहते हैं,
मीडिया के व्यवसायी करण से ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों को आस थी कि शहरी पत्रकारों के साथ वेतन विसंगति दूर होते हुए उन्हें भी इसका लाभ होगा लेकिन उनकी ये उम्मीद बदलते वक्त के साथ जस की तस हैं।
ग्रामीण स्तर पर पत्रकारिता करने वाले पत्रकार अभी भी मुख्य धारा के पत्रकारिता से स्वयं का जुड़ाव ना कर पाना मुख्य व्यवहारिक समस्या है।
पत्रकारिता अभी उनका सिर्फ पार्ट टाइम वर्क बनकर रहा गया है, इसका सीधा कारण वेतन विसंगति है।
ग्रामीण स्तर के पत्रकारों को अपने ही मीडिया संस्थान से सुरक्षा ना मिलना भी सबसे बड़ी समस्या हैं, अमूनन सत्ता के असफलता की खबर प्रदर्शन करने के बाद पत्रकारों पर पड़ने वाले दबाब में स्वम को अकेला महसूस करते हैं
पत्रकारिता लाइन से होने के नाते अक्सर संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को पढ़ता रहता हूँ, और जैसा कहा गया पत्रकारिता की आजादी ही संविधान में दिए गए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का मूल आधार है।
लेकिन आज के समय मे पत्रकारिता के इन्ही मौलिक अधिकारों को दबाने का भरसक प्रयास हर उस सत्ताधीश अथवा उस अधिकारी द्वारा किया जाता हैं जिसकी भ्रष्टाचार की ख़बर अखबार के पन्ने पर छपती हैं।
ग्रामीण स्तर पर अकेले पड़ जाने वाला पत्रकार में डर की भावना ग्रसित होता जाता है और कई विसंगतियों के कारण न तो अपने मौलिक अधिकारों का व्यवहारिक रूप में कर पाता है न ही अपने मानवीय मूल्यों की रक्षा पत्रकारिता में कर पाता है।
विषय की बाध्यता होने के बावजूद बतौर पत्रकार स्वयं भी मुझे यह सवाल बहुत कचोटते हैं और एक सवाल जो हमेशा दिमाग में जमा रहता है पत्रकारों को आप इंसान की जमात में तो मानते हैं कि नहीं?
यूं ही किसी वरिष्ठ पत्रकार द्वारा कह दिया जाता है कि घर चलाने पत्रकारिता में मत आईए तो प्रतिप्रश्न उठता है कि जीवनयापन के मूल साधन भी न जुटा पाए अपने ही मूल अधिकार नहीं ले पाये तो फिर बतौर मानव सर्वाईवल का क्या उपाय है?
इस फील्ड जैसी दुश्वारियां कहीं नहीं हैं। समस्याओं के समाधान पर बात करने से खुद पत्रकार ही कतराते हैं।
निष्कर्ष यह कि मौलिक अधिकारों को पत्रकार पढ़ते तो हैं, समझते हैं पर स्वजागरूकता का अभाव यहां भी उतना ही है जितना अन्य किसी सामान्य नागरिक में हो सकता है या होता है।
ऐसी ही कुछ व्यवहारिक समस्याओं के मद्देनजर 100 से ज्यादा पत्रकारों को यह दो सवाल भेजे गए थे। 100 में से 4 पत्रकारों ने प्रतिक्रयाएं लिखित में दीं कुछ ने फोन पर और ज्यादातर ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा।
इस रिपोर्ट को तैयार करने पत्रकारों को सवाल भेजे गए थे
1) पत्रकारों की मुख्य व्यवहारिक समस्याएं क्या हैं?
2) क्या आपने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को पढ़ा, समझा, जाना है? खुद के जीवन में व्यहारिक तौर कितना अमल कर पाते हैं
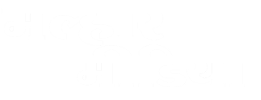
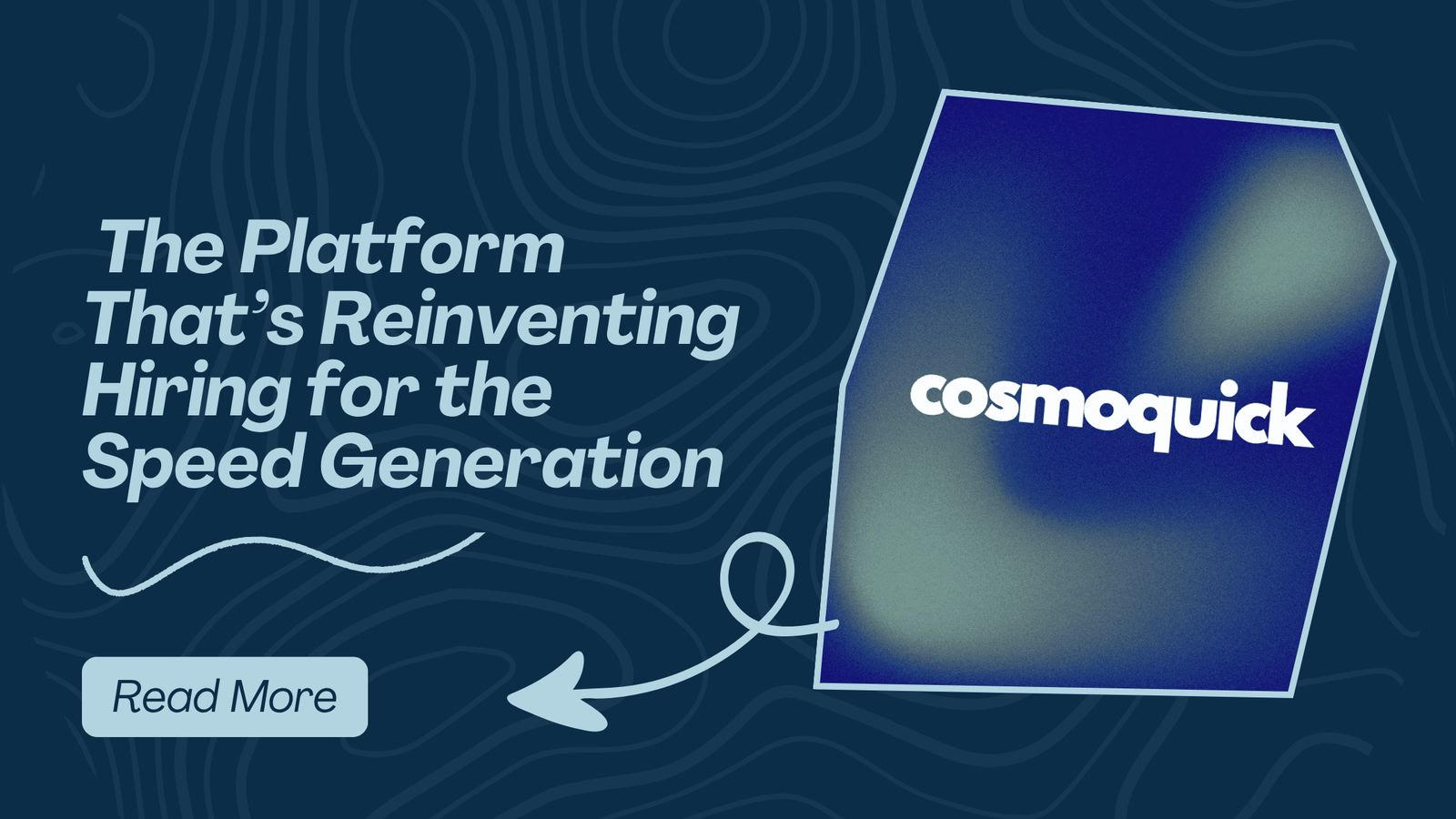
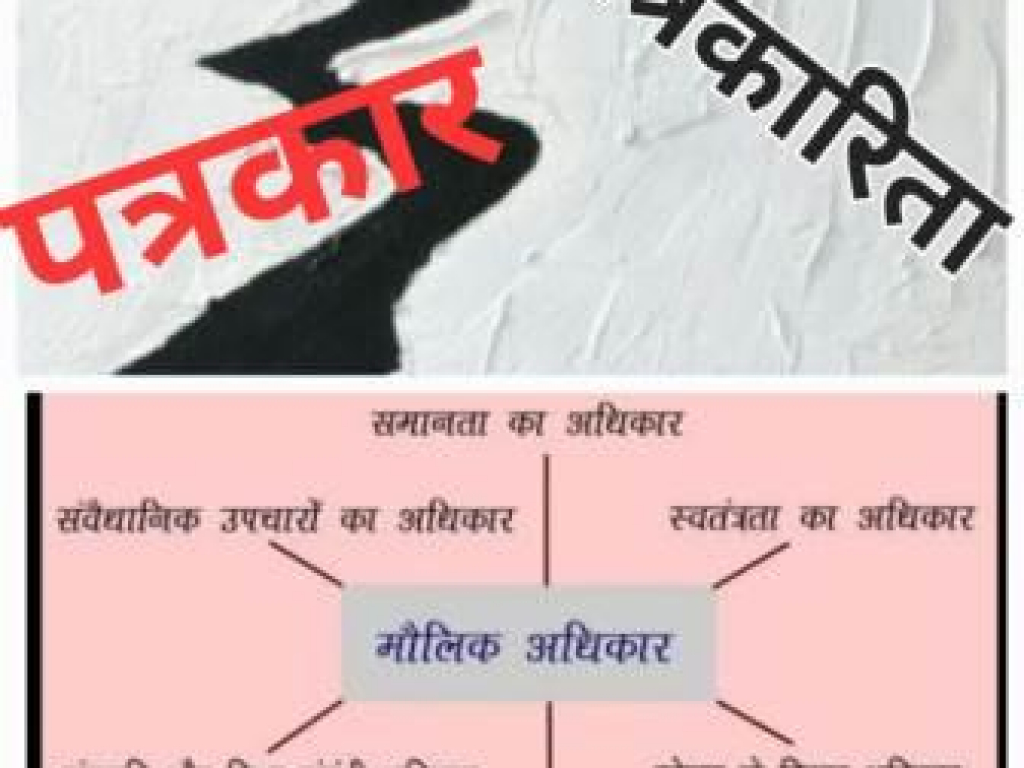





Comments