 मनोज कुमार।
मनोज कुमार।
जब हम सब स्कूल में पढ़ते थे तो एक स्वाभाविक सी आदत होती थी कि हम अपनी गलती दूसरों पर ढोल दें। ऐसा करके हम कुछ समय के लिये डांट से बच जाते थे लेकिन इससे हमें ही नुकसान होता था। इस बात को कितने लोगों ने समझा और सीखा, मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे जल्द ही अपनी गलती का अहसास हो गया और कोशिश करके अपनी गलती अपने सिर लेने लगा। इससे मुझे दो फायदे हुये जिसमें पहला यह कि पोल खुल जाने पर बड़ी सजा का डर मन से खत्म हो गया और दूसरा अपनी गलती मान लेने पर आत्मविश्वास जागने लगा। आज जब उम्र के पचास के आसपास हूं तो यह मेरी शक्ति बन चुका है।
खैर, इन दिनों इसी को संबद्ध करते हुये एक नये अनुभव से गुजर रहा हूं। अखबारों में छपने वाले लेख के आखिरी में सारी जवाबदारी लेखक पर थोपते हुये कि व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं, इनसे समाचार पत्र का कोई लेना-देना नहीं है। अखबारों में इन पंक्तियों ने मेरे बचपन की यादें ताजा कर दी हैं। ऊपर जो बातें मैंने लिखी, वह इन पंक्तियों से बहुत अलग नहीं है।
अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब अखबारों में सम्पादक नाम की संस्था होती है और वह प्रकाशन के पूर्व लेखों के तथ्य और तर्क को अखबार की नीति की कसौटियों पर जांचता है और जांचने के बाद प्रकाशन के लिये सहमत होता है। ऐसी स्थिति में लेख में व्यक्त विचारों के प्रति अकेला लेखक कैसे जवाबदार हो सकता है? सम्पादक जिसने लेख को जांचा-परखा और अपनी रजामंदी की मुहर ठोंकी, वह इससे कैसे बरी हो सकता है?
यदि ऐसा है तो सम्पादक संस्था की जरूरत ही नहीं है और शायद ऐसा हो रहा है इसलिये ही सम्पादक संस्था का ह्रास हो रहा है। यदि सम्पादक संस्था है तो वह पहले जवाबदार है कि उसने बिना जांचे-परखे और अखबार की नीतियों की कसौटी पर परखे बिना अपनी रजामंदी की मुहर कैसे लगा दी।
दुर्भाग्य से विचार लेखक के निजी हैं, इनसे समाचार पत्र का कोई लेना-देना नहीं है, जैसे जवाबदारी से बचने वाली पंक्तियों के खिलाफ लगभग सब लोग मौन हैं, स्वयं लेखक भी। मैंने इस संबंध में कई लोगों से बात की तो उनका कहना होता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका अर्थ तो यह होता है कि जिस तरह सम्पादक की पंक्तियों का कोई असर नहीं होता है, उसी तरह लेख में व्यक्त विचार समाज को न तो दिशा देते हैं और न उद्वेलित करते हैं। लेखक लिखने की औपचारिकता पूरी कर रहा है और सम्पादक और अखबार खाली जगह को भरने की।
ऐसे में जवाबदारी और जिम्मेदारी जैसे भारी-भरकम शब्द बहुत बौने से हो जाते हैं। पाठक अब पत्र लिखते नहीं हैं और जो पत्र प्रकाशित भी होते हैं, वे देश की बड़ी समस्याओं पर होते हैं। मुझे स्मरण हो आता है कि मेरे 30 वर्षों से ज्यादा की पत्रकारिता में दो-तीन अवसर ऐसे आये जब हमारे अखबार में छपे लेख और खबर पर पूरा शहर टूट पड़ा था। तथ्य और तर्क को लेकर पाठक का अपना पक्ष था। यहां तक कि वह प्रूफ की गलतियां भी झेल नहीं पाता था लेकिन तब भी किसी सम्पादक ने साहस नहीं किया कि वह लेख के आखिर में चिपका दे कि विचार लेखक के निजी हैं, इनसे समाचार पत्र का कोई लेना-देना नहीं है और वह अपने को बचा ले।
जहां तक मुझे पता है कि पीआरबी एक्ट में अनेक बंधन है और इसी बंधन के चलते समाचार पत्रों की प्रिंटलाईन में यह पंक्तियां भी जाती हैं कि समाचार चयन के लिये पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। कायदे से तो यह जिम्मेदारी सम्पादक की होना चाहिये लेकिन वह यहां भी स्वयं को बचाते हुए स्थानीय सम्पादक या फिर समाचार सम्पादक को पीआरबी एक्ट के तहत चिपका देता है।
जिस तेजी से सम्पादक अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं और बचने की छोटी-छोटी गलियां तलाश कर रहे हैं, यही कारण है कि सम्पादक संस्था की जो अहमियत थी, सम्मान था और गर्व हुआ करता था, अब गर्त में जा रहा है। सम्पादक संस्था के पास अब वक्त लेख को जांचने-परखने का नहीं है, वह तर्कपूर्ण वैचारिक बहस से स्वयं को दूर रखना चाहता है। उसका पूरा मन और समय इस जुगाड़ में गुजर जाता है कि किस तरह वह सत्ता और अखबार का संतुलन बनाये रखे क्योंकि प्रबंधन को भी सम्पादक नहीं मैनेजर चाहिये और एक मैनेजर के लिय शायद यही पंक्तियां उपयुक्त हैं कि विचार लेखक के निजी हैं, इनसे समाचार पत्र का कोई लेना-देना नहीं है।
यह ठीक है लेकिन एक बात मन में बार बार उठती है, वह यह कि क्या यह जवाबदारी स्थानीय सम्पादक या समाचार सम्पादक नहीं उठा सकता कि वह लिख सके कि अखबार में प्रकाशित हर सामग्री के लिये अंतत: वही जवाबदार है। खैर, गैर-जवाबदारी के इस समय में जवाबदारी की अपेक्षा करना बेमानी ही नहीं, निरर्थक है।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और समागम पत्रिका के संस्थापक संपादक हैं।


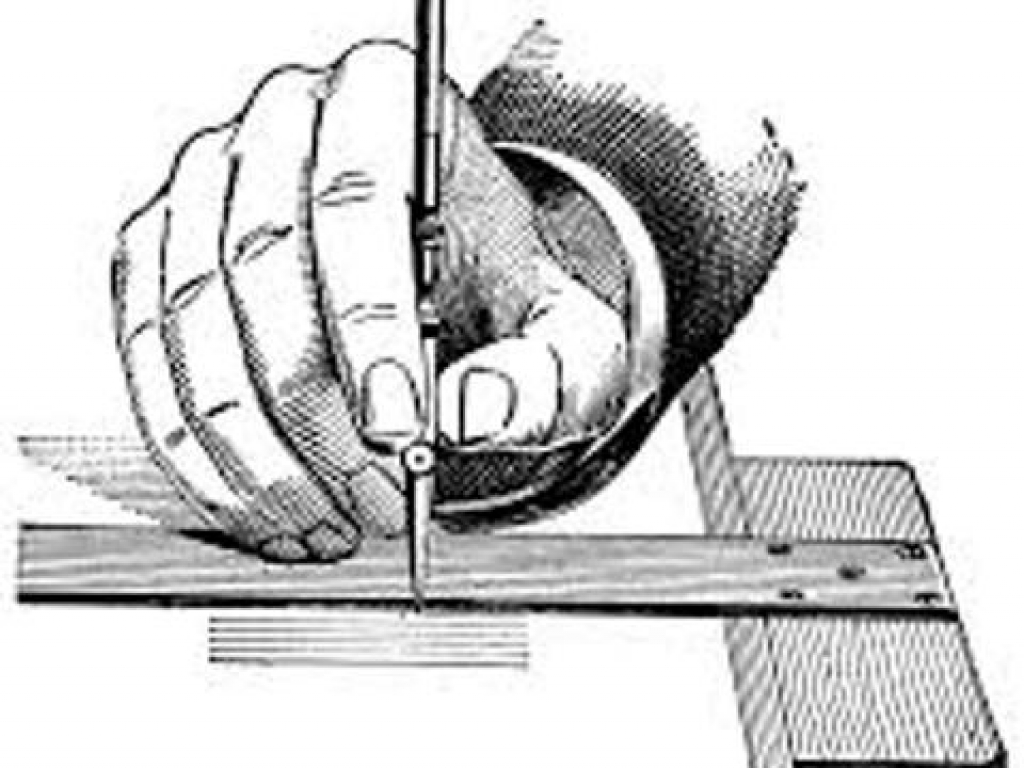





Comments